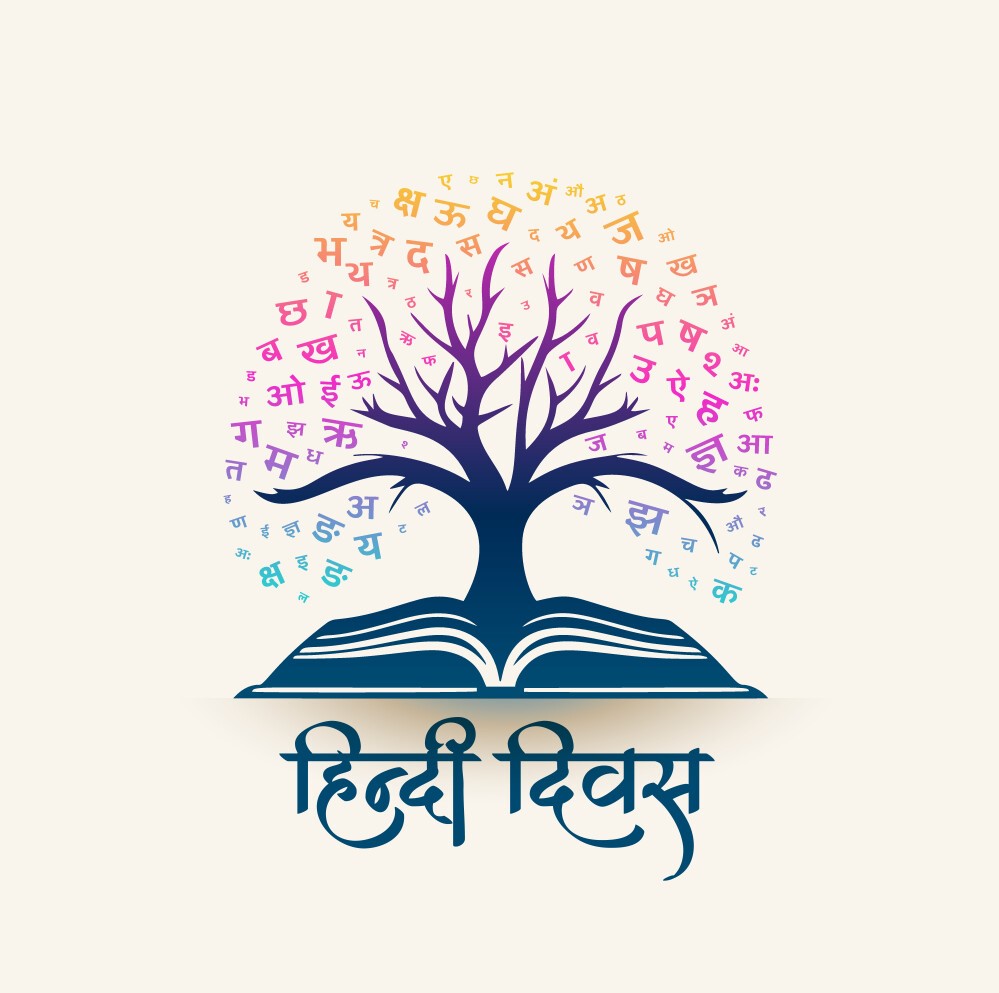
विषय सूची
- संपादकीय – अनीता वर्मा
- अलका सिन्हा, दिल्ली – फादर ऑन हायर (कहानी)
- डॉ. शैलजा सक्सेना, कनाडा – मेरी भाषा (कविता)
- डॉ. बरुण कुमार, दिल्ली – हिंदी का सरलीकरण या हिंदी का अंग्रेजीकरण? (आलेख)
- सरस दरबारी, कनाडा – भाषा (कविता)
- नरेश शांडिल्य, दिल्ली – हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे (कविता)
- डॉ. रवि शर्मा ‘मधुप’, दिल्ली – मैकाले की आत्मा (व्यंग्य कथा)
- आशा बर्मन, कनाडा – हिंदी भाषा, मेरे विचार (आलेख)
- डॉ. मंजु गुप्ता, दिल्ली – हिंदी (हिंदी)
- कल्पना लालजी, मॉरिशस – आर्टिफिशियल इनटैलीजैन्स ( ऐ आई ) (माँ ) – (कविता)
- डॉ. वेद व्यथित, फरीदाबाद (हरियाणा) – भरोसे लाल का पुस्तक प्रेम (व्यंग्य आलेख)
- डॉ सुनीता शर्मा, ऑस्ट्रेलिया – हिंदी हम सब से है (कविता)
- सुनीता पाहूजा, दिल्ली – हिंदी का वैश्वीकरण (आलेख)
- अजेय जुगरान – हिंदी सी माँ (कविता)
- डॉ सविता चड्ढा, दिल्ली – विश्व की लोकप्रिय भाषा हिंदी और मीडिया (आलेख)
- सांद्रा लुटावन, सूरीनाम (दक्षिण अमेरिका) – जय हिंदी (कविता)
- डॉ. वंदिता सिन्हा, कनाडा – हिंदी दिवस (आलेख)
- डॉ दीप्ति अग्रवाल, दिल्ली – माँ हिन्दी (कविता)
- स्वरांगी साने, पुणे (महाराष्ट्र) – भारतीय उच्चारणों का विकृतिकरण अब तो बंद हो (आलेख)
- डॉ सुनीता श्रीवास्तव, इंदौर (म.प्र.) – मेरी अभिलाषा (कविता)
- डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा ‘उरतृप्त’, महाराष्ट्र – सिंथेटिक शॉल और हिंदी की आत्मा (व्यंग्य कथा)
- निशा भार्गव, दिल्ली – भाषा (कविता)
- डॉ. संध्या सिलावट, इन्दौर (म.प्र.) – हिंदी में विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रचलन, हिंदी हेतु आशीर्वाद है या अभिशाप (आलेख)
- वर्षा महेश, मुंबई (महाराष्ट्र) – हमारी हिंदी! हमारा गौरव (कविता)
- मनोज कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली – हिन्दी दिवस (कविता)
- डॉ. वीणा विज ‘उदित’, जालंधर (पंजाब) – हिंदी की महत्ता (कविता) – प्रवासी साहित्य एवं संस्कृति में हिंदी का योगदान – (आलेख)
- शैली, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) – हिन्दी-दिवस का सार (कविता)
- डॉ॰ अर्जुन गुप्ता ‘गुंजन’, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – हिंदी साहित्य की सामाजिक तथा लोकतान्त्रिक भूमिका (आलेख)
- डॉ. पूर्णिमा, पटियाला (पंजाब) – हिन्दी का पूजन पग-पग है!! (कविता)
- नन्दकुमार मिश्र आदित्य, चम्पारण (बिहार) – जय हिन्दी (कविता)
- उर्मिला यादव ‘उर्मि’, महेंद्रगढ़ (हरियाणा) – हिन्दी भारत भाल की बिन्दी (कविता)
संपादकीय

अनीता वर्मा
विश्व में हिन्दी भाषा का बदलता परिदृश्य
वर्तमान समय भूमंडलीकरण का है, जिसका विस्तार बाजार के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। बाजार-संस्कृति ने हमारी अस्मिता, खानपान, पहनावा, भाषा, संस्कृति आदि ने उनको प्रभावित करना शुरू कर दिया है। छात्रों के सपने में बाजार का प्रवेश हो चुका है। बाज़ार को सुरक्षित रखने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। ठीक यही हिन्दी के साथ होना शुरू हुआ।विदेशों में 2010 से 2015 के अन्तराल में विश्वविद्यालय में जो छात्र बालीवुड फ़िल्मों के लिए हिंदी पढ़ते थे, उन्हीं छात्रों ने हिन्दी भाषा को इसलिए पढ़ना शुरू किया क्योंकि वो उनके व्यवसाय से जुड़ रही थी। योग, आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा पद्धति उन्हें हिन्दी भाषा से जोड़ने का कार्य करने लगी।
भाषाओं के इस विलुप्तीकरण के दौर में हिंदी अपने को न केवल बचाने में सफल हो रही है बल्कि उसका उपयोग-अनुप्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह भाषा लगभग डेढ़ हजार वर्ष पुरानी है और इसमें डेढ़ लाख शब्दावली समाहित है। हिंदी के विकास के लिए विश्व की पैंतीस सौ विदेशी कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है। वैश्विक हिन्दी परिवार भी इसी दिशा की तरफ़ अग्रसर है। वेबसाइट, हिन्दी शिक्षण, कार्यशाला, साप्ताहिक कार्यकमों में हिन्दी भाषा से उन देशों को जोड़ना जहां हिन्दी भाषी लोग कम हैं, युवाओं को कार्यक्रमों से व हिंदी से जोड़ना, अधिक से अधिक अनुवाद कार्य करना हिन्दी को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित कर रहा है। हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं का साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन, हिन्दी नाटकों के मंचन, पॉडकास्ट, कहानी, कविता पाठ इसकी प्रमुख योजनाएं हैं जिन पर बहुत उत्साह के साथ उत्कृष्ट कार्य हो रहा है।
हिंदी को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए किए जाने वाले हमारे सतत प्रयास इसे हिन्दी का वैश्विक विस्तार दे सकते है। यह सच है कि बाजार के कारण भी हिंदी का प्रचार-प्रसार व्यापक हो रहा है।हिन्दी अब साहित्य की भाषा ही नहीं, बल्कि बाजार की भी भाषा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने विज्ञापनों को जन्म दिया, जिससे न केवल हिंदी का अनुप्रयोग बढ़ा, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिले। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि भारत उनके उत्पाद का बड़ा बाजार है और यहां के अधिकतर उपभोक्ता हिंदीभाषी हैं। इसलिए उन्हें अपना उत्पाद बेचने के लिए उसका प्रचार-प्रसार हिंदी में करना पड़ेगा।
हमें हिंदी को ज्ञान और संचार की भाषा के रूप में विकसित करना होगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक अनुवाद कार्य, नई तकनीकों का प्रयोग करना होगा। AI व अन्य नवीन प्रयोगों व तकनीकी प्रयोग करके हम हिंदी के वैज्ञानिक आधार व वैश्विकता को विस्तार दे सकेंगे। भाषा के विकास के लिए बदलते तकनीकी परिदृश्य के साथ समन्वय करना ज़रूरी है। वैश्विक हिन्दी परिवार इसके लिए प्रयासरत व प्रतिबद्ध है। हिन्दी दिवस पर ये विशिष्ट विशेषांक हिन्दी भाषा के प्रति आपकी निष्ठा व प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है
अलका सिन्हा, दिल्ली

फादर ऑन हायर
मयंक मायूस भी था और झल्ला भी रहा था। कल क्या होगा, वह क्या करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह कोरिडोर की अंतिम सीढ़ी पर बैठा बाजुओं में सिर छुपाए कल के बारे में सोच रहा था।
“हे मैकी! वाट आर यू डूइंग हियर?” ऐरिक ने मयंक को झकझोर दिया, “क्लास में चल, क्या मस्ती पीट रहे हैं सब रोहित के साथ।”
यह एक पब्लिक स्कूल था और यहाँ हिंदी में बोलने पर फाइन देना पड़ता था। फिर भी, बच्चे बाज कहाँ आते थे। बड़े-बड़े रइसों के बेटे, फाइन देना कौन सी बड़ी बात थी। बल्कि फाइन देने के बाद शाम को दोस्तों में आइसक्रीम की ट्रीट भी देते थे, “फाइन ही देना पड़ा न, पर वे मुझे मेरी मातृ भाषा, आई मीन मदर टंग से जुदा तो नहीं कर पाए न !” और उपहास का ठहाका गूंज जाता।
स्कूल की मस्ती का तो क्या कहना। इसीलिए लाख बंदिशों के बावजूद सभी स्कूल में मस्ती करते हैं।
“देख मैकी, हमने ये ‘स्पिट बॉक्स’ बनाया है… स्पेशल गिफ्ट फॉर रोहित्स फादर।” ऐरिक मयंक को क्लास-रूम में ले आया था। कॉपी के गत्ते को काटकर उससे एक चौकोर डिब्बा जैसा बनाया गया था, जिसे ऊपर से गोल काटा हुआ था। स्टेला उस पर गोल्डन पेपर चिपका रही थी, “यू नो, कल जब रोहित के पापा आएंगे तो प्रखर इसे उनके पीछे-पीछे लिए चलेगा, ऐसे…।” और ऐरिक ने अभिनय प्रारंभ किया। कुछ सहमा-सहमा, दाएं-बाएं देखता दो कदम चला, फिर रुककर दाएं हाथ के अंगूठे से बायीं हथेली को रगड़ा, दो-तीन बार चार उंगलियों से पटका, फिर हथेली पर चुटकी ली और बहुत संभालकर निचले होंठों में बाहर की तरफ दबा ली। दाएं-बाएं देखकर जैसे ही उसने दीवार की ओर मुँह फेरा कि प्रखर ने गोल्डन बॉक्स आगे कर दिया।
“फच्च !” प्रखर ने आवाज की और क्लास में जोर का ठहाका गूंज गया।
पिछली बार जब रोहित के पापा पेरेंट्स-टीचर्स मीटिंग में आए थे, तब उन्होंने जहाँ-तहाँ अपने स्मृति-चिह्न छोड़ दिए थे। दोस्तों ने खूब मजाक बनाया था। स्टेला तो एक मोटा लेंस लेकर पूरे कोरिडोर में ऐसे घूमती फिरी थी जैसे वह किसी खूनी के फिंगर प्रिंट्स तलाश रही हो। बहुत दिनों तक ‘रोहित्स फादर’ का टॉपिक उनका सामूहिक मनोरंजन करता रहा था। काफी दिनों के बाद यह टॉपिक फिर से गरमाया था और सभी साथी बिलकुल नयेपन से उसका स्वाद ले रहे थे। वैसे चाहे क्लास में कितने ही ग्रुप बने हों, पर ऐसे किसी कार्यक्रम में उनकी एकता देखते ही बनती थी। अब वे लोग आगे की योजना बना रहे थे। वृंदा प्रखर को ‘डेयर’ दे रही थी, “कल तू रोहित के फादर को ये स्पिट बॉक्स गिफ्ट करेगा।”
“नहीं, गिफ्ट नहीं करेगा, पीछे-पीछे लेकर चलेगा और जब-जब वे अपने मुँह का जूस बाहर निकालना चाहेंगे, तू ये बॉक्स हाजिर कर देगा।” स्टेला ने संशोधन किया।
क्लास हँस-हँसकर दोहरी हुए जा रही थी। दसवीं कक्षा के ये साथी… पता नहीं अगली क्लास में कौन साथ रहेगा, कौन छूट जाएगा। इसलिए इस साल तो हर पल मस्ती में काटा था सबने। इस बार टीचर्स डे पर ‘ट्रुथ एंड डेयर’ खेलते हुए मयंक को डेयर दी गई थी कि वह अनुराधा मैम के पैर छूकर आए।
“इसमें क्या बड़ी बात है,” वह लम्बे डग भरता अनुराधा मैम के पास जाकर खड़ा हो गया। बच्चे क्लास रूम से बाहर झांक रहे थे।
“येस, वाट डू यू वांट मयंक?” हाथ में कई सारे गुलाब संभाले अनुराधा मैम ठहर गईं। मयंक एक पल को ठिठका, क्लास की ओर तिरछी निगाह से देखा, कई आँखें चौकसी कर रही थीं।
“हैप्पी टीचर्स डे मैम !” मयंक मैम के पैरों की तरफ झुक गया।
“गॉड ब्लेस यू माइ सन !” पचास वर्षीया अनुराधा मैम विह्वल हो गईं, “आइ नो, यू आर अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। तुम हमारा नाम रोशन करोगे।”
“नहीं मैम, ये आपकी ग्रेटनेस है।” मयंक जल्दी से वहाँ से खिसक जाना चाहता था।
“यही तो मुश्किल है मयंक, यू डोंट नो योरसेल्फ,” अनुराधा मैम ने अपने से लगभग दुगुने लम्बे मयंक के कंधे थपथपाने की कोशिश की, “यू कैन डू मिरेकल्स, बिलीव मी…।”
“मे बी विद योर ब्लेसिंग्स मैम।” मयंक बाल खुजलाता वहाँ से भाग आया। फिर क्लास में जो सब हँस-हँसकर दोहरे हुए, उसका क्या कहना !
मगर आज उसे ‘ट्रुथ एंड डेयर’ का यह खेल कोई खुशी नहीं दे रहा था। क्लास के साथी रोहित के पापा की ऐक्टिंग उतार-उतार कर हँस रहे थे।
“मेरे सो कॉल्ड पापा कैसे भी हों, आते तो हैं। पान चबाते, खैनी खाते ही सही, बोर्ड का रोल नम्बर तो दिलवा देते हैं।” रोहित ने सख़्त स्वर में आगे कहा था, “जोक्स अपार्ट…. मेरे रियल पापा की तरह अपनी बिजनेस मीटिंग्स में मुझे इग्नोर तो नहीं कर देते।”
एक पल को क्लास रूम में सन्नाटा छा गया। पिछली मीटिंग में जब बोर्ड के इम्तहान के रोल नंबर दिए जाने थे, तब सभी के पेरेंटस को स्कूल में बुलाया गया था। रोहित क्लास टीचर के पास जाकर गिड़गिड़ाया था, “मैम, माई फादर इज आउट ऑफ टाउन।”
“नो एक्सक्यूज,” मैम चिल्लाई थी, “बोर्ड के इग्ज़ैम में बैठना है तो अपने पापा को लेकर आओ।”
“नॉट पॉसिबल मैम।” रोहित लगभग रो पड़ा था।
“देन ब्रिंग योर मॉम।”
” शी इज़… शी इज़ वेरी बिजी।” शब्द रोहित के मुँह में ही रह गये थे। रोहित जानता था, कुछ भी कहना बेकार था।
अगले दिन सभी छात्रों के पापा-मम्मी आए थे। टीचर्स से परीक्षा के बारे में चर्चा की थी।
कई टीचर्स परेंट्स को समझा रहे थे, “बच्चे पर स्ट्रेस नहीं डालें, सैम्पल पेपर्स के अनुसार ही तैयारी कराएं। इन स्टूडेंट्स के साथ हमारे स्कूल की रेपूटेशन जुड़ी है। डोंट टेक इट लाइट्ली।”
बच्चे भी खुद को कुछ तनावग्रस्त महसूस करने लगे थे। मगर मयंक और ही तरह के तनाव से घिरा था। वह समझ नहीं पा रहा था, क्या करे।
“वेयर इज योर फादर मयंक ?” अनुराधा मैम ने हैरानी से पूछा था।
“ही वुड कम एनी मोमेंट।”
“बट वेयर इज ही ? आखिर कौन सा काम उनके लिए बेटे के इग्ज़ैम्स से ज्यादा इंपोर्टेंट है ?”
“ही इज़ इन ए बिजनस मीटिंग।” मयंक मुँह छुपाकर सुबक पड़ा था। मैम थोड़ा पिघल गई, “ओ के, वी विल वेट फॉर हिम।” सबके पेरेंट्स लगभग लौट चुके थे, बस मयंक और रोहित के पापा का कुछ पता न था। मगर मीटिंग का समय खत्म होने से बस कोई पाँच मिनट पहले रोहित अपने पापा को लेकर आ पहुँचा था। पाँच मिनट में वह अपने पापा को अनुराधा मैम से मिलाकर ले आया। बाहर निकलते ही उसके पापा ने जेब से सिल्वर की एक छोटी-सी डिब्बी निकाली, चुटकी भर तम्बाकू निकालकर बायीं हथेली पर रखा और अच्छे से रगड़कर उंगलियों से थपकाया, फिर चुटकी भरकर मुँह में रख लिया। सभी साथियों में हलचल होने लगी। प्रखर और ऐरिक जान-बूझकर रोहित के सामने आ खड़े हुए। रोहित ने दोनों से परिचय कराया, “माइ फादर।” अभी ऐरिक और प्रखर सोच ही रहे थे कि हाथ जोड़कर अभिवादन करें या हाथ मिलाकर कि रोहित के पापा ने मुँह उल्टी तरफ घुमाकर रंगीन पिचकारी छोड़ी-फच्च!
“रोहित के पापा मिनिस्टर हैं, सच्ची! उसने हमें इंट्रोड्यूस कराया।” वे दोनों वापस अपनी मंडली में आ मिले थे। फिर तो खूब मजाक बना था।
मगर जो भी हो, रोहित को रोल नंबर मिल गया था। मयंक मायूस बैठा था। मीटिंग खत्म होने के बाद भी मयंक के पापा नहीं आए थे। मैम नाराज हो रही थीं- कैसे पेरेंट्स हैं जिन्हें बच्चे के भविष्य की भी चिंता नहीं। मैम को मयंक से हमदर्दी थी, पर उसे रोल नंबर नहीं दिया गया। अगर इस बार भी उसके पापा नहीं आए तो संभवत: वह इस साल बोर्ड इग्ज़ैम ही न दे पाए। और इस बार ही क्यों? ये शर्तें तो हमेशा ही रहेंगी, अगले साल भी। उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह बहुत परेशान था। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके मम्मी-पापा ने उसका नाम ऐसे स्कूल में लिखाया ही क्यों? क्यों ज़रूरी है ये लाम-काफ? आखिर इग्जैम तो उसे देना है, फिर पापा का आना ज़रूरी कैसे हो गया ?
“कम ऑन मैकी, तू इतना वरी क्यों करता है,” ऐरिक ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, “तू डरता है कि तेरे पापा कल भी नहीं आएंगे और तू इग्ज़ैम नहीं दे पाएगा?” रोहित की आँखों में चमक थी, “कंसल्ट मी… डॉक्टर रोहित अग्रवाल, मेरे पास हर मर्ज की दवा है।”
सभी साथियों ने रोहित को घेर लिया, लगे मिन्नतें करने, “यार, तू ही कुछ कर। इसे भी कोई मिनिस्टर पकड़ा दे। कहीं ऐसा न हो, हम एक प्यारा-सा साथी खो दें।”
“फिकर नॉट पापे, फादर तो अरेंज हो जाएगा, पर होगा कोई पान-बीड़ी ब्रांड ही।” रोहित ने भरोसा दिलाया, “बोल है मंजूर?”
“कोई नहीं डियर, तू अरेंज तो कर, हम तेरे पापा के लिए तैयार बॉक्स मयंक के पापा को गिफ्ट कर देंगे।” दोस्तों ने मयंक की ओर से हामी भरी, मगर मयंक खामोश बैठा रहा।
अगले दिन खूब गहमा-गहमी थी। स्कूल में जैसे मेला लगा था। अन्य कक्षाओं के बच्चों के पेरेंट्स अपने तय समय के मुताबिक आकर टीचर्स से मिल रहे थे, उनसे सफलता के मंत्र हासिल कर रहे थे। मुलाकात के बाद कैंटीन की तरफ रुककर, कुछ खा-पीकर दूसरे अभिभावकों से चर्चा कर रहे थे। कैंटीन के बाहर, बीच कैंपस में स्कलैस्टिक बुक्स ने अपनी नई किताबों का मेला सजा रखा था। हर उम्र के बच्चों के लिए बेहद आकर्षक पुस्तकें। बच्चे मचल रहे थे, “मम्मा प्लीज़, गेट मी रॉबिनहुड सिरीज़…।”
ऐसा अजूबा भी इन अंगेरजी स्कूलों में ही देखने को मिलता है कि बच्चे ही किताबें खरीदने की गुहार कर रहे हों।
कैंपस के दूसरे छोर पर रंग-बिरंगे फूलों का मेला सजा था। मेन गेट के नज़दीक हरी घास का लॉन… जिसे सिर्फ देखकर मुग्ध हुआ जा सकता था, वहाँ बैठने की इजाज़त किसी को नहीं थी। चौड़े मेन गेट के दोनों तरफ साइकस के दो कीमती पेड़। कहते हैं, द्वार पर साइकस का वृक्ष लगा हो तो भीतर खुशहाली आती है। वैसे इस स्कूल में हर तरह से खुशहाली थी। खूबसूरत बिल्डिंग, सुविधा-संपन्न पुस्तकालय और प्रयोगशाला, कंप्यूटर रूम, खेल का बड़ा मैदान, पारर्दशी प्लास्टिक की छत के नीचे प्रेयर कैंपस और सबसे अधिक आकर्षक – फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते बच्चे…। जिस प्रकार दूध-घी की नदियाँ बहना वैभव का प्रतीक है, उसी प्रकार फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना, पढ़े-लिखे होने का प्रतीक समझा जाता है।
तभी, साइकस की नोंकदार पत्तियों की ओट में एक रिक्शा रुका, सफेद कमीज़-पैंट में लगभग चालीस-बयालीस की उम्र का व्यक्ति उतरा। सर के बाल तेल के अनुशासन में, सधे हुए कदमों से मार्च पास्ट करता सीधा स्कूल के ऑफिस की तरफ बढ़ा। लगता था जैसे कोई छात्र अभिभावक की भूमिका अदा कर रहा हो। उसने गार्ड से अस्फुट शब्दों में कुछ पूछा, “क्लास टेंथ… फॉर्म साइन… ?”
गार्ड ने बायीं तरफ इशारा कर दिया।
“प्लीज कम विद मी,” जाने कहाँ से मयंक अचानक आ खड़ा हुआ। वह उसे तेज कदमों से स्टाफ रूम तक ले गया। फिर लगभग बिना मुँह खोले धीरे से बोल गया, “खामखा बहस मत कीजिएगा, बस चुपचाप साइन करके आ जाइएगा।”
“ऐसी क्या बात है बेटे, तुम्हारा बोर्ड है, टीचर से मुझे भी बात करनी है।”
“पापा प्लीज़,” मयंक गिड़गिड़ा पड़ा, “आपकी बात समझने के लिए पहले यहाँ हिंदी वर्क शॉप करानी पडे़गी…। आप बस साइन कर आइए, मैं अपना साइंस-मैथ सब सुधार लूंगा…. प्रॉमिस।”
बात कहीं सूई-सी चुभ गई, “इसी हिंदी वर्कशॉप की तनख्वाह से तुम्हें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, समझे।”
“सॉरी पापा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, पर आप जितना कम बोलेंगे, हम दोनों के लिए उतना ही ठीक रहेगा।”
बहस थम गई। दोनों ने टीचर्स रूम में प्रवेश किया।
“लेबोरियस स्टूडेंट, बट सम प्रॉब्लम मिस्टर पांडे,” टीचर बातचीत करना चाहती थी, मगर पांडे साहब वचन से बंधे थे। सरकारी दफ्तर के हिंदी अधिकारी का बच्चा अंग्रेजी गमले में लगा दिया था, परेशानी तो थी। मस्तिष्क में फ्लैश बैक-सा चल रहा था, जब ड्रॉ में बच्चे का नाम पुकारा गया था, वे खुशी से भर उठे थे – अपने बेटे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊँगा।
“प्लीज़ डिपॉजिट ट्रवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ बाइ टुमॉरो, ” स्कूल ने फरमान सुनाया था। स्कूल की फीस जुटाना बहुत मुश्किल भी न था, वे इसके लिए पहले से तैयार थे। मगर स्कूल के वातावरण की और भी बहुत-सी मांगें थीं, जिनका उन्हें कतई अहसास नहीं था। हर साल का बिल्डिंग फंड, कभी फ्लड रिलीफ फंड तो कभी गरीब बच्चों के लिए डोनेशन। कभी-कभी तो लगता कि वे भी अपने बच्चे का नाम गरीब बच्चों वाले सेक्शन में लिखवा देते। मगर बच्चे का भी तो स्वाभिमान देखना था, उसकी रोज की पॉकेट मनी, कभी बर्थ-डे पार्टी का खर्चा, तो कभी बर्थ-डे गिफ्ट का। उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी।
“…अदरवाइज, ही इज इंटेलिजेंट,” टीचर एकपक्षीय संवाद बोले जा रही थी। वे टीचर की बताई जगहों पर हस्ताक्षर करने लगे तो हाथ लड़खड़ा से गए, अपने कार्यालय में हिंदी में हस्ताक्षर करने के लिए वे लम्बे-लम्बे भाषण देते हैं, मगर इस फॉर्म पर हिंदी में हस्ताक्षर करना अंगूठा छाप होने के बराबर था। उन्होंने बहुत संभालकर अंग्रेजी में वी.पी.पांडे लिखकर उसे हौले से काट दिया और नीचे तारीख भर दी। अपने जमाने के स्कूल टॉपर का आत्मविश्वास आज हस्ताक्षर करते हुए डगमगा रहा था।
वे कक्ष से बाहर निकल आए थे। मयंक आधे रास्ते तक उन्हें छोड़ आया, “मैं बाद में लौटूंगा, अभी मेरी एक्सट्रा क्लास है।”
वे गेट के बाहर निकलने लगे तो साइकस के बड़े पत्तों की नोंक बांह पर चुभ गई, जिसे हौले से सहलाते हुए वे रिक्शे पर बैठ गए।
“तुसी ग्रेट हो प्राजी !” मयंक को साथियों ने घेर लिया था।
“आइ वांट टु चेंज माइ फादर, यार,” रोहित ने मयंक के कंधे पर कोहनी टिका दी, “गेट मी वन लाइक योर्स।”
“मगर मेरे गिफ्ट का क्या होगा ?” स्टेला बोल पड़ी।
“इतना लर्नड, इतना कल्चर्ड फादर तुझे मिला कहाँ से ?”
मयंक अपने दोस्तों के कमेंट्स से हैरान था कि हिंदी का आदमी लर्नड और कल्चर्ड… दे मस्ट बी जोकिंग। वह हौले से मुस्करा भर दिया।
डॉ. शैलजा सक्सेना, कनाडा

मेरी भाषा
भाषा के आकाश में
अपने-अपने कोनों से उडाईं
सबने
अपनी-अपनी पसंद की पतंगें।
कोई चित्र लिपि में
कोई मंत्रों को लिये
कोई वाद्ययंत्रों सी ध्वनित होती हुई।
मेरी पतंग में कई रंग थे
कई उगते सूरजों की ऊष्मावान रश्मियाँ
कई डूबते सूरजों की लालिमा
कई घाटों के विविधरंगी नीर छलकते थे उससे
इतने रंग थे उसमें
कि वह पतंग नहीं रह गई
स्वयं आकाश हो गई
मेरे हिस्से का और मेरे जैसे एक अरब से भी ऊपर के लोगों का आकाश!
हम इस आकाश के तले,
गेहूँ की बालियों पर कवितायें लिखते
और ज़मीन में अपनी कल्पनाओं के बीज बोते।
हवाओं के पंखों पर
तितलियों के परों जैसे चमकीले गीत लिखते
और जंगलों में ॠचाओं से गूँजने लगते।
इस आकाश तले
हमने
शुरू की बनानी वो सड़क
जो
साहित्य और जीवन तक जाती है,
हम कूटते हैं
अपने विचारों, तर्कों की ईंटे
और डालते हैं इस पर अपनी मानवीय संवेदना का तारकोल
हम सदियों से बढ़ाते जा रहे हैं यह सड़क
और शामिल करते जा रहे हैं हर
पीछे छूट गये आदमी की पीड़ा को,
हम समेटते चले जाते हैं
हर दृश्य के सौन्दर्य को अपनी इस सड़क में।
आकाश के इस कोने के नीचे
संस्कृति के अविरल बहते सागर से
हमने जाने कितने ही
दर्शनों के मुक्ता माणिक निकाले
और पाया जीवन का,
जीवन को कहने का सौन्दर्य।
फिर हम गाने लगे इस सुन्दरता को
अनुभव करने लगे शिवम को
सुनने लगे सत्य को।
हम इसी भाषा में प्यार करते हैं,
लड़ते हैं, बहसते हैं, गाते हैं, लगातार हँसते चले जाते है
हम अपने को ढूँढने इसी भाषा में उतरते हैं गहरे
मैं देख रही हूँ
मेरी भाषा का आकाश फैल रहा है
कई सागरों, पर्वतों जंगलों को ढ़के हुये
लगातार फैल रहा है
मैं खुश हूँ
कि मैं भी उसके हज़ारों रंगों में घुली
उसकी हवाओं की खुश्बू सी
हो गई हूँ
जिसके इस छोर के पद्य से
उस छोर के गद्य तक फैल रही है
एक व्यापक मानवीय संवेदना!
मेरी भाषा
वसुधैव कुटुंबकं सी,
बन गई है
जीवन की ऊष्मा की भाषा।
डॉ. बरुण कुमार, दिल्ली

हिंदी का सरलीकरण या हिंदी का अंग्रेजीकरण?
“संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।”
(अनुच्छेद 351,भाग-XVII, भारतीय संविधान)
भारतवर्ष ढेर सारी भाषाओं का देश है। आठवीं अनुसूची में दर्ज बाईस बड़ी भाषाओं के अतिरिक्त अन्य कितनी ही बड़ी-छोटी भाषाएँ यहाँ प्रचलित हैं। २०११ की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ऐसे लोग जो १०००० से ज्यादा एक भाषा को बोलते हैं ऐसी १२१ भाषाएँ भारत में बोली और समझी जाती हैं। पूर्वोत्तर भाषा की दृष्टि से सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश है। यहाँ तीन सौ से अधिक भाषाएँ हैं, हालाँकि यह आबादी की दृष्टि से देश की जनसंख्या का केवल पाँच प्रतिशत ठहरता है। इतनी सारी भाषाओं के प्रदेश में कभी यह मांग नहीं उठी कि बंगला भाषा सरल की जाए, असमिया सरल की जाए, मिजो सरल की जाए। या फिर, दक्षिण भारत में तमिल को या तेलुगु को या मलयालम को, कन्नड़ को आसान किया जाए। मराठी, गुजराती, पंजाबी वगैरह के लिए भी यह मांग कभी नहीं उठी। तो फिर अकेली हिंदी के साथ सरलता की मांग क्यों है?
दरअसल इसकी वजह हिंदी को राजभाषा का दायित्व प्रदान करना है। राजभाषा यानी राजकाज की भाषा, सरकार के काम करने की भाषा। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान में संकल्प लिया गया है। प्रजातंत्र में चूँकि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की बनी हुई सरकार होती है इसलिए जनता की सरकार को जनता की भाषा में काम भी करना चाहिए। जब हिंदी राजभाषा बनी तो इसके प्रयोग का एक नया क्षेत्र खुला। चूँकि हमने आजादी के बाद अंग्रेजों की शासन-व्यवस्था को विरासत में ग्रहण किया था इसलिए हमारे पास अंग्रेजी की शब्दावली, अंग्रेजी के अर्थ, अंग्रेजी की अवधारणाएँ, अंग्रेजी का ढाँचा और तौर-तरीके विरासत में मिले थे। इसलिए हिंदी में काम करने के लिए ऐसे शब्दों की जरूरत पड़ी जो हिंदी में दिखें तो सही लेकिन अंग्रेजी का ही अर्थ दें। फलस्वरूप हिंदी को राजभाषा के रूप में व्यवहार करने के लिए अंग्रेजी के समान अर्थ वाले शब्द बनाने पड़े। इन नए गढ़े गए शब्दों से, पूर्वप्रचलित शब्दों के भी अंग्रेजी के अर्थ में प्रयोग से और अंग्रेजी की तर्ज पर बनी वाक्य-रचना से भाषा में कृत्रिमता आनी स्वाभाविक थी। ऐसे में हिंदी पर कठिन होने और हिंदी जैसी नहीं दिखने का आरोप लगने लगे। उसे ‘महाराजभाषा’, ‘फीलपाँवी हिंदी’ आदि कहकर ताने दिये जाने लगे। इसलिए हिंदी के सरलीकरण की मांग का एक संदर्भ है – यह उस हिंदी से अभिप्रेत है जिसका प्रयोग सरकार में किया जाता है। अन्यथा जनसामान्य की भाषा के रूप में हिंदी वैसे ही प्रचलित और व्यवहृत है जैसे कि कोई भी भाषा होती है। उस हिंदी को सरलीकृत करने का कोई खयाल भी किसी के मन में नहीं आता।
भाषा में कठिनता दो तरह से आती है – अगर अर्थ ऐसा हो जो अमूर्त, गंभीर एवं जटिल हो। धर्म, दर्शन, कानून आदि में ऐसे अमूर्त अवधारणापरक गंभीर अर्थ वाले शब्दों की भरमार होती है। इसलिए ये विषय भी कठिन समझे जाते हैं। दूसरी तरह से जटिलता आती है जब अर्थ तो कठिन या अमूर्त नहीं होता लेकिन उस अर्थ का वाहक शब्द ही अपरिचित या अल्पपरिचित होता है। शब्द अगर जाने हुए हों तो उनका अर्थ-बोध तुरंत होता है। जिन शब्दों को हम बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, उनसे परिचय गहरा हो जाता है और वे आसान हो जाते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग के लगभग छह दशकों में ऐसे कितने ही शब्द हैं जो प्रचलन में आ गए हैं और स्वाभाविक लगने लगे हैं। इनके बारे में याद करना पड़ता है कि ये तो गढ़े हुए कृत्रिम शब्द हैं। जैसे, कार्यालय, परिपत्र, ज्ञापन, आवेदन, अधिकारी, प्रबंधक, सचिव, सहायक, निरीक्षक, विभागाध्यक्ष आदि। इन शब्दों के इनके कठिन होने की शिकायत शायद ही कोई करेगा। लेकिन जो शब्द अप्रचलित हैं या जिन्हें हमने कम व्यवहार किया है उनके बारे में मांग आ जाती है कि उनकी जगह अंग्रेजी शब्दों को ही क्यों न उठा लिया जाए।
एक हद तक तो यह मांग ठीक भी है। लेकिन क्या इसको हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं? अधिकारी, विभागाध्यक्ष, सचिव जैसे कितने ही शब्द, जो आज चल चुके हैं, उनकी तुलना में ऑफिसर, हेडऑव डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी वगैरह का प्रयोग अभी भी अधिक होता है। अगर सरलता की तलाश में हम अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग करने लगें तो फिर क्या हम उसी जगह नहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी? हमें फिर से अधिकारी के लिए ऑफिसर ही लिखना पड़ेगा, लिपिक को क्लर्क ही लिखना पड़ेगा, सहायक को असिस्टेंट, शाखा को ब्रांच, प्रबंधक के लिए मैनेजर और शाखा प्रबंधक के लिए ब्रांच मैनेजर ही लिखना पड़ेगा। हमें परिपत्र के लिए सर्कुलर, आदेश के लिए ऑर्डर, पत्र के लिए लेटर ही रखना पड़ेगा। चूँकि अंग्रेजी का प्रयोग बदस्तूर चल रहा है, इसलिए हिंदी के शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी की तुलना में कम ही रहेगा। अगर सिर्फ प्रचलन को आधार बना लें तो उसका सीधा सीधा मतलब यह निकलेगा कि हमें हिंदी के शब्दों को छोड़कर अंग्रेजी के ही शब्द व्यवहार करने हैं। हमने हिंदी में काम करने के लिए हिंदी के शब्दों के प्रयोग की जो परंपरा शुरू की थी उन प्रयासों को ही छोड़ देना पड़ेगा। क्या अंग्रेजी के शब्दों से बनी भाषा को हम हिंदी कह सकेंगे? संविधान का अनुच्छेद ३५१ हिंदी भाषा के बारे में सरकार के दायित्वों को परिभाषित करता हुआ कहता है कि हिंदी की मूल प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदी का प्रयोग करना है। क्या हिंदी में अंग्रेजी के शब्द भरकर हिंदी की मूल प्रकृति की रक्षा हो सकेगी? दुर्भाग्य से सरलीकरण के उत्साही पैरोकारों का ध्यान इस अंतर्विरोध की ओर बहुत कम जाता है। अगर अंग्रेजी के शब्दों को ही हम यथावत लेते रहेंगे तो उसकी सीमा क्या होगी? अगर सचिवालय के लिए सेक्रेटेरिएट, सचिव के लिए सेक्रेटरी, अध्यक्ष के लिए चेयरमैन ही ले लें तो फिर क्या सारे पदनाम और विभागों के नाम भी अंग्रेजी में ही रहेंगे? फिर संज्ञाओं के साथ-साथ क्रियाएं भी अंग्रेजी की लेनी पड़ेंगी। जब अर्थवान शब्द अंग्रेजी के होंगे तो हिंदी के क्या केवल सर्वनाम, कारक चिन्ह, अव्यय, सहायक क्रियाएं और कालवाचक ही रहेंगे?
सरलीकरण का मामला इतना सरल नहीं है जितना अक्सर समझ लिया जाता है। भाषा सरल होनी चाहिए यह बिल्कुल वाजिब मांग है। यह भी सही है कि भाषा माध्यम है उसे भावों और विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे तक ले जाने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन यह कोई यांत्रिक वाहन भी नहीं है कि यहाँ से माल उठाकर वहाँ रख दिया। वह अपने आप में एक प्रणाली है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है, उसका एक अपना संस्कार है, उसकी एक पूरी दुनिया है। अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी आए हैं तो उसके पिता के प्रति सम्मान सहित कह रहे हैं। पर अगर हम कहते हैं कि तुम्हारा बाप आया है तो घटना तो एक ही है लेकिन एक में उसके पिता के प्रति सम्मान व्यक्त होता है जबकि दूसरे में अवहेलना। और अंग्रेजी में कहते हैं, Your father has come तो यह स्पष्ट नहीं होता कि हमने फादर के प्रति सम्मान प्रकट किया या अवहेलना। इसकी अंतर की जड़ें इस बात में निहित हैं कि पश्चिम के समाज में उम्र में बड़े होने के आधार पर सम्मान देने की प्रथा नहीं है। वहाँ सभी बराबर समझे जाते हैं। इसलिए भाषा सिर्फ माध्यम है इतना कह देना काफी नहीं है। भाषा माध्यम तो है लेकिन जितना हम समझते हैं उससे बहुत ज्यादा संप्रेषित करती है। इसलिए भाषा के प्रयोग में अगर हम शब्दों का विस्थापन करेंगे तो इसके संस्कारों को ही खंडित करेंगे। इसलिए वह भाषा जो आजकल हिंग्लिश के नाम से जानी जा रही है – अंग्रेजी शब्दों से लदी हुई भाषा – वह सरलता की भाषा होगी, ऐसा तुरंत मान लेना कठिन है।
सरलता होनी चाहिए लेकिन किन शर्तों पर? भाषा की एक अपनी मर्यादा, एक अपना अनुशासन होता है। अंग्रेजी के साथ इस मर्यादा और अनुशासन का निर्वाह अवश्य किया जाता है लेकिन हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के साथ नहीं। भारतीय भाषाओं को बोलते समय अंग्रेजी के शब्द जिस तरह मिलाए जाते हैं वैसा अंग्रेजी बोलते समय नहीं किया जाता। हिंदी में तो हम कहते हैं कि आप मेरे रेसिडेंस पर थ्री थर्टी बजे आ जाइए। लेकिन अंग्रेजी में हम कभी ऐसा नहीं कहते, “यू कम ऐट माय निवास एट साढ़े तीन बजे।” अंग्रेजी में हिंदी शब्दों की मिलावट के दो-चार नमूने दिखाकर हिंदी में अंग्रेजी की बेलगाम मिलावट की वकालत करना दरअसल समाज को गुमराह करना है। मीडिया विशेषज्ञों की दलीलों और स्वयं मीडिया की भाषा ने इस संबंध में घोर मिथ्या और भ्रम का वातावरण रच रखा है। मीडिया की भाषा आज घोर प्रदूषण और अपसंस्कृति की शिकार है।
हिंदी की क्लिष्ठता का एक अन्य पहलू भी है – उसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग। संस्कृतनिष्ठ हिंदी क्लिष्ठ होती है, उससे बचा जाना चाहिए ऐसी मांग लोगों से अक्सर ही सुनने को मिलती है। संस्कृत शब्दों से हिंदी की वैसी प्रीति नहीं है, जैसी अन्य भारतीय भाषाओं की। पंजाबी, जिसमें उर्दू के शब्दों की प्रीति हिंदी के ही समान, बल्कि उससे बढ़कर है, उसको छोड़कर अन्य किसी भी भारतीय भाषा में तत्सम शब्द क्लिष्ठ नहीं होते। बांग्ला, असमिया, ओड़िया, तमिल तेलुगू, कन्नड, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि में संस्कृत शब्दों के ग्रहण की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हिंदी में जो तत्सम शब्द भारी-भरकम लगते हैं, वे बंगलाभाषियों के सामान्य व्यवहार के शब्द हैं। इसलिए राजभाषा हिंदी में जब संस्कृत के शब्द आते हैं तो उनसे बंगलाभाषियों को या उड़ियाभाषियों को या तमिलभाषियों को कठिनता का वैसा एहसास नहीं होता जैसा हिंदीभाषियों को होता है। सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करते समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस हिंदी का प्रयोग उनके द्वारा भी किया जाना है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है।
पारिभाषिक शब्दावली के लिए नए शब्दों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। शब्द-निर्माण के स्रोत और पद्धति उस भाषा की परम्परा से आते हैं। हिंदी की भाषिक परम्परा संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश की है। शब्दावली के निर्माताओं को जब शब्द-निर्माण की आवश्यकता पड़ी तो स्वाभाविक रूप से उन्हें संस्कृत के स्रोतों की ओर जाना पड़ा। उर्दू की परम्परा अरबी-फारसी की है। उससे हिंदी के लिए व्युत्पन्न शब्द नहीं बनाए जा सकते। राजभाषा हिंदी में उर्दू के उन्हीं शब्दों को लिया जा सकता है जो हिंदी में बिल्कुल आत्मसात हो गए हों और जिनसे फिर नए शब्द बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हो।
राजभाषा हिंदी की क्लिष्ठता और कृत्रिमता का असल कारण कुछ और है। वह है हिंदी में मूल रूप से काम न होना। लोग पहले अंग्रेजी में लिखते या सोचते हैं, बाद में उसका हिंदी में रूपांतर करते हैं। ऐसी हिंदी अनुवाद की भाषा प्रतीत होती है। भाषा अगर मूल रूप में प्रयुक्त हो तो स्वाभाविक लगेगी, लेकिन अगर उसे किसी दूसरी भाषा का प्रतिरूप बनाने की चेष्टा की जा रही हो तो उसका नकली और विद्रूप लगना तय है। राजभाषा हिंदी की शब्द से लेकर वाक्य रचना सब कुछ अंग्रेजी से प्रभावित है। हम हर जगह Work in progress के लिए हिंदी में ‘कार्य प्रगति पर है’ लिखा देखते हैं, जबकि कार्य का प्रगति पर होना हिंदी का मुहावरा है ही नहीं। बोलचाल में तो हम कहते हैं ‘काम चल रहा है’ या ‘काम हो रहा है।’ अंग्रेजी शिक्षितों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ हिंदी के शब्द और वाक्य विन्यास को अंग्रेजी की तर्ज पर ढालने की मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है। एक सोच लोगों के मन में विकसित हो गई है कि हिंदी ऐसी होनी चाहिए जिसको अंग्रेजी पढ़े लोग समझ लें। इसके संकेत सत्ता के शीर्ष तक में देखने को मिल रहे हैं। उन्हें लगता है कि खालिस हिंदी शब्दों के प्रयोग से वे केवल हिंदी प्रदेशों तक ही सीमित रह जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर पूरे भारत तक पहुँच सकेंगे। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अब वह हिंदी भी कठिन और अस्वाभाविक होती जा रही है जिसका प्रयोग सरकारी तंत्र के बाहर स्कूल, कॉलेजों, पत्र-पत्रिकाओं आदि में होता है। मीडिया तो इसका सबसे बड़ा अपराधी है ही। हमें सचमुच हिंदी को कृत्रिमता से बचाने की जरूरत है। उसके अपने शब्द, मुहावरे, विन्यास, रूढ़ियाँ आदि जिंदा रखने होंगे। लेकिन इसके लिए भाषा के प्रति अपनी समझ सही रखनी होगी। यह कोशिश कि हिंदी ऐसी बना दी जाए कि हिंदी के अर्थवान शब्दों को सीखे बिना केवल उसके संरचनात्मक शब्दों – सर्वनाम, कारक चिन्ह, सहायक क्रियाओं आदि – से ही काम चल जाए, अत्यंत दुखद है। क्या केवल ‘ही’, ‘शी’, ‘इट’, ‘दे’, ‘यू’, ‘इज’, ‘एम’, ‘आर’, ‘वाज’, ‘वेयर’ ‘शैल’, ‘विल’ ‘शुड’, ‘वुड’ और प्रिपोजीशनों के बल पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं। लेकिन लगता है सारे देश को यह रोग लग गया है कि अंग्रेजी ही प्रमाण है और इस देश की भाषाओं को उसका अनुकरण करना है। भाषा को जानने-समझने-इस्तेमाल करने के लिए उसके पास जाकर, उसको सीखना होता है। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं चल सकता। भाषा के अंदर भी तकनीकी या विशेष क्षेत्र की अपनी अपनी शब्दावली होती है, उसे प्रयास करके सीखना पड़ता है। अंग्रेजी जानते हों तब भी उसमें कानून विज्ञान व्यापार प्रबंधन आदि की विशिष्ट शब्दावली को अलग से सीखना पड़ता है राजभाषा भी प्रयुक्ति का एक विशेष क्षेत्र है, उसे भी सीखना, जानना होगा। सरकारी तंत्र में अंग्रेजी के आदी बाबू हिंदी के शब्दों को सीखने की बजाय हिंदी को ही बदलकर अंग्रेजीमय करने की मांग कर रहे हैं। विडम्बना और अत्यंत दुख की बात है कि ऐसा हो भी रहा है। सरलता की जो गलत अवधारणा पढ़े-लिखे लोगों के मन में बन गई है वह अंततः हिंदी के अस्तित्व पर ही खतरा उपस्थित कर रही है।
सरस दरबारी, कनाडा

भाषा
भाषाएँ तो सब सुन्दर हैं
भाषा में निहित मान अपना
कोई छोटी न कोई बड़ी
सबमें बसा सम्मान अपना
यह तो अल्हड सहेलियाँ हैं
हाथों में हाथ लिये फिरतीं
कुछ गोरी तो कुछ साँवर सी
कोई भी भेद न मन धरतीं
फिर क्योंकर अपनी भाषा को
औरों से कम समझते हैं
उसके ओजस और तेज़ को
अज्ञान से यूँ ढक देते हैं
अपनी सब वेद ऋचाओं से
जीवन दर्शन का ज्ञान मिला
हैं असंख्य विश्व की भाषाएँ
हिंदी को तीसरा स्थान मिला
साहित्य मिला अनमोल जहाँ
ऐसी समृद्ध यह भाषा है
महादेवी पंत निराला ने
भावों से जिसे तराशा है
तुलसी मीरा जायसी के
पद ने जिसको संवारा है
जिसके गीतों की सुर लहरी
से मोहित यह जग सारा है
हिंदी केवल बिंदी नही
वह तो इस देश का ताज है
जिसकी आभा मीलों फैली
अनगिन देशों में राज है
महिमा से उसकी प्रेरित हो
विदेशों ने अपनाया है
हिंदी के वैभव, गौरव ने
दुनिया को आज रिझाया है
किसी और को नीचा करने से
है निज सम्मान नहीं बढ़ता
उसकी ही महिमा होती कम
बोली अपमान की जो गढ़ता
साहित्य विचार हैं मानव के
जिसकी न कोई भाषा हैं
वह तो एहसास है अंतस के
भाषा ने जिसे तराशा है
फिर क्योंकर मानव जब देखो
भाषा को लेकर लड़ते हो
जिसके अपने मन भेद नहीं
उसे लेकर व्यर्थ झगड़ते हो
यह भेद तुम्हारे मन में है
है मान अपमान का ज़हर भरा
तुमने भाषा में हरदम ही
है पक्षपात का गरल भरा
उस विष को क्योंकर हरदम तुम
इनके रिश्तों में बोते हो
यह तो सदा से निश्छल हैं
इनको निश्छल ही रहने दो
आओ मिलकर प्रण करें हम
हर भाषा का सम्मान करें
ऊँची करने अपनी भाषा
ना दूजी का अपमान करें
नरेश शांडिल्य, दिल्ली

हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे
हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे,
भारत देश में हम, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे ;
भारत की भाषाएं लाएंगे,
भारत देश में हम, भारत की भाषाएं लाएंगे।
जर्मन हो, जापान, चीन या रूस कि तुर्किस्तान,
सबने अपनी भाषा में ही ऊंची भरी उड़ान ;
हम भी अलख जगाएंगे, घर-घर अलख जगाएंगे,
भारत देश में हम, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे।
पौंछ ही देंगे दीवारों से मैकाले के नारे,
दिखला देंगे काले-अंग्रेज़ों को दिन में तारे ;
बापू की बात उठाएंगे, बापू का स्वप्न सजाएंगे,
भारत देश में हम, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे।
अंग्रेज़ी से बैर नहीं है, अंग्रेज़ी भी सीखें,
लेकिन हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी दीखें ;
ख़ुद को क्यों बिसराएंगे, ख़ुद्दारी अपनाएंगे,
भारत देश में हम, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे।
पटरानी थी जो इस घर की, बन बैठी क्यों आया ?
हटा ही देंगे मां के सिर से अब ये काली छाया ;
मां को चंवर डुलाएंगे, आसन पर बिठलाएंगे,
भारत देश में हम, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे।
भाषा अपना हक़ है इसको हर कीमत पर लेंगे,
कट जाएंगे, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे ;
क्रांति का बिगुल बजाएंगे, जन-जन का गीत गुंजाएंगे,
भारत देश में हम, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे।
डॉ. रवि शर्मा ‘मधुप’, दिल्ली

मैकाले की आत्मा
मैकाले तो आम आदमी की तरह वक्त आने पर नश्वर देह को त्यागकर इस संसार से कूच कर गए। परंतु आत्मा तो अजर-अमर है। शरीर से निकलने के बाद वह यमदूतों के साथ चल देती है। ऐसा प्रायः सामान्य आत्माएँ करती हैं। कुछ आत्माएँ असामान्य-असाधारण होती हैं। वे बँधे-बँधाए कायदे कानूनों को नहीं मानतीं। मैकाले की आत्मा भी ऐसी ही असामान्य-असाधारण आत्मा थी। मैकाले की मृत्यु के बाद उसने धरती न छोड़ने का निर्णय लिया। यमदूतों की तेज नज़रों से बचना कठिन था।
मैकाले की आत्मा छुपने की जगह तलाशने लगी। उसे अधिक समय नहीं लगा। वह जानती थी कि मैकाले ने अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बनाया था – भारतवासियों को शिक्षित, सभ्य और आधुनिक बनाने का। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैकाले ने आजीवन प्रयास किया। तीनों लक्ष्यों को साधने का एक रामबाण उपाय उसे सूझ गया था। वह था – अंग्रेज़ी भाषा और अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति। उसने अपने इस महान कार्य को करने की शुरुआत भी कर दी थी। काम चल रहा था। इसी बीच मैकाले के शरीर ने साथ छोड़ दिया। काम अधूरा रह गया। मैकाले की आत्मा को अपने छुपने के लिए भारत से बेहतर और कौन-सी जगह मिल सकती थी ? मैकाले मरा। यमदूत आए। शरीर पड़ा था। आत्मा गायब थी। यमदूतों ने सब जगह ढूँढ़ा। ‘डिपार्टमेंटल इंक्वायरी’ हुई। अंत में इस आत्मा को असामान्य-असाधारण ‘लापता आत्माओं’ की श्रेणी में डालकर फाइल बंद कर दी गई।
मैकाले की आत्मा अब आज़ाद थी। उसने राहत की साँस ली और जुट गई अपने मिशन पर। मैकाले के शरीर में रहते-रहते उसे मैकाले से प्यार हो गया था, इसलिए मैकाले के देहांत के बाद उसने मैकाले के सपने को अपना सपना बना लिया था। देश में आज़ादी का आंदोलन ज़ोरों पर था। चारों ओर अंग्रेज़ों, अंग्रेज़ी तथा अंग्रेज़ियत का जमकर विरोध हो रहा था। मैकाले की आत्मा ने दुबके रहने में ही भलाई समझी। उसे यह भी मालूम था कि भारत में आत्माओं को वश में कर लेने वाले तांत्रिक भी होते हैं, जिनसे बचकर रहना बहुत ज़रूरी था। अगर वह किसी तांत्रिक के हत्थे चढ़ जाती, तो उसकी सारी हेकड़ी हवा हो जाती, उसकी आज़ादी उससे छिन जाती तथा उसे उस तांत्रिक के इशारों पर नाचना पड़ता। भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम निरंतर आगे बढ़ता रहा। मैकाले की आत्मा शांति से सारा तमाशा देखती रही। वह उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रही थी।
अंततः भारत स्वतंत्र हो गया। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त हो गया। लोग अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालकर खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जंग जीत ली गई है। किसी को भी ज़रा-सा आभास तक न था कि मैकाले की आत्मा भारत में ही भटक रही है। मैकाले की आत्मा चूँकि शरीर त्याग चुकी थी, इसलिए अब किसी भी शरीर में प्रवेश कर, उस शरीर की आत्मा को अपने वश में कर लेना तथा उससे मनचाहे काम करवा लेना, उसके लिए सरल था। मैकाले की आत्मा अच्छी तरह जानती थी कि उसके लक्ष्य के मार्ग में रोड़े अटकाने वाले वे लोग हैं, जो भारत, भारतीयता, भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हैं। उन्हें ठिकाने लगाए बिना तथा मैकाले के मानस पुत्रों को ऊँचे पदों पर बिठाए बिना, उसकी दाल नहीं गलने वाली।
मैकाले की आत्मा ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी – महात्मा गाँधी नामक दुबला-पतला, मगर मजबूत व्यक्ति, जिसने साफ़ शब्दों में कह दिया था, ”दुनिया को कह दो कि गाँधी अंग्रेजी भूल गया। ….यदि मेरे पास तानाशाही शक्ति होती तो मैं आज से ही अंग्रेज़ी पढ़ना-पढ़ाना बंद करवा देता।“ आदि आदि। ऐसी बातें मैकाले की आत्मा को तीर-सी चुभतीं। इसीलिए महात्मा गाँधी उसे फूटी आँख न सुहाते। एक दिन उसने नाथू राम गोडसे नामक व्यक्ति की आत्मा को काबू किया तथा उसके हाथों गाँधी जी को बैकुंठ धाम पहुँचा दिया।
स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया था। लोकतंत्र की आत्मा बसती है – उसके संविधान में। भारत का संविधान बनाया जाने लगा। मैकाले की आत्मा चिंतित हो उठी। यदि कहीं भारतीयता समर्थकों ने हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान में महत्त्वपूर्ण स्थान दे दिया तो…और इस तो पर आकर मैकाले की आत्मा की सूई अटक जाती। उसका रक्तचाप बढ़ जाता। साँसें तेज़ चलने लगतीं और दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता। आप कहेंगे कि आत्मा को यह सब नहीं होता, तो मैं आपको बता दूँ कि सामान्य आत्मा को नहीं होता, मगर मैकाले की आत्मा तो असामान्य-असाधारण आत्मा थी, जो लापता थी और चौदह भुवनों (लोकों) के यमदूत उसे ढूँढ़कर हार गए थे, जैसे डॉन को ग्यारह देशों की पुलिस नहीं ढूँढ़ पा रही थी।
भारत की आज़ादी के बाद धीरे-धीरे मैकाले की आत्मा की ताकत दिन-पर-दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने संविधान निर्मात्री समिति के सदस्यों की आत्माओं को अपने वश में करने के लिए साम-दाम-दंड-भेद जैसी नीतियाँ अपनाईं। अधिक तो नहीं, किंतु कुछ सदस्य अवश्य ही उसके मायाजाल में फँस गए।
संविधान बना, मगर अंग्रेज़ी में। संघ की राजभाषा बनी – हिंदी, मगर अंग्रेज़ी पंद्रह वर्ष तक साथ-साथ चलने की बात भी जोड़ दी गई। अब मैकाले की आत्मा को लगा मानो उसने आधा किला जीत लिया हो। मैकाले की आत्मा को यदि भारतीय नेताओं में कोई सर्वाधिक पसंद था, तो वह था – जवाहर लाल नेहरू। वह उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती थी। मैकाले की आत्मा ने दिन-रात एक कर दिया, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, सारी नीतियाँ अपनाईं और नेहरू जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाकर ही दम लिया। उनके प्रधानमंत्री बनने से मैकाले की आत्मा की जान में जान आई। मैकाले की आत्मा को अब भारत में मैकाले के सपने सच होने की संभावनाएँ दिखाई देने लगीं।
इतना होने पर मैकाले की आत्मा ने अपने अगले मिशन पर आगे कदम बढ़ाए। उसने अन्य भाषा-भाषियों को भड़काना शुरू किया। और तो कोई उसके काबू नहीं आया, हाँ तमिल वाले मैकाले की आत्मा की चिकनी-चुपड़ी बातों में आ गए। हिंदी विरोध को लेकर उन्होंने खूब बवाल मचाया, दंगे-फसाद किए, तोड़-फोड़ की और अपने लिए विशेष दर्जा तो लिया ही, साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री से संसद में यह आश्वासन भी ले लिया कि जब तक एक भी राज्य अंग्रेज़ी का पक्ष लेगा, अंग्रेजी चलती रहेगी।
संविधान और संसद में अंग्रेज़ी का आसन मज़बूती से जमा देने के बाद मैकाले की आत्मा थोड़ी संतुष्ट हुई। अब वह चल पड़ी जनसामान्य में अंग्रेज़ी के प्रचार-प्रसार के लिए। उसे यह देखकर घोर निराशा हुई कि सरकार की जी तोड़ कोशिशों के बावजूद भारत का सामान्य जन अंग्रेजी के प्रति आकर्षित नहीं हुआ। मैकाले की आत्मा के सौभाग्य और संयोग से उसी समय साम्यवाद का किला ध्वस्त करके पूँजीवाद की प्रतिनिधि महाशक्ति ‘विश्वविजय’ के अभियान पर निकली।
अंग्रेज़ी और पूँजीवाद का तो चोली-दामन का साथ है। अंग्रेज़ी से पूँजीवाद पनपता है और पूँजीवाद से अंग्रेज़ी का प्रचार-प्रसार होता है। मैकाले की आत्मा ने ‘आव देखा न ताव’ घुस गई संसद भवन में। दरअसल उसे तलाश थी – सत्ता शिखर पर बैठे मैकाले के मानस पुत्रों की। इसके लिए भारतीय संसद सर्वाधिक उपयुक्त स्थान था। हिंदी और भारतीय भाषाओं में जनता से वोट की भीख माँगने वाले हमारे अधिकतर माननीय सांसद संसद भवन में घुसते ही मैकाले की आत्मा को नित्य नियम से प्रणाम किया करते थे। उनकी इसी श्रद्धा भक्ति को देख-समझकर ही मैकाले की आत्मा ने संसद भवन में प्रवेश किया।
अभी भी काफी सांसद मैकाले की आत्मा के प्रभाव से अछूते थे, उनका ‘ब्रेन वाश’ करना शुरू किया। सांसदों के मन में सोए अंग्रेज़ी प्रेम को जगाया। चूँकि पूरा देश सांसदों के ही इशारों पर नाचता है, अतः सांसदों में अंग्रेज़ी प्रेम जागते ही पूरे देश में अंग्रेज़ी प्रेम अंगडाई लेने लगा। सांसदों ने उद्योगपतियों से साँठ-गाँठ करके अपने भाई-भतीजों, बीवी-बच्चों के नाम से जगह-जगह अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल खोलने शुरू कर दिए। जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि इस देश में सबसे अच्छा धंधा है – अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल तथा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलने का। ये, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी आए चोखा, कहावत का साक्षात प्रमाण हैं।
मैकाले की आत्मा ने अंग्रेज़ी शिक्षा के संबंध में अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई ‘फिल्टरेशन थ्योरी’ को ही आगे बढ़ाया। महानगरों के अंग्रेज़ी माध्यम के पब्लिक तथा कांवेंट स्कूलों में पढ़ा-पला उच्च वर्ग तो पहले से ही अंग्रेज़ी का भक्त था। धीरे-धीरे देश भर में भ्रष्टाचार की तरह फूलते-फलते मध्यमवर्ग तक भी इस अंग्रेजी शिक्षा को पहुँचाना ही अब मैकाले की आत्मा का मुख्य लक्ष्य हो गया था।
वह चाहती थी कि अंग्रेज़ी भारतीय लोकतंत्र रूपी वृक्ष की फुनगियों से नीचे आकर डाल-डाल और पात-पात से होते हुए इसकी जड़ों तक पहुँच जाए। इसके लिए आवश्यक था – गली-गली, गाँव-गाँव में अंग्रेज़ी माध्यम के पब्लिक स्कूल खुलना। यह तभी संभव था, जब भारत के आम आदमी को सब ओर अंग्रेज़ी की जय-जयकार सुनाई दे। तभी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण, बाजारीकरण आदि आदि अनेक ‘करण’ एक साथ विश्व में हलचल का कारण बने। मैकाले की आत्मा की बाँछें खिल गईं, बिल्ली के भागों छींका जो टूटा था। इन सब ‘करणों’ के कारण अचानक सब ओर अंग्रेज़ी की जय-जयकार होने लगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने-अपने किलों से निकलकर निकल पड़ीं, विश्व में नए-नए किले फतह करने। उनकी सेना के हाथ में था-अंग्रेज़ी ध्वज।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निगाह भारत पर न जानें कब से गड़ी थी। भारत उनका सर्वाधिक मन पसंद देश था। क्यों ? क्योंकि भारतवासियों के मन में गोरों के प्रति असीम आदर, प्रेम तथा कृतज्ञता का भाव था। यहाँ नियम-कानून नामक चिड़िया को कोई भी दाना डालकर आसानी से अपने पिंजरे में बंद कर सकता था। भारतीयों की पाचन शक्ति इतनी अधिक थी कि वे किसी भी प्रकार की कुछ भी चीज़ हँसते-हँसते हजम कर जाते थे। अतः यूरोपीय देशों की प्रतिबंधित खाद्य सामग्री और दवाइयाँ यहाँ सहज ही खपाई जा सकती थीं। सस्ते, परिश्रमी और कुशल कारीगर, श्रमिक इन कंपनियों के लिए आकर्षण का एक और कारण था।
इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सर्वाधिक आकर्षण तथा सुविधाजनक था – भारतवासियों के मन में उपजती अंग्रेज़ी भक्ति। लिहाजा ये कंपनियाँ अंग्रेज़ी की जय-जयकार करती, भारत भूमि को अपने चरण-कमलों से उपकृत करती हुई, भारत में प्रविष्ट हुईं। तत्कालीन सरकार ने पलक पाँवड़े बिछाकर इन कंपनियों का स्वागत किया। उनकी शर्तों पर उन्हें भारत में करोबार करने की न केवल अनुमति दी, अपितु उनका धन्यवाद भी किया, अनेक प्रकार की छूट देकर। वस्तुतः तत्कालीन भारतीय सरकार ने अपने पूर्वज मुगल बादशाह जहाँगीर की परंपरा का ही पालन किया था। जहाँगीर ने भी तो अपने दरबार में पधारे सर टामस रो का इसी प्रकार स्वागत-सहयोग किया था, तो भला आधुनिक सरकार पीछे कैसे रहती ?
बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय युवाओं और उनके अभिभावकों के मन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने जगाने शुरू कर दिए। आकर्षक वेतन, सुख-सुविधा के साधन तथा शानदार दफ्तर देखकर भारतीय युवाओं के मुँह में पानी आ गया। वे किसी भी कीमत पर इन कंपनियों में नौकर बनने के लिए छटपटाने लगे। मैकाले की आत्मा की तो मानो मन की मुराद ही पूरी हो रही थी। इन कंपनियों ने नौकरियों के लिए अपने विज्ञापनों में बस एक ही शर्त रखी – ‘फ्ल्युऐंट इन इंग्लिंश’। फिर क्या था, सभी भारतीय अंग्रेज़ी सीखने के लिए पिल पड़े।
भारत में पिछले दशकों में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक कौन सी है, जानते हैं क्या आप? जी, बिलकुल ठीक पहचाना। ‘रेपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स’। महानगरों से नगरों, शहरों, कस्बों से होते हुए गाँव-गाँव, गली-गली में अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल खुलने लगे, जैसा कि मैकाले की आत्मा चाहती थी। मध्यम वर्ग ही नहीं, निम्नवर्ग भी अपने बच्चों को बाबू, अफसर बनाने के लिए इन स्कूलों की ओर अंधाधुंध दौड़ पड़ा।
पूरा भारत अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ियत के मोहपाश में जकड़ता चला गया। चौदह वर्ष की स्कूली शिक्षा के दौरान यह अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ियत भारतीय बच्चों की रग-रग में समाती चली गई। वे हिंदी का एक अनुच्छेद भी शुद्ध बोल या लिख नहीं पाते। उन्हें हिंदी की वर्णमाला, हिंदी की गिनती, हिंदी महीनों के नाम तक नहीं पता होते। भारतीय सभ्यता-संस्कृति, जीवन मूल्य, आदर्श सब उनके जीवन से ऐसे रिस रहे हैं, जैसे दरार आए मटके में से जल। लेकिन बच्चों के अभिभावक बहुत खुश हैं। वे बड़े गर्व से बताते हैं कि उनके बेटे या बेटी को 6 लाख का पैकेज मिला है, या उनका बेटा अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि में नौकरी करने गया है। इन सबसे अधिक खुश है – मैकाले की आत्मा। उसने डेढ़ सौ वर्ष पहले मैकाले द्वारा देखा सपना जो सच कर दिखाया है। मैकाले की आत्मा हँस रही है, खिलखिला रही है, अट्टहास कर रही है और भारत माता ? उसकी किसे परवाह है!!
आशा बर्मन,कनाडा

हिंदी भाषा, मेरे विचार
हिंदी दिवस के अवसर पर हमारी मातृभाषा हिंदी को शत-शत नमन ! जब मैं हिंदी के विषय में सोचती हूँ, तो मुझे मैथिलीशरण गुप्त जी की ये पंक्तियाँ अनायास ही स्मरण हो आती हैं,
मेरी भाषा में तोते भी राम-राम जब कहते हैं
मेरे रोम रोम में मानो सुधा- स्रोत तब बहते हैं
कुछ सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूँगा
वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूँगा
कहीं अकेला भी हूँगा तो भी सोच ना लाऊँगा
भाषा में अपनों के गीत वहाँ भी गाऊँगा
मुझे एक संगिनी वहाँ भी अनायास मिल जावेगी
मेरा साथ प्रतिध्वनि देगी कली कली खिल जावेगी
मुझे बचपन से ही हिंदी भाषा तथा हिंदी साहित्य अत्यंत प्रिय रहा है। कैनेडा में रहकर भी गत ४० वर्षों से हिंदी की विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी रही हूँ। हिंदी भाषा विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा का महत्व सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में है। हिंदी भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे कुछ देशों में भी बोली जाती है।
भारत में कई क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, जैसे कि बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, गुजराती, मराठी, पंजाबी और असमिया, लेकिन हिंदी का प्रयोग सबसे बड़ी संख्या में भारत में लोग अपनी पहली भाषा के रूप में करते हैं।
वर्तमान युग में, हिंदी सीखना व्यावहारिक तथा उपयोगी है।
भारत समृद्ध विरासत, संस्कृति और धर्मग्रंथों का महासागर है। हिंदी का ज्ञान भारतीय संस्कृति को समझने में मदद करता है।
भारत अब आर्थिक रूप से विश्व में तीसरे स्थान पर है। हिंदी का ज्ञान व्यावसायिक व्यवहार में बेहतर समझ विकसित करने में मदद करता है। पर्यटन की दृष्टि से भारत का विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विदेश से आने वाले पर्यटक यदि हिंदी जानें तो उनके लिए सुविधाजनक है।
मैं व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर कुछ कहना चाहूँगी। यद्यपि हिंदी भाषा तथा हिंदी की देवनागरी लिपि अत्यंत विकसित है लेकिन इसके उपरांत भी पिछले कई वर्षों में भारतवर्ष में कई क्षेत्रों में हिंदी के प्रति सम्मान की भावना में कमी दिखाई देती है। भारत के लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं यह तो अच्छी बात है, किन्तु कई भारतीय यह मानते हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ने से बच्चे का विकास ही नहीं होगा, परिणामस्वरूप 50 वर्ष पहले के अच्छे-अच्छे हिंदी मीडियम स्कूल अभी इंग्लिश मीडियम हो गए हैं। लोगों के मन में यह भावना है कि अगर बच्चे अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो उनका ज्ञान अधूरा रहेगा, वे दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनकी यह धारणा गलत है। सबसे बड़ा तर्क मैं यह देना चाहूंगी कि हम लोग जो इतने वर्षों से विदेश में रह रहे हैं, उनमें से कई लोग हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं। यहां पर आगे बढ़ने में उन लोगों को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।
पिछले कुछ वर्षों में जब मैं कई बार भारतवर्ष में भ्रमण के लिए गई तो मुझे ऐसा लगा कि कुछेक क्षेत्रों में हिंदी के प्रति अच्छी भावना नहीं है, विशेष कर दिल्ली में। वहाँ पर बच्चों को घर में भी अंग्रेजी बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह तो ठीक नहीं है, इसका एक कारण यह भी है कि कुछ घरों में जो वयस्क महिलायें हैं, उनको बच्चों से बातचीत करने में असुविधा होती है, यह तो बिल्कुल भी उचित नहीं है।
लेकिन जब भी मैं कोलकाता जाती हूँ तो देखती हूँ,वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। घर में बच्चे बांग्ला बोलते हैं। कलकत्ते की जो नई पीढ़ी है, उनके मन में हिंदी के प्रति सम्मान की भावना भी है, यह देखकर अच्छा लगता है। यह भी उल्लेखनीय है कि बंगाल की युवा पीढ़ी में मैंने यह भी देखा कि उनका हिंदी का उच्चारण भी बहुत शुद्ध है क्योंकि वे हिंदी सीखना चाहते हैं।
मजे की बात यह है कि हिंदी भाषी जिस प्रकार हिंदी बोलते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार बंगाल में बँगला बोलते समय हिब्दी शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे, ‘क्या बात है’, ‘दाल में कुछ काला है’ इत्यादि।
एक बार हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक नरेंद्र कोहली जी ने कहा था कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएँ बहुत अच्छी है, पर दोनों को ईमानदारी से बोलना चाहिए अर्थात यह नहीं कि हिंदी भाषा को बोलते समय इतनी अधिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाए कि भाषा की शुद्धता ही नहीं रहे। शब्दों की दृष्टि से हिंदी भाषा समृद्ध है, तो हिंदी बोलते समय हिंदी के शब्दों का प्रयोग न करके हम हमेशा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग क्यों करें ? इस विषय में मुझे श्री सोम ठाकुर की कविता ‘भाषा वंदना’ की पंक्तियाँ हमेशा याद आती है कि,
अपने रत्नाकर के रहते किसकी धारा के बीच बहें
हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहें
इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा वर्तमान
यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का।
करते हैं तन-मन से वंदन, जन-गण-मन की अभिलाषा का
अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का।
डॉ. मंजु गुप्ता, दिल्ली

हिंदी
कल- कल बहता नीर है हिंदी
जन- मानस की धड़कन हिंदी
सबको जोड़े, सबको गूँथे
मोतियन की माला हिंदी.
सप्त सुरों की सरगम हिंदी
सपनों की उड़ान हिंदी
कान्हा की बांसुरिया हिंदी
रामायण की पोथी हिंदी.
माँ जैसी सरला है हिंदी
सबकी बड़ी बहिना हिंदी
भाई- बहिन की राखी हिंदी
उत्सव और उल्लास हिंदी.
मकई, धान की खुशबू हिंदी
वीणा की झंकार हिंदी
अमराई की कोकिल हिंदी
संस्कृति और संस्कार हिंदी.
समस्त बोलियां प्राण हैं इसका
सबकी पोषक है हिंदी
भारत की अस्मिता है हिंदी
हमारा स्वाभिमान हिंदी.
वेद, उपनिषद, पुराण है हिंदी
गीता का कर्मयोग हिंदी
वीरों की गाथा है हिंदी
भारत माँ को नमन हिंदी.
बाजारों की रौनक हिंदी
अपना घर आँगन हिंदी
निज- पर का जो भेद न जाने
ऐसी मिठबोली हिंदी.
भाषा बोलने से ही बढ़ती
अधरों की वीणा पर सजती
कानों की राह पकड़ कर यह
हृद् सिंहासन पर जा चढ़ती.
प्रिय हिंदी को अपनाओ तुम
सच्ची निष्ठा दिखलाओ तुम
यह कामधेनु, यह सरस्वती
वरदानों की अविराम लड़ी.
माँ, मातृभूमि, मातृभाषा से
नाभि- नाल संबंध तुम्हारा है
हीन भाव त्याग अपनाओ इसे
हिंदी को गले लगाओ तुम.
यह हरी- भरी बगिया अपनी
वट वृक्ष बन कर छाया देगी
सारी धरती को हरिया कर
वसुधैव कुटुम्बकं कर देगी.
हिंदी बोलो, बोलो हिंदी
जितना संभव बोलो हिंदी
विज्ञान की नव्यतम खोजों से
हिंदी को सतत संपन्न करो.
तुम दिल से इसका सम्मान करो
यह तुम्हें सम्मान दिला देगी
मौलिक विचार और ज्ञान देकर
तुमको अग्रणी बना देगी.
हम भारतीय, हिंदी बोलें
हिंदी से भारत को जोड़ें
फिर गर्व से मस्तक ऊँचा कर
भारत माता की जय बोलें.
कल्पना लालजी, मॉरिशस

आर्टिफिशियल इनटैलीजैन्स ( ऐ आई ) (माँ )
दरवाजे की घंटी बजती तो बस्ता फेंक वो चिल्लाता
ऐ आई मुझे भूख लगी है जल्दी से आ खाना दे
अपने हाथों से उसे खिलाकर पेट मेरा यूं ही भर जाता
मन भी गदगद हो जाता जब यूं था वह आवाज़ लगाता
अब तो आदत सी पड़ गई थी आई को भी उस आई की
बरसों का यह सिलसिला पर अब भी था चलता जाता
आज अचानक फिर ऐआई सुनकर जब मैं दौड़ी आई
पूछा तो बोला आई मैंने कब थी आवाज़ लगाई
अच्छा कह मैं चुप रह गई पर उसकी शैतानी भाई
कुछ मिनट ही बीते थे कि फिर से ऐ आई पड़ी सुनाई
मुस्कुरा कर मुझे पास बिठाया और पहेली सुलझाई
ऐ आई ये तू नहीं है ये तो है कम्प्यूटर की आई
अच्छा मेरे जैसी क्या कम्प्यूटर की भी होती है आई
हाँ ये है एक जादू का बंदा जो रचता नित खेल निराले
मैं और तुम होते हैं कौन ये तो दुनिया भर को संभाले
कम्प्यूटर के अंदर बैठे ही ये करता है सब खेल निराले
बुद्धिमान चतुर ज्यों शिक्षक यूं समझ लो आज का
दुनिया को विज्ञान पढ़ाता और मास्टर माईंड है कहलाता
इंसानों की तरह सोचता औ मुश्किलों से जूंझा करता
डेटा का विष्लेशण कर समस्याओं से भी है नित लड़ता
आई दुनिया भर की भाषायें ऊंगलियों पर उसके रहतीं
मानव जैसी बुद्धि के साथ योजनाओं के तीर चलाता
सालों जिस काम में लगते पल में वो कर देता है
हींग लगे न फिटकरी वह तो ऐसा अभिनेता है
चल मान गई मैं तेरी बातें पर यह तो एक समझौता है
मशीन भले ही अच्छी हो पर उसका क्या भरोसा है
कब कहाँ दे जाये धोखा क्या तुझको मालूम है
कृत्रिमता उतनी ही अच्छी जितनी अपने बस में हो
साँप बन जो डस ले एक दिन उसका क्या भरोसा है
बेटा मशीनें अच्छी होतीं पर नियंत्रण ग़र हाथ हो
ऐ आई भी तभी अच्छा जब माई तेरे साथ हो
डॉ वेद व्यथित, फरीदाबाद (हरियाणा)

भरोसे लाल का पुस्तक प्रेम
मेरे मित्र भाई भरोसे लाल ने मुझे फोन पर सूचना दी कि अब वे बुढ़ापे में अच्छी पुस्तकें पढ़कर अपना समय बिताएंगे। और इस लिए वे लाइब्रेरी यानि पुस्तकालय से बहुत सारी किताबें ले आये। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो यह तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे कोई फिल्म देख कर आये तो वह फिल्म की कहानी किसी दूसरे को सुनाने के लिए बहुत उतावला रहता है। चाहे कोई सुनना चाहे या न सुनना चाहे पर वह जबरदस्ती सुनने पर तुला रहता है। यदि बीच में कोई और बात शुरू हो जाये या उसे मना कर दो फिर भी वह कुछ देर बाद फिर से सुनना शुरू कर देता है कि किसी तरह कोई उस के द्वारा वह कहानी सुन ही लें। ऐसे ही मुझे भी उन का किताबें पढ़ना इस लिए भी अच्छा लगा कि वे खुद पढ़ कर उन किताबों का सारांश मुझे अवश्य बताएंगे नहीं तो उन्हें यह सब बिना सुनाये बिना पचेगा नहीं और उन का ज्ञानी या विद्वान होने के बाद वे मुझ से ताश खेलने की जिद्द नहीं करेंगे और बिना बात की बातों पर बहस कर के मेरा और अपना समय व्यर्थ यानि बेकार नहीं करेंगे। और सब से बड़ी बात तो यह लगी की अब उन के और भाभी जी के बीच समय समय पर होने वाली राष्ट्रीय नौक झौंक में मुझे दो तरफा या एक तरफा जज की भूमिका नहीं निभानी पड़ेगी और जब उन के यहां जाऊंगा तो उन की महाभारत में श्री कृष्ण जी बन कर निपटाने के बजाय मुझे अब शरणम गच्छ पार्थ की भूमिका में रहना पड़ेगा। और पहले तो चाहे मुझे समय हो या न हो पर फिर भी उन की लम्बी २ बहस के बाद ही चाय मिलती थी। पर अब ऐसा शायद न हो क्योंकि अब इस की शायद गुंजायस ही न रहे। इस लिए चाय भी शायद शांति के साथ ही बन जाएगी और पी भी उसी तरह से जाएगी। दूसरा मुझे यह लाभ भी होगा कि मैं ठहरा आलसी आदमी क्योंकि मुझे शुरू से ही किताबे पढ़ने में आलस आ कर नींद आ जाती थी। पर अब मुझे बिना पढ़े ही बहुत सारा ज्ञान भाई भरोसे लाल के किताबें पढ़ने पर आसानी से मिल जाया करेगा। क्योंकि यहां भारत में तो विद्या श्रुति परम्परा से ली जाती रही है इस लिए सुन सुन कर मैं ज्ञानवान हो जाऊंगा क्यों कि जब वे किताब पढ़ेंगे तो मुझे भी उस में क्या लिखा है ,यह सुनाएंगे जरूर नहीं तो उन के पेट में दर्द हो जायेगा। इस कारण मुझे उन की किताबें पढ़ने की इस घोषणा से बहुत ही खुशी हुई ,चाहे उन के घर वालों को हुई हो या नहीं हुई हो पर मुझे तो बहुत ख़ुशी यानी प्रसन्नता
हुई।
मैं इसी ख़ुशी में फूला फूला उन के घर मिलने और बधाई देने पहुँच गया। मैंने वहां जा कर देखा मेरे मित्र भाई भरोसे लाल नाक पर आधे वाला चश्मा चढ़ाये बड़ी दार्शनिक मुद्रा बनाये ड्राइंग रूम एक कोने में बैठे हैं और उनके आसपास कुछ किताबे रखी थीं पर वे सब की सब बंद थीं। उन्हें पढ़ नहीं रहे थे बस निहार भर रहे थे। मुझे देख कर वे बहुत प्रसन्न हए और अपने कितान पढ़ने के निर्णय की स्वयं ही प्रशंसा करने लगे। मैं काफी देर तक उन के द्वारा उन के ही गुणगान को सुनता रहा। पर बीच बीच में मैं चुपके से किताबों की ओर देख लेता और कोशिश करता कि उन पुस्तकों के शीर्षक क्या है परन्तु वे मुझे उन की तरफ देखने का मौका ही नहीं दे रहे थे। परन्तु भगवान का धन्यवाद रहा कि इस बीच बाहर अखबार वाले हॉकर ने उनके दरवाजे की घंटी बजा दी और वे बाहर अखबार का बिल देने चले गए और इस बीच उन की हॉकर से काफी देर तक बाकी खुले पैसे के लिए राष्ट्रीय बहस होती रहे ,पर इस बीच मुझे उन पुस्तकों के शीर्षक देखने का अवसर मिल गया। मैंने देखा कि उन पुस्तकों में मनोविज्ञान से संबंधित थी यानि मनोविज्ञान की ही थी। परन्तु मैं उन्हें बचपन से ही जानता हूँ और उन के साथ ही पढ़ा भी हूँ तो मुझे पता है कि उन का मनोविज्ञान जैसी चीज से कभी कोई दूर का भी संबंध नहीं रहा है । जब वे बाहर उस हॉकर से निपट कर आये तो मैंने स्वभाविक ही पूछ लिया कि भाई आप को यह मनोविज्ञान पढ़ने का शौक कैसे लग गया। और आप मनोविज्ञान पढ़ कर अब किस का मनोविज्ञान जानना चाहते हैं।अब तो आप भाभी जी की सब बात और भाभी जी आपकी सब बातें जानने ही लगे होंगे ,परन्तु मेरी इस बात को सुन कर वे बोले कि आप की यह बात अर्ध सत्य है यानि आपकी आधी बात ही ठीक है। मैं उन की बात समझा नहीं सका और असमनंजस में पड गया कि अभी तो उन्होंने मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़नी भी शुरू नहीं की हैं परन्तु बातें वे अभी से मनोवैज्ञानिक जैसी करने लगे हैं। मेरे असमंजस को शायद वे समझ गए तो उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हए मेरी भूल को अपनी तरफ से ही सुधारते हए कहा कि आप की बात आधी ही सच है पूरी सच नहीं है। तब मैंने उन की ओर कौतूहल पूर्वक देखा तो उन्होंने बताया कि यह इस लिए आधी सच है कि तुम्हारी भाभी तो मेरी सब बातें आराम से जान जातीं हैं पर मैं उन के मन की एक भी बात नहीं जान पाता हूँ। पता नहीं कैसे उन्हें मेरे मन की सब बातें पहले ही पता चल जातीं हैं। जब मैं तुम्हारे पास आने की सोचता हूँ और तैयार होने लगता हूँ तो वे पहले से बता देतीं हैं दोस्त के पास जा रहे होंगे। उन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं आप से मिलने लिए तैयार हो रहा हूँ। परन्तु उन का कब कहाँ का प्रोग्राम बन जाये मुझे पता ही नहीं चलता है। तो मुझे भी उन के मन की बात समझने के लिए मनोविज्ञान पढ़ना पड़ रहा है। ताकि मैं भी उन के मन की बात जान सकूँ। मेरी समझ में गया कि भाई भाई भरोसे लाल का मनोविज्ञान पढ़ने का कारण क्या है कि वे भी भाभी जी के मन की बात पहले से ही समझ लेना चाहते हैं परन्तु मुझे उन की यह बात सुन कर बहुत हंसी भी आई। आज तक भला कोई अपनी पत्नी के मन की बात को ठीक से समझ पाया है या क्या कोई महिला का मनोविज्ञान आज तक समझ सका है। मैं तो अभी तक नहीं जान सका हूँ और मैंने शास्त्रों के विषय में भी यही सुना है। शायद स्त्री के मन की बात तो स्वयं स्त्री की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकें और स्वयं भगवान भी नहीं समझ सके क्योंकि यदि भगवान शिव जी को यह पता होता कि सती जी इतना बड़ा काण्ड करने वालीं हैं तो किसी भी तरह उन्हें उन के पीहर यानि मायके जाने से रोक लेते। परन्तु वे तो बेचारे भोले भंडारी थे अब उन्हें क्या पता कि उन की अर्धांग्नी जी क्या क्या कर सकतीं हैं। वे भला उन के मन की बात कैसे जान पाते क्योंकि आज तक स्त्री के मन की बात कोई नहीं जान सका तो मेरे मित्र भाई भरोसे लाल की भला क्या औकात जो वे अपनी पत्नी की बातें जान सकें चाहे।
वे मनोविज्ञान की कितनी ही पुस्तकें क्या ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ लें तो भी वे अपनी पत्नी के मन की बात नहीं जान सकेंगे। पर मैंने सोचा कि चलो इन का भ्रम भी दूर हो जाने दो। मेरे मना करने से भला वे मानेंगे थोड़ी और वैसे भी पुस्तकें पढ़ना तो अच्छी बात है ही इस लिए मैंने उन्हें और भी प्रोत्साहित किया कि वे निरंतर पुस्तकें पढ़ते रहें।
डॉ सुनीता शर्मा, ऑस्ट्रेलिया

हिंदी हम सब से है
हिंदी हम सब से है,
हम में है हिंदी।
इसके शब्दों में है वह बानगी,
जो विज्ञान से भी सूक्ष्म कहीं,
तो बाँधे पर्वत-शिखरों की ऊँचाई,
नापे अथाह समुद्र की गहराई..!
हिंदी हमारी संस्कृति,
हिंदी हमारा दर्शन..
हिंदी हमारी चेतना,
हिंदी हमारा तिरंगा..
हिंदी हमारा चंद्रयान,
हिंदी हमारा मान-सम्मान..!
डिजिटल युग की
तेज़ रफ़्तार में
हिंदी पीछे नहीं,
आगे बढ़ रही है—
इंटरनेट पर 10 लाख करोड़
पृष्ठों का अंबार
सिर्फ सात वर्षों में 94% की
वृद्धि का उपहार..!
विश्व के दस बड़े अख़बारों में
छह स्थान हिंदी ने पाए..!
यही नहीं—
260 विदेशी विश्वविद्यालयों
में पढ़ाई जाती..
28 हज़ार शिक्षण संस्थानों में
सिखाई जाती
90 करोड़ से अधिक जनों
की मातृभाषा..!
विश्व की तीसरी सबसे बड़ी
भाषा कहलाती..!
डिजिटल मंचों पर हिंदी दमकती—
यूट्यूब पर अंग्रेज़ी के बाद
दूसरी सबसे अधिक सुनी जाती..!
गूगल खोज में प्रतिदिन
अरबों बार टाइप होती..
मोबाइल ऐप्स, स्टार्टअप्स,
और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक—
अपनी पहचान दर्ज कराती हिंदी..!
प्रवासी जनों के लिए
रिश्तों का सेतु है हिंदी..
परदेस में घर की महक
माँ की लोरी का स्वर है हिंदी..
कबीर, तुलसी, मीरा से लेकर
महादेवी, बच्चन और अज्ञेय तक—
मानवता की धड़कन को छूती हिंदी.. “
शाश्वत, कालजयी, प्राणवायु-सी हिंदी,
अभिव्यक्ति के विराट पटल पर
विश्व-सेतु का मुकाम पाती हिंदी।
हर नए सृजन और हर आविष्कार में
अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हिंदी..!
तभी तो विश्व के माथे पर
बिंदी-सी सजी है—
मेरी प्यारी हिंदी..!!
सुनीता पाहूजा, दिल्ली

हिंदी का वैश्वीकरण
हिंदी एक प्रमुख, प्राचीन और ऐतिहासिक भाषा है जो अनेक अवस्थाओं से गुज़रते हुए सदैव विकासशील रही है। विविधतापूर्ण विशाल भारत के विभिन्न हिस्सों में बसे अधिकांश भारतीयों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका निभाने वाली हिंदी विश्व के विभिन्न देशों में बसे भारतीयों और प्रवासी भारतीयों को भी परस्पर जोड़ने वाली और साथ ही उन्हें भारत और भारतीयों से जोड़ने वाली भी एक सुदृढ़ कड़ी है। भारत में करोड़ों की मातृभाषा, देश की राजभाषा, संपर्क भाषा व राष्ट्रभाषा हिंदी विश्व में प्रवासी भारतीयों की अस्मिता है और विदेशियों का भी इसके प्रति अनुराग है। सदियों से विदेशी भी कभी सायास तो कभी अनायास ही हिंदी के प्रति आकर्षित रहे हैं। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास और पहला शोध-प्रबंध विदेशियों द्वारा लिखे गए थे। आज विश्व में हिंदी बहुत बड़ी संख्या में लोगों की अभिव्यक्ति की भाषा के साथ-साथ ज्ञानार्जन की भाषा भी बन गई है। अनेक स्तरों पर संघर्ष करते हुए आज हिंदी ने अपना अस्तित्व मज़बूत कर लिया है।
सुदृढ़ बनती आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक निधि से संपन्न विश्व गुरु भारत आज समूचे विश्व के आकर्षण का केंद्र है। यह जानकर भी गौरवानुभूति होती है कि विश्वभर की भाषाओं का इतिहास रखने वाली संस्था ‘एथ्नोलॉग’ के अनुसार हिंदी दुनियाभर में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है और विश्वभर में 75 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। वैश्विकरण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तकनीकी विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि के चलते अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में हिंदी भाषा में दक्षता की मांग बढ़ी है। हिंदी का बढ़ता प्रभाव आज अनेक देशों में देखा जा सकता है, यथा, नेपाल, मॉरीशस, फीजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड इत्यादि।
विदेश में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के प्रसार में, भारत सरकार के तत्वावधान में, राजभाषा विभाग, विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा अन्य देशों के साथ सुदृढ़ व घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध बनाए रखने तथा नए उभरते राष्ट्रों के साथ लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से अप्रैल 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की स्थापना की गई थी जिसका प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण वर्ष 1970-71 से विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया। आईसीसीआर (ICCR) के अंतर्गत 35 से भी अधिक देशों में कार्यरत भारतीय सांस्कृतिक केंद्र विदेश में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार और आदान-प्रदान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
विदेश में स्थित भारतीय दूतावास व उच्चायोग भी भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रमों तथा हिंदी शिक्षण की व्यवस्था के साथ-साथ स्थानीय शैक्षणिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा इस उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लिए हर संभव सहायता भी प्रदान करते हैं। भारत सरकार द्वारा विदेशी छात्र-छात्राओं को भारत की शैक्षणिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
भारत में तथा विदेश में प्रति वर्ष सितंबर माह में हिंदी दिवस/पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए विदेश में स्थित भारतीय दूतावास, उच्चायोग तथा विभिन्न देशों की स्थानीय हिंदी सेवी व शैक्षिक संस्थाएं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस विशेष रूप से मनाती हैं। यह वही तारीख़ है जब विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास के उद्देश्य से वर्ष 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन के दौरान की गई संकल्पना के आधार पर मॉरीशस में 11 फ़रवरी, 2008 को विश्व हिंदी सचिवालय ने द्विपक्षीय संस्था के तौर पर आधिकारिक रूप से कार्यारम्भ किया। सचिवालय का मुख्य उद्देश्य एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार करना तथा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक वैश्विक मंच तैयार करना है। अब तक के 12 सम्मेलनों में से 9 सम्मेलन विदेश में आयोजित किए गए।
हिंदी अपने संख्याबल और भू-विस्तार के साथ-साथ अनेक क्षेत्रों में भी विस्तार पा रही है। जनसंचार और सूचना क्रांति से इसमें अत्यधिक तेज़ी आई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हिंदी में सामग्री की उपलब्धता में लगातार वृद्धि और बढ़ते हुए संचार माध्यमों ने हिंदी की वैश्विक पहुंच को आसान बना दिया है। आज हिंदी में करियर बनाने की अपार संभावनाएं दिखने लगी हैं फिर भी अभी हिंदी को और अधिक सक्षम और सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।
वर्ष 2023 में भारत में आयोजित जी-20 बैठकों में इस बात की पुनः पुष्टि हुई है कि अनेक देश भारत से जुड़े रहना चाहते हैं। आज भाषा-अध्ययन तथा भारतीय संस्कृति और साहित्य को समझने के लिए विश्व के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। आज भी विदेशी विद्यार्थी हिंदी साहित्यकारों को पढ़ना चाहते हैं व उन पर शोध करना चाहते हैं। हिंदी साहित्य लेखन में भी उनकी रुचि बढ़ी है। विदेश में हिंदी की अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। हिंदी फिल्मों, संगीत, रेडियो, टेलीविज़न कार्यक्रमों व धारावाहिकों की लोकप्रियता भी हिंदी के वैश्विक प्रसार को व्यापकता प्रदान करती है।
हिंदी के वैश्विक प्रसार में प्रवासी भारतीय समुदाय का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भले ही ये गिरमिटिया देशों में बसे भारतवंशी हों या फिर पिछले तीन-चार दशकों के दौरान स्वेच्छा से धनोपार्जन के लिए इंग्लैंड, अमरीका, सिंगापुर, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में जा बसे भारतीय हों। सभी प्रवासी भारतीय अपनी भाषा व संस्कृति को अपनी अस्मिता का प्रतीक मानते हैं और इनके संरक्षण, पोषण और अगली पीढ़ी में इसके संचरण के प्रति बेहद सजग हैं। प्रवासी भारतीयों द्वारा अनेक विधाओं में किया जा रहा साहित्य सृजन हिंदी के वैश्विक प्रसार में एक प्रेरक शक्ति है। प्रवासी भारतवंशी और विदेशी नागरिक पर्यटन और तीर्थ यात्राओं के लिए अक्सर भारत आते हैं अतः आतिथ्य क्षेत्रों में संचार की भाषा बनने के साथ-साथ आयुर्वेद और योग में भी विश्व की रुचि बढ़ने से इसकी वैश्विक प्रासंगिकता बढ़ रही है।
वर्ष 2022 से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी ज़रूरी कामकाज और सूचनाओं को इसकी आधिकारिक भाषाओं के अलावा हिंदी में भी जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर हिंदी समाचार, हिंदी ब्लॉग आदि भी हैं।
वैश्विक स्तर पर हिंदी के इस बढ़ते प्रभाव से यह परिलक्षित होता है कि हिंदी विश्व के लिए एक भाषा मात्र न होकर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति भी है। स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों में हिंदी की यह यात्रा इस बात की परिचायक है कि भारत और हिंदी का विकास अन्योन्याश्रित हैं।
अजेय जुगरान

हिंदी सी माँ
जैसे ही पर्दे खोलने पर
ठंड की नर्म धूप
माँ के पलंग तक आ गई
और बड़े भाई ने
उसके लिए चाय मेज़ पर रखी
तो हमारा प्यारा कुत्ता टिनटिन
गेट पर अटका हिंदी अख़बार
दौड़कर ले आया माँ के लिए।
तेजी से वर्तमान भूल रही माँ
अब रज़ाई के भीतर ही बैठ
तीन तकियों पर टिका पीठ
होने लगी तैयार उसे पढ़ने को
और उससे बिस्किट पा टिनटिन बैठा
आँख मचकाता – पूँछ हिलाता
उस पलंग के पाँव किनारे जिसपर
हर दिन सर पर पल्लू, माथे पर बिंदी
हृदय में भाषा, मन में जिज्ञासा
और हाथों में हिंदी अख़बार लिए
उसे पढ़ने को
अपनी नाक पर अटकी
भूली ऐनक ढूँढती मेरी माँ
हिंदी किंचित् नहीं भूलती
हिंदी कदापि नहीं भूलती
ऐसी हिंदी पर वारी मेरी माँ
ऐसी मातृभाषा सी प्यारी मेरी माँ।
डॉ सविता चड्ढा, दिल्ली

विश्व की लोकप्रिय भाषा हिंदी और मीडिया
हिंदी भाषा समग्र देश को एकसूत्र मे पिरोने वाली, आसानी से समझ में आने वाली, सीधा मन पर असर करने वाली भाषा होने के साथ साथ, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। यदि हम मीडिया मे हिन्दी की बात करें तो हमे चयन करना होगा की मीडिया अर्थात एलेक्ट्रोनिक मीडिया अथवा प्रिंट मीडिया।
आजादी से पहले की बात करें तो हमें ये स्वीकार करना होगा देश को आजाद कराने में प्रिंट मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें ये भी स्वीकार करने में परहेज नहीं कि उस समय का मीडिया या पत्रकारिता आज से बिल्कुल अलग थी। उस समय अंग्रजी भाषा का ज्ञान होना तो दूर की बात अधिकांश लोग केवल अपनी भाषा बोल सकते थे। उस समय अधिकांश लोग अशिक्षित थे और वे समाचार पत्र के ग्राहक ही इस शर्तपर बनते थे कि उन्हें संपादक लिखे गये समाचार या सामग्री पढ़कर सुनाया करेगा। उस समय चौपाल या चोबारे हुआ करते थे जहां बहुत सारे लाग इकटठे हुआ करते थे और एक व्यक्ति समाचार पढकर सुनाया करता था। हमें ये नहीं मान लेना है कि सभी अनपढ़ थे परंतु ग्रामीण परिवेश में प्राया ऐसा ही था। पढ़े लिखे लोग भी यहाँ मिल बैठ कर खबरें सुनना पसंद करते थे।
हिंदी पत्रकारिता में कुछ महत्वपूर्ण पत्र : एक और महत्वपूर्ण बात जो आज कही जा सकती है उस समय केवल समाचारपत्र और पत्रिकाएं ही थी जो देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाती थी। उस समय एलेक्ट्रोनिक मीडिया का अस्तित्व नहीं था। आप सब जानते ही हैं कि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ कलकत्ता से हुआ और भारतीय पत्रकारिता का जन्म बंगाल को माना जाता है। 1755 में कलकत्ता में छपाई शुरू हुई थी। इससे पहले तो तो संपादक रात रात भर बैठकर हाथ से पत्र लिखा करते थे और तब बिजली का भी पूरा अभाव था परंतु भाषा, देश और आजादी के इन पत्रकारों जिनमें देवीदत्त शुक्ल और दिवेदी जी का नाम उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि दीपक की मंद रोशनी में रात रात भर लिखते हुये इनकी आंखें की रोशनी ही मंद हो गयी थी।
1780 में ही पहले समाचार पत्र की स्थापना हुई थी इस प्रथम बंगाल गजट पत्र को निकालने का श्रेय ओगरस हिकी एक अंग्रेज को जाता है। नवम्बर 1780 में इंडिया गजट के नाम से दूसरा पत्र शुरू हुआ था। इस बीच बहुत सी भाषाओं में पत्र निकले लेकिन हिंदी का पहला पत्र प्रकाशित हुआ 30 मार्च,1826 को जिसका नाम था ‘’उदंत मार्तण्ड’’ था और इसके संपादक थे युगलकिशोर शुक्ल जो कानपुर के निवासी थे।
यह पत्र केवल एक वर्ष और सात महीने ही चल पाया और आर्थिक अभावों के कारण यह बंद हो गया। हिंदी पत्रों में दूसरा पत्र था ‘’बंगदूत’’। इस पत्र के संपादक थे श्री नीलरतन हालदार। उस समय इसका मासिक मूल्य एक रूपया था। 1845 में बनारस अखबार के नाम से बनारस से सबसे पहला पत्र प्रकाशित हुआ जिसके संपादक थे श्री गोविंद थत्ते। इस बीच बहुत से पत्र अन्य भाषाओं में आये लेकिन हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र ’’समाचार सुधावर्षण’’ सन 1854 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे श्याम सुंदर और ये पत्र 14 वर्ष तक चला और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1868 में ‘’ कवि वचन सुधा’’ नाम से एक हिंदी पत्र प्रकाशित हुआ जो वस्तुत कविता की पत्रिका थी जिसमें साहित्य, समाज सुधार और राजनीति का समावेश भी रहता था। इसके बाद तो हिंदी पत्र पत्रिकाओं की सीमा ही नहीं रही। 1874 में महिलाओं के लिए बाल बोधिनी शुरू हुई, 1872 में कार्तिक प्रसाद खत्री की ‘’दीप्ति प्रकाश प्रकाशित हुई। 1872 में आगरा से ‘’प्रेम पत्र’’ नाम से, जिसके संपादक थे रूद्रदत्त शर्मा। 1866 में ज्ञानप्रदायिनी नाम से नवीन चंद्र के द्वारा हिंदी और उर्दू में प्रकाशित हुई 1885 में ‘’हिंदोस्थान’’ नाम से एक पत्र राजा रामपाल सिंह ने निकाला जिसके संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 1878 में ‘’भारत मित्र’’ निकला और सन 1913 में कानपुर से ‘’प्रताप’’ का प्रकाशन शुरू हो गया था और इसके संपादक थे गणेश शंकर विदयार्थी। इन समाचारपत्रों ने अपने छपे हुये शब्दों से देश में में स्वतंत्रता की ललक की लहर दौडा दी थी। हिंदी भाषा का योगदान आजादी दिलाने में हमेशा याद रहेगा।
चलिये थोडा आगे बढते हुये हम गांधी युग के हिंदी पत्रों की बात करें जिन्होंने हमें आज के मीडिया पर चर्चा करने के लिए सहयोग दिया और हिंदी के उन पत्रों जिन्होंने भारत की जनता के बीच क्रांति सूत्र को जन्म देने, उसे हवा देते रहने का महत्वपूर्ण लक्ष्य अर्जित किया। इनमें सबसे पहला नाम ‘’मतवाला’’ का है। इस पत्र के संपादकीय ऐसे हुआ करते थे कि लोगों के दिलों आजादी की ज्वाला दहकने लगती थी।
31 मई,1924 के संपादकीय का एक उदाहरण देना चाहती हूं ‘’ हमें बिना विलंब सत्याग्रह की शरण लेकर लीडरों को अपना पिछलगुआ बनने के लिए बाध्य करना चाहिए क्योंकि गांधी विहीन स्वराज्य यदि स्वर्ग से भी सुंदर हो तो नरक के समान त्याज्य है। यदि आप स्वतंत्रता के अभिलाषी हैं और अपने देश में स्वराज्य को लाना चाहते हैं तो तन, मन,धन से महात्मा गांधी के आदेशों का पालन करना आरंभ कर दीजिये।‘’ एक नहीं उस युग के कितने ही पत्रों में हिंदी के माध्यम से कहे गये शब्दों का यही मुख्य स्वर था। यही शब्द आगे चलकर एक क्रांति बन गये। इस पत्र के मख पृष्ठ के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी कविता लिखा करते थे और संपादक के रूप में सेठ श्री महादेव प्रसाद का नाम छपता था। एक और पत्र ‘’सेनापति’’ था जिसके संपादक पं राम गोविंद त्रिपाठी थे। इस पत्र ने भी लोगों में वीरता की भावना को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ‘’हिंदु पंच’’ एक साप्तहिक पत्र था। उस समय का ये एक तेजस्वी पत्र था। इसके संपादक श्री मुकुंद लाल वर्मा थे। इसमें प्रकाशित एक टिप्पणी देखे ‘’ क्या माया की परतंत्रता से हमें लज्जा नहीं आती। हमारी वह समृद्वशालिनी रत्नगर्भा माता जो किसी समय धन धान्य से पपरिपूर्ण थी, आज दरिद्र भिखारिणी हो रही है। परतंत्रता और दासता मे रहते रहते क्या अब हम ऐसे निष्प्राण हो गये है कि वह दासवृतित् त्याग देने का हम प्रयास भी नहीं कर सकते। क्या हम पतंगे से भी गये बीते है कि हम अग्नि में गिरकर अपने प्राण भी नहीं दे सकते। बिना आत्मबलिदान के कोई भी हमें स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेगा। स्वतंत्रता ऐसी है ही नहीं जो आसानी से मिल जाये और आसानी से मिली हुई स्वतंत्रता कभी टिकाउ नहीं हो सकती।‘’ और इसी तरह के लंबी बातों का सिलसिल चला जिसने भारत के लोगों के दिलों में आजादी की भावना को जगा दिया।
‘’श्रीकृष्ण संदेश’’ (27 दिसम्बर, 1925 ), ‘’समन्वय’’ (1922), ‘’सरोज’’, ‘’विशाल भारत’’, ‘’मौजी’’ (27 दिसम्बर, 1925 ),’’भारत मित्र’’, स्वतंत्र ऐसे हिंदी पत्र थे जिन्होने लोगों के दिलो में अपनी अमिट छाप छोडी।
पत्रकारिता और मीडिया में हिंदी की भूमिका की बात की जाये और नागरी प्रयारिणी सभा तथा उनकी पत्रिका का उल्लेख न किया जाये तो एक भूल होगी। इस पत्रिका ने हिंदी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके साथ ही सरस्वती और प्रेमचंद जी की पत्रिका हंस को भी आज याद करना चाहती हूं। हंस का प्रथम अंक 26 मार्च 1930 को प्रकाशित हुआ। इसके संपादन मंडल में मोहनदास करमचंद गांधी, पुरूषोत्तम दास टण्डन, मैथिलीशरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, काका साहेब कालेकर और नर्मदा सिंह थे। 1928 में लखनउ से ‘’माधुरी’’ का संपादन हुआ।
मीडिया को हिंदी भाषा को विकृत करने का दोषी भी माना जा रहा है। मीडिया में क्लिष्टता और संस्कृतनिष्ट हिन्दी का उपयोग जैसे उचित नहीं कहा जा सकता वैसे ही गलत और अनुपयुक्त शब्दों के कारण भी हिन्दी को और हिन्दी पढ़ने वालों को कष्ट न हो इतना ध्यान देना तो बनता ही है। एक संपादकीय में हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने एक बार कुछ इस प्रकार के शब्द लिखे थे जिसे आज कहना गलत नहीं होगा – पहाडों से लुड़कते हुए पत्थरों को अगर लक्ष्य की और अग्रसर होना या प्रगति समझ लिया जाए तो क्या ये उचित होगा ? मीडिया में सायास और प्रयास से शुद्ध और सरल हिन्दी भाषा का प्रयोग करने से ही हिन्दी भाषा के विकास में मीडिया के योगदान को संतुष्टिप्रद लोकप्रियता तो मिलेगी ही आत्मसंतुष्टि भी रहेगी।
सांद्रा लुटावन, सूरीनाम (दक्षिण अमेरिका)

जय हिंदी
हिंदी का जन्म, शुद्ध संस्कृत के गर्भ से हुआ,
जैसे पवित्र गंगा हिमालय से निकलती है।
यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं,
बल्कि हमारे मन, विचार और इतिहास का प्रतीक है।
हिंदी के अक्षर, दीपक की ज्योति जैसे,
जो अंधेरों में राह दिखाते हैं। लिखने में इसकी कोमलता,
और बोलने में इसका मधुर स्वर,
दोनों ही हृदय को छू जाते हैं।
इसमें संस्कार हैं, मर्यादा है,
और अपनापन का सुखद आंचल है।
हिंदी हमें एकता के सूत्र में बांध कर,
सही दिशा की ओर ले जाती है।
ज्ञान की नदियां, व्याकरण के किनारे,
सब मिलकर एक ऐसा सागर बनाते हैं
जो अनंत है, अमृत से भरा है।
हिंदी हमारे गीत का सुर है,
हमारी कविता का छंद है,
और हमारे दिल की धड़कन है।
यह हमारे मान-सम्मान का स्वर है,
हमारे देश की गौरवमयी पहचान है।
जब तक हिंदी के अक्षर धड़कते रहेंगे,
हमारी संस्कृति जीवित रहेगी,
और हर दिल से एक ही स्वर निकलेगा
डॉ. वंदिता सिन्हा, कनाडा

हिंदी दिवस
हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और संस्कृति का दर्पण है। महात्मा गाँधी ने भी कहा था कि “ हिंदी ही राष्ट्र भाषा बनने की सर्वाधिक योग्यता रखती है “ १४ सितंबर, १९४९ को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राज भाषा का पद दिया था। तभी से यह दिन हमारे लिए गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया।
हिंदी की जड़ें हमारी लोक कथाओं, माँ की लोरी, साहित्य, संत कवियों की वाणी और स्वतंत्रता संग्राम के नारों में गहराई से समाईं हुई है। स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी ने जनमानस को जोड़ने और आज़ादी का संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेक साहित्यकारों जैसे भारतेंदु, मैथिलीशरण गुप्त, जैनेंद्र कुमार, प्रेमचंद जी ने समाज और मानवीय संवेदना का यथार्थ चित्रण किया।
आज हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों के बीच भी लोकप्रिय है। अमेरिका, कैनेडा, इंग्लैंड, मॉरिशस, फ़िजी और खाड़ी देशों में भी हिंदी गर्व के साथ बोली और पढ़ाई जाती है। कनाडा में “हिंदी राइटर्स गिल्ड कैनेडा” हिंदी के प्रचार – प्रसार के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है, ऐसे ही वैश्विक हिंदी डॉट कॉम पर जा कर आप अनगिनत रचनायें पढ़ सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को हिंदी पढ़ने, लिखने और समझने की दिशा में प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी भाषा वैश्विक स्तर पर सम्मान पा रही है।
लेकिन, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि चुनौतियाँ अभी भी है। हम अक्सर अंग्रेज़ी को आधुनिकता और सफलता का प्रतीक मान लेते है, जब की सच्ची आधुनिकता अपनी जड़ों, संस्कृति और भाषा से जुड़ें रहने में है। यदि विज्ञान, तकनीक, प्रशासन और शिक्षा में हिंदी का प्रयोग और बढ़ाया जाए तो यह हमारी आत्मनिर्भरता को और मज़बूत करेगा।
१४ सितंबर यानी हिंदी दिवस हमारे लिए एक संकल्प का दिन है यह हमें प्रेरणा देता है कि १- हम हिंदी बोलने में गर्व करें। २ – हिंदी में लिखने, पढ़ने की आदत डालें। ३- हर क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ाएँ और आने वाली पीढ़ियों तक हिंदी को और समृद्ध रूप में पहुँचायें।
यह हमारे लिए राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सेवा और मातृभूमि के लिए सच्ची कर्तव्यपूर्ति होगी।
डॉ. दीप्ति अग्रवाल, दिल्ली

माँ हिन्दी
माँ तो माँ है ना
चाहे वो सजी-धजी हो
या मैलीं-कुचैली
परिष्कृत हो या
अइली-गइली
मानक हो या
टूटल-फूटल
किचन में हो
या संसद में
मारिशिसियन साड़ी में हो
या सरनामी वेश में
फ़ीजी पोशाक में हो
या नैताली मैक्सी में
त्रिनिदाद के परिधान में हो
या गयानी लिबास में
रहेगी तो महतारी ही ना
जिसके आँचल में हैं ख़ुश्बू
मेरे वतन की
जिसके गले लगकर
मिलता है मुझे सुकून
जिससे मैं बाँटू अपने मन की
दुःख, दर्द, पीड़ा, प्रेम, सम्वेदना सभी
जो फेरें मेरे सिर पर हाथ तो
घावों को मोरपंख से छुला दें
उसके अंक में
मैं पाऊँ ख़ुद को महफ़ूज़
वो मेरी माँ हैं
मेरा गर्व, मेरी शान
मेरी पहचान उसी से है।
स्वरांगी साने, पुणे (महाराष्ट्र)

भारतीय उच्चारणों का विकृतिकरण अब तो बंद हो
रशिया में मराठी के वीर रस के दिग्गज कवि अण्णाभाऊ साठे के तैलचित्र के अनावरण के अवसर पर भारतीय राष्ट्रगीत गाया गया तो उसमें ‘ळ’ का उच्चारण ओडिशा राज्य के मूल नाम उत्कळ के इसी उच्चारण से किया गया, उत्कल नहीं। हिंदी की खड़ी बोलियों में भी यह अक्षर है, जिसे अमूमन मराठी भाषा का मान लिया जाता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ‘ळ’ देवनागरी में भी स्वीकृत है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉस्को में लोक शाहिर के नाम से जाने जाते मराठी के दलित लेखक अण्णा भाऊ साठे के तैलचित्र का अनावरण किया जिसे ऑल रूस स्टेट लाइब्रेरी फ़ॉर लिटरेचर में लगाया गया है। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत-रूस संबंधों का उत्सव इस आयोजन के माध्यम से मनाया गया। अण्णाभाऊ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के सदस्य और भारत के उन चुनिंदा लेखकों में शामिल हैं जिनके लेखन का रूसी भाषा में अनुवाद हुआ है। केंद्र सरकार ने मॉस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में साठे के तेल चित्र को लगा रूस और भारत के बीच सांस्कृतिक संवाद को बढ़ाने की कोशिश की है।
सांस्कृतिक संवाद केवल दो देशों के बीच ही नहीं, दो भाषाओं के बीच भी बढ़ना चाहिए और उसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से पहली बार ‘ळ’ का गान हुआ उससे कई लोगों को ख़ुशी मिली तो कइयों की भवें तन गईं और इसे प्रांतीयता का जामा पहनाने की कोशिश की जाने लगी। हिंदी की किसी बोली या वैदिक संस्कृत के किसी शब्द को लिखने में भी इस अक्षर का प्रयोग देखा जा सकता है। इसका उच्चारण कइयों के लिए कठिन होता है लेकिन यदि आप ड़ का उच्चारण कर पाते हैं, तो इसे भी उच्चारित कर सकते हैं। ड़ के उच्चारण में मूर्धा को बिना जिह्वा का स्पर्श करते हुए कहिए तो वही ‘ळ’ हो जाएगा। हिंदुस्तानी समूह की भाषाएँ बोलने वाले सभी लोग इसका उच्चारण कर सकते हैं।
सन् 1867 में जब देवनागरी को स्वीकार किया गया था, उसी समय ‘ळ’ को भी स्वीकृति मिल गई थी। सन् 1983 की हिंदी निदेशालय की वर्णमाला तक यह मूल वर्णावली में था लेकिन उसके बाद शनैः शनैः यह गायब हो गया। यह कैसे, क्यों हुआ वह चर्चा का अलग विषय हो सकता है। सन् 2020 की परिवर्धित देवनागरी में यह फिर शामिल कर लिया गया और जैसे अब सामूहिक तौर पर इसे किसी अधिकृत मंच से स्वीकारा गया है। परिवर्धित देवनागरी का उद्देश्य यही है कि राजभाषा में अन्य भाषाओं के विशेष नाम जिन्हें व्यक्ति और स्थान वाचक संज्ञाएँ कहते हैं, लिखते समय विशिष्ट चिह्नों का प्रयोग करके विकृतिकरण को टाला जाए। टिळक जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए परिवर्धित देवनागरी के प्रयोग से इसे ऐसे ही लिखा जाए तिलक नहीं।
हिंदी में मूर्धन्य ध्वनि ट, ठ, ड, ढ, ण होने के बावज़ूद टिळक का ‘ट’, ‘त’ हो जाता है और ठाणे का ‘ठ’, ‘थ’ या लोणावळा का ‘ण’, ‘न’, ऐसा क्यों? पुणे के रावेत निवासी प्रकाश निर्मळ (निर्मल नहीं) इसे एक मुहिम की तरह चलाते हुए कहते हैं कि लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक का सही नाम दुनिया को बताने का यही सही समय है। आंबेडकर को अंबेडकर मत लिखिए, होळकर को होलकर, माळवा को मालवा और तेंडुलकर को तेंदुलकर मत लिखिए। भारतीय उच्चारणों का विकृतिकरण बंद कीजिए।
डॉ. सुनीता श्रीवास्तव, इंदौर (मप्र)

मेरी अभिलाषा
पूरब से लेकर पश्चिम तक
उत्तर से लेकर दक्षिण तक
भाईचारे का मेल कराती
मेरी हिंदी भाषा है l
हिंदी भाषा हिंदुत्व की जुबा है
संस्कृत, हिंदी की जननी है
वेदों, पुराणों की आत्मा है
राष्ट्र भाषा का जो ताज पहने
वह मेरे देश हिंदी की भाषा है l
बोली का सुकून है हिंदी
एकता की शान है हिंदी
राष्ट्र का संवाद है हिंदीl
हर प्रीत की आवाज में
रग में लहू बन दौड़ती
ह्रदय की भाषा है हिंदी
मुड़कर नही देखतीl
हिन्दी में सभी गुण मिलते
लिपि शब्द व्याकरण हिंदी में खिलते
आंग्ल उर्दू फ़ारसी को अपनाती
तेलगू कन्नड़ मलयालम हिंदी में समातीl
तोड़ दी हमने अब
बरसो पुरानी बेड़ियाँ
अब गुलामी की भाषा ना होगीl
बढ़ते कदमो की सीढ़ियाँ
अब तो धड़कन बन गयी
हिंदी हिंदुस्तान की l
हिन्द के लालो ने दे दी
विश्व मे पहचान भी
नमस्ते ट्रंप बोल बोल कर
गांधी चरखा चलवा दिया
प्यार से हिंदी बोल बोलकर
सर्वशक्तिमान को,जमी पर बिठा दियाl
हिन्द के सपूतों
हिंदी हिन्द की जुबान है
हिंदी के कल्याण से ही
राष्ट्र का उत्थान हैl
करते हैं हम सब वंदन,
मातृभाषा हिंदी का,
हर हिन्दुस्तानी के मन में,
अंकुरित हो जन गण मन,
हिंदी भाषा का पुष्प खिले,
यह मेरी अभिलाषा हैl
डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा ‘उरतृप्त’, महाराष्ट्र

सिंथेटिक शॉल और हिंदी की आत्मा
इस वर्ष भी हिंदी दिवस का पवित्र समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहर के एकमात्र सरकारी हॉल को, जो साल के बाकी दिनों में शादी-ब्याह और राजनीतिक रैलियों के लिए किराए पर दिया जाता था, आज सुबह से ही उसकी आत्मा को धो-पोंछकर चमका दिया गया था। हॉल के बाहर प्लास्टिक के दो-रंगों वाले बैनर पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था: “हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्र की आत्मा है।” नीचे प्रायोजकों के नाम थे – एक तेल कंपनी, एक मोबाइल फोन निर्माता और एक इंग्लिश-स्पीकिंग इंस्टीट्यूट। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि आत्मा की सफाई का ठेका आजकल इन्हीं कंपनियों के पास है। हॉल के अंदर, मंच पर एक विशाल तस्वीर लगी थी, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित नेहरू मुस्कुरा रहे थे, और उनके बीच एक गुमनाम कवि की धुँधली सी तस्वीर थी, जिसे शायद किसी सरकारी बाबू ने गूगल से डाउनलोड किया था। हॉल में भीड़ कम थी, लेकिन उत्साह बहुत था। कुर्सी पर बैठने वाले कम थे, लेकिन मंच पर बैठने वाले ज्यादा थे। और जो बैठे थे, वे ऐसे बैठे थे जैसे राष्ट्र का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर हो। इस भीड़ में सबसे अलग एक वृद्ध सज्जन बैठे थे, जिनका नाम था मास्टर चिंतामणि। उन्होंने हिंदी को अपनी कमाई का जरिया नहीं, अपनी आत्मा का पोषण माना था। वे बैठे थे, जैसे किसी मृत भाषा के अंतिम संस्कार में आए हों, और हॉल में बज रही हल्की देशभक्ति धुन उनकी आत्मा के लिए श्रद्धांजलि हो। उनके बगल में बैठी एक युवा महिला अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम रील्स देख रही थी और बीच-बीच में भावुक होकर हिंदी दिवस पर स्टोरी पोस्ट कर रही थी।
समारोह की शुरुआत हुई। नगर के मेयर, जो स्वयं हिंदी की व्याकरण से अधिक नगर पालिका के बजट की अंकगणित में रुचि रखते थे, ने माइक संभाला। उन्होंने आह्वान किया कि हिंदी को उसका गौरव वापस दिलाना है। वे खुद अपने वाक्य में डिप्लोमा, प्रोजेक्ट, बजट, और कॉर्पोरेट जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मानो हिंदी को आधुनिक बनाने का यही एकमात्र तरीका हो। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि हर शब्द के साथ एक अंगरेजी शब्द अपने आप बाहर निकल आता था। उन्होंने कहा, “आज न्यू जनरेशन को हिंदी की वैल्यू समझनी होगी। हिंदी हमारी रूट्स है।” उनके इस रूट्स शब्द पर हॉल में बैठे कुछ बुद्धिजीवियों ने ताली बजाई। एक शिक्षण संस्थान के प्रमुख ने, जो बच्चों को प्ले-वे मेथड से अंग्रेजी सिखाते थे, बताया कि हिंदी की सेवा के लिए उन्होंने एक नया ऐप बनाया है, जिसमें हिंदी के कठिन शब्दों को डिकोड करने के लिए अंग्रेजी में डिक्शनरी दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी संस्था हिंदी के प्रमोशन के लिए फंड इकट्ठा कर रही है, और इस फंड का सदुपयोग करने के लिए विदेश से एक कंसलटेंट बुलाया जाएगा।
मास्टर चिंतामणि अपनी कुर्सी पर बैठे-बैठे अपना ही इतिहास दोहरा रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदी को पवित्र और महान बताया था, जबकि उनके छात्र उन्हें दकियानूसी कहकर छोड़ गए थे। वे सोचते थे कि हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा नहीं, एक भावना है। वह एक मां है, जो अपने बच्चों को लोरी सुनाती है, कहानी सुनाती है। लेकिन आज हिंदी एक आइटम बन गई थी, जिसे सेल करने के लिए मार्केटिंग की जरूरत थी। उन्होंने याद किया वह दिन, जब उनकी कक्षा में एक भी छात्र अंग्रेजी का शब्द नहीं बोलता था। वे हिंदी पढ़ाते थे, और छात्र हिंदी में ही सवाल पूछते थे। आज, उनकी ही पोती जब उनसे बात करती है तो डैडी के अचीवमेंट और स्कूल के होमवर्क की बात करती है। उन्हें लगता था कि हिंदी ने नहीं, उन्होंने ही अपना आत्मसम्मान खो दिया है। वे एक ऐसे भूत की तरह थे, जो एक ऐसे घर में भटक रहा था जहाँ अब कोई नहीं रहता। उनका मन हुआ कि वे खड़े होकर चिल्लाएं, “यह पाखंड बंद करो!” लेकिन वे चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी आवाज को सुनने के लिए वहाँ कोई कान नहीं थे, सिर्फ ताली बजाने के लिए हाथ थे।
फिर मुख्य अतिथि, जो शहर के एक बड़े बिल्डर थे, मंच पर आए। उनका नाम था मिस्टर कठोरसिंह। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत जेन्टलमेन एंड लेडीज़ कहकर की। वे हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन उनका लहजा ऐसा था मानो वे किसी इंटरनेशनल कॉन्फ़्रेंस को संबोधित कर रहे हों। उन्होंने कहा, “हिंदी सिर्फ हिंदी नहीं, बिजनेस की लैंग्वेज है।” उन्होंने बताया कि कैसे उनकी कंपनी ने डेवलपमेंट के लिए एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहाँ आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का काम हिंदी में होगा, ताकि लोकल टैलेंट को बढ़ावा मिले। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि उन्होंने स्मार्ट सिटी के हर सेक्टर का नाम हिंदी में रखा है: अटल नगरी, विवेकानंद विहार। लेकिन उनके पम्पलेट और प्रॉस्पेक्टस सारे अंग्रेजी में छपे थे। उन्होंने अपनी स्पीच के अंत में एक डायलॉग मारा, “हिंदी हमारी पहिचान है।” जिसे सुनकर हॉल में बैठे व्यापारी वर्ग के लोगों ने जोर से ताली बजाई, क्योंकि पहिचान का मतलब अँगरेजी में ब्रांडिंग होता है, और ब्रांडिंग का मतलब प्रॉफिट। मास्टर चिंतामणि ने कठोरसिंह को देखा और सोचा कि एक बिल्डर ही हिंदी की नींव को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है, और वही आज हिंदी का संरक्षक बना बैठा है।
इसके बाद शिक्षाविद् का नंबर आया। वे एक मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने वैज्ञानिक भाषा में हिंदी की अध्यात्मिकता पर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, “हिंदी वैदिक काल से साइंस की भाषा रही है। इसमें भावनात्मकता और तार्किकता का परफेक्ट संतुलन है।” वे इमोशनल होकर बोले, “हम स्कूल में हिंदी को कम्पलसरी सब्जेक्ट बनाते हैं, ताकि बच्चों को अपनी संस्कृति से कनेक्ट कर सकें।” लेकिन उनके स्कूल में हिंदी को एक टार्चर की तरह पढ़ाया जाता था, और जो बच्चा हिंदी में ए ग्रेड लाता था, उसे बैकवर्ड समझा जाता था। उन्होंने हिंदी के डेवलपमेंट के लिए एक फंड की घोषणा की, जिसका अकाउंट नंबर और वेबसाइट का लिंक उन्होंने अंग्रेजी में बताया। उन्होंने कहा, “हम ग्लोबल हिंदी को प्रमोट करेंगे।” उनका हर शब्द अंग्रेजी की तरह ग्रेविटी से भरा था। उन्होंने कहा, “हिंदी में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना होगा।” उनके इस कथन पर हॉल में बैठे कुछ नौजवानों ने वाह-वाह कहा। मास्टर चिंतामणि को लगा कि वे हिंदी की लाश पर टेक्नोलॉजी का ड्रेस पहनाकर उसे फैशन शो में प्रेजेंट कर रहे हैं।
अगला कार्यक्रम था कवि सम्मेलन। यह हिंदी दिवस का सबसे रोमांचक हिस्सा था। मंच पर चार युवा कवि आए, जो जींस और टी-शर्ट में थे। उनके बालों का स्टाइल कुछ ऐसा था कि लगता था जैसे उन्होंने साइंस के किसी मॉडल को सिर पर रख लिया हो। पहले कवि ने अस्तित्ववाद पर कविता सुनाई, जिसमें इंसान की पहचान और मॉडर्न लाइफ की फ्रस्ट्रेशन की बात थी। उनकी कविता में लॉनलीनेस, एग्ज़िस्टेंस, कंफ्यूजन और सोशियोलॉजी जैसे शब्द इतने थे कि कविता के बीच में एक-दो बार मास्टर चिंतामणि ने उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का आग्रह कर दिया। दूसरे ने पोस्ट-मॉडर्निज़्म पर कविता सुनाई। उनकी कविता में डिजिटल युग और स्टार्टअप कल्चर की रोमांटिकता थी। उन्होंने कहा, “ऐप में दिल धड़केगा, सोशल मीडिया पर प्यार होगा।” मास्टर चिंतामणि को लगा कि हिंदी को भी अब आयातित विचारों का वाहन बनाया जा रहा है। ये युवा कवि हिंदी में नहीं, महानगर की लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और हिंदी को अपग्रेड करने के बहाने उसे अंग्रेजी का सहारा दे रहे थे।
आखिरकार, वह क्षण आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। मास्टर चिंतामणि को सम्मानित किया गया। उनके नाम की घोषणा हुई। जब वे धीरे-धीरे मंच पर चढ़े, तो उनकी साधना उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उन्हें एक शॉल ओढ़ाया गया, जो इतना सिंथेटिक था कि उसमें से प्लास्टिक की गंध आ रही थी, और एक सम्मान पत्र दिया गया, जिसमें उनका नाम और पदनाम गलत लिखा हुआ था। सम्मान पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम अंग्रेजी में लिखा था। कठोरसिंह ने उन्हें माला पहनाई, और फोटोग्राफर ने फ्लैश जलाया। वे उस क्षण सिर्फ एक प्रतीक थे, एक शोपीस, जिन्हें दिखाकर ये लोग यह साबित कर सकते थे कि वे हिंदी की सेवा कर रहे हैं। मास्टर चिंतामणि को लगा कि उन्हें नहीं, बल्कि उनकी गरीबी और दकियानूसी को सम्मानित किया गया है, ताकि आधुनिक और उन्नत लोगों का कद और भी ऊँचा लगे।
फिर उनसे दो शब्द कहने का आग्रह किया गया। मास्टर चिंतामणि ने माइक पकड़ा, उनकी आवाज कांप रही थी। वे प्रवचन नहीं देना चाहते थे। वे बस अपने दिल की बात कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, “हिंदी सिर्फ लिखने-पढ़ने की भाषा नहीं है। हिंदी वो लोरी है जो मां सुनाती है। हिंदी वो गाली है जो गुस्से में निकलती है। हिंदी वो भजन है जो मंदिर में गाया जाता है।” उनके शब्द सरल थे, उनमें कोई अहंकार नहीं था। वे आत्म-चिंतन की बात कर रहे थे, भाषा के व्याकरण की नहीं। उन्होंने कहा, “हम हिंदी को दिमाग से स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे दिल से नहीं अपनाते।” उन्होंने कहा, “जब हम बाजार में जाते हैं, तो दुकानदार से अंग्रेजी में बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी में बात करना बेइज्जती है।” वे हॉल में बैठे लोगों की असलियत को उजागर कर रहे थे।
जैसे-जैसे मास्टर चिंतामणि बोलते रहे, हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग बोर हो रहे थे। एक अधिकारी ने अपनी घड़ी देखी, मानो वह कोई मीटिंग मिस कर रहा हो। मेयर साहब ने अपने फोन पर सोशल मीडिया चेक करना शुरू कर दिया। बिल्डर कठोरसिंह को एक ज़रूरी कॉल आ गया और वे हॉल से बाहर चले गए। कवि अपने मोबाइल पर फीडबैक देख रहे थे। मास्टर चिंतामणि की आवाज सिर्फ हॉल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उन्हें लगा कि उनकी आत्मा बोल रही है, लेकिन आत्मा की भाषा कोई नहीं समझता, क्योंकि लोग व्यवहार की भाषा समझते हैं। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि वे अपनी मातृभाषा के सम्मान समारोह में अनदेखे हो रहे थे। वे बोल रहे थे और लोग धीरे-धीरे हॉल से बाहर जा रहे थे, जैसे वे प्रवचन नहीं, अहम् का व्याकरण सुन रहे हों।
मास्टर चिंतामणि ने अपनी बात पूरी की और माइक वापस रख दिया। कोई ताली नहीं बजी। वे मंच से नीचे उतरे, और उनके कंधे पर अभी भी वह सिंथेटिक शॉल था। वे धीरे-धीरे बाहर निकले। बाहर सड़क पर एक बड़ी सी बिलबोर्ड लगी थी, जिस पर लिखा था, “स्पोकन इंग्लिश में मास्टरी करें और ब्राइट फ्यूचर पाएँ।” वे हँसे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन का त्योहार है, और बाकी 364 दिन हिंदी की पराजय का उत्सव है। वे घर की तरफ चले, और रास्ते में एक बच्चा मोबाइल पर पबजी खेल रहा था, और अपने दोस्त को अंग्रेजी में गालियाँ दे रहा था। मास्टर चिंतामणि ने शॉल को ठीक किया, जैसे वह उनकी असफलता का बोझ हो।
निशा भार्गव, दिल्ली

भाषा
हिंदी एक भाषा
कोमल सी अभिलाषा
सुमधुर आशा
भोली सी जिज्ञासा
हिंदी है मनोहर
सादगी की सहोदर
प्यारा सा कलेवर
सादा सा तेवर
देश का सम्मान
जनमास की पहचान
हिन्दी है पावन संस्कार
जन-जन को जोड़ने का आधार
सुहानी भोर है
नर्तन करता मोर है
इसमें बहुत जोर है
शतप्रतिशत प्योर है
आंचल है धवल
चेतना है नवल
छोटी नहीं, बड़ी है
अपने पैरों पर खड़ी है
विविध भाषाओं से रखती है मेल
इसको सीखना जैसे कोई खेल
हमारी है धरोहर
बहुत है मनोहर
हिंदी हमारी धड़कन है
इसकी किसी से नहीं अनबन है
ये हमारी सरताज है
इससे मुस्कराता हमारा कल और आज है
संगीत की सरगम है
मिटाती हर गम है
समझने में सरल है
पीती हर गरल है
हिंदी अरमान है
संस्कृति का मान है
इससे बढ़ता ज्ञान है
देश का अभिमान है।
डॉ. संध्या सिलावट, इन्दौर (म.प्र.)

हिंदी में विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रचलन, हिंदी हेतु आशीर्वाद है या अभिशाप
भाषाएँ सदा से ही अपना रूप परिवर्तित करते हुए चली आ रही हैं। सोलहवीं शताब्दी में बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा वर्तमान की अंग्रेजी भाषा से बहुत अलग है। वैसे ही सातवीं सदी से हिंदी भाषा अपना रूप परिवर्तित करते हुए चली आ रही है। सदा से ही जन सामान्य अपनी आवश्यकताओं एवं तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित भाषा के साथ अपना सामंजस्य बिठाता चलता है। भारत में इतिहास इस बात का साक्षी है कि मुगलकाल में फारसी एवं अंग्रेजी काल में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला रहा। शासन से जुड़े एवं शिक्षित व्यक्तियों ने मुगलकाल में फारसी-उर्दू एवं अंग्रेजी काल में और वर्तमान में भी अंग्रेजी सीख, उसी को जीविकोपार्जन और अपनी श्रेष्ठता का साधन बना लिया। जन सामान्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं व हिंदी भाषा के साथ जीवनयापन करता चला आ रहा है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद से लेकर खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो तक और आज के विज्ञान और तकनीक से भरे इस युग में हिंदी जनसामान्य की भाषा होते हुए उन्नति करती चली आ रही है। आज भी हिंदी पहले से कहीं अधिक लोगों द्वारा बोली-सुनी तथा पढ़ी – लिखी जा रही है। आज भी हिंदी चैनल मुख्यतः न्यूज चैनल जितने देखे जा रहे हैं, जितने लोगों तक उनकी पहुंच है, जितना वे कमा रहे हैं, अंग्रेजी चैनल उसका आधा भी नहीं।
वैश्वीकरण के कारण विश्व के अन्य देश व भारत के हिंदी इतर प्रदेश अपने यहाँ निर्मित धारावाहिक, फिल्में एवं अन्य कार्यक्रम हिंदी अनुवाद कर हिंदी जानने वालों हेतु परोस रहे हैं। यह उनका हिंदी प्रेम नहीं अपितु आर्थिक लाभ एवं व्यावसायिक लाभ हेतु अपनी रचना विश्व के अधिकतम व्यक्तियों तक पहुंचाने का एवं अपनी सफलता मनवाने हेतु किया गया, व्यावसायिक बुद्धि का उपाय है। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, “हमारे पूर्वजों ने दीर्घकाल की तपस्या और मनन से जो ज्ञानराशि संचित की है, उसे सुरक्षित रखने का सबसे मजबूत पात्र है, अकारण और सकारण, शोषित और पोषित, मूढ़, निर्वाक जनता तक आशा और उत्साह का संदेश इसी जीवंत और समर्थ भाषा के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, यदि देश में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को हमें जनसाधारण तक पहुंचाना है तो इसी भाषा का सहारा लेकर हम यह कर सकते हैं। हिंदी इन्हीं संभावनाओं के कारण बढ़ी है।”
स्वतंत्रता पश्चात् भारत सरकार ने हिंदी के प्रचार–प्रसार हेतु अनेक प्रयास आरंभ किए, जिससे अंग्रेजी को धीरे-धीरे अपदस्थ कर हिंदी को उसके स्थान पर प्रस्थापित किया जा सके। इस कार्य के लिए ऐसे लोगों की नियुक्तियॉं की गईं, जो हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी समुचित ज्ञान रखते थे। डॉ. हरिशंकर बच्चन एवं सिद्धेश्वर वर्मा आदि अनेकों विद्वान थे, जिन्हें यह कार्य सौंपा गया था। पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्याय बनाने की समितियाँ बनाई गई थीं।
विद्वानों को इस कार्य में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वास्तविकता यह है कि आरंभ से हिंदी का जहाँ विकास किया जाना चाहिए था, वहीं से हिंदी को वर्जित किया हुआ है। कोई भी भाषा निरंतर प्रयोग से ही विकसित होती है। हिंदी भी केवल प्रयोग से और प्रयोग से ही विकसित होगी। आरंभिक परिणाम असंतोषजनक हो सकते हैं, परन्तु जिस कोटि के मस्तिस्क उन प्रयोगों में लगेंगे वे हिंदी को सुस्पष्ट, सुसंबद्ध, तर्कसंगत विचारों की मौलिक वाहिका बनाकर उसकी सक्षमता का प्रमाण दे रहे हैं और भविष्य में भी देंगे।
गलत हिंदी से चलकर हम सही हिंदी पर पहुंच सकते हैं, पर अहिंदी से हिंदी की ओर कोई रास्ता नहीं बनाया जा सकता। भाषा वह बैल है जिस पर जितना अधिक बोझ लादा जाए वह उतना ही मजबूत होता जाता है। भाषा की शक्ति उसकी संभावना से आंकी जानी चाहिए। हिंदी की प्रकृति-प्रवृत्ति ऐसी है कि उसके विकास की संभावनाएँ असीमित है। आवश्यकता केवल अधिक से अधिक प्रयोग करने की है।
तत्कालीन समय शिक्षा मंत्रालय की कार्यकारी समिति में ‘मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल’ को हिंदी में क्या कहा जाए इसकी चर्चा थी। तब कार्यकारी यूनिट का सुझाव था ‘परराष्ट्र मंत्रालय’ या ‘परराष्ट्र कार्य मंत्रालय। पर्यायों को खोजने में विद्वानों की प्रवृति प्रायः शब्दानुयायी होने की थी और बच्चन जी स्वतंत्रता और मौलिकता के पक्ष में थे। उन्होंने ‘विदेश मंत्रालय’ का सुझाव दिया। उन्होंने पं. नेहरू से इसकी चर्चा की। उनकी स्वीकारोक्ति के बाद सभी दस्तावेजों में ‘विदेश मंत्रालय’ का प्रयोग किया जाने लगा जो अब तक प्रचलन में है।
शब्दों के हिंदीकरण के पीछे एक लक्ष्य यह भी था कि हिंदी राष्ट्रभाषा रूप में स्वीकृत होने के साथ ये शब्द प्रांतीय भाषाओं में भी स्वीकार कर लिए जाएंगे, परन्तु प्रांतीय भाषाओं की सहमति भी आवश्यक थी। दो समितियां बनाई गई थीं। एक वैज्ञानिक शब्दों के लिए, दूसरी रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की अध्यक्षता में विज्ञानेत्तर शब्दों के लिए। इस समिति के सदस्य बच्चन भी थे। उन्होंने अनुभव किया कि संस्कृत आधारित शब्दावली ही समस्त प्रातों में सहजता से स्वीकृत होती है, अस्वीकृति आती थी तो प्रायः तमिल से। अब लगता है कि उसके पीछे एक सुनिश्चित हिंदी विरोधी प्रवृति थी जो आगे-आगे अधिकाधिक उग्र होती गई है। यह बात इस उदाहरण से भी स्पष्ट है, जब राष्ट्रीय प्रसारण ‘आकाशवाणी’ के प्रयोग पर इतना बावेला मचाया गया कि प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करके उसे पूर्व प्रयुक्त ऑल इंडिया रेडियो रखने का आश्वासन देना पड़ा था। वस्तुतः तमिल नीति हिंदी विरोधी ही नहीं संस्कृत विरोधी भी है।
एक अन्य उदाहरण लीजिए, ‘कस्टम’ के लिए ‘सीमा शुल्क’ बना, ‘कस्टम हाउस’ के लिए सीमा शुल्क सदन’ ‘कस्टम हाउस ऑफिसर’ के लिए ‘सीमा शुल्क सदन अधिकारी’ बना। दिनकर बोले पड़े, यह तो तुलसीदार की एक चौपाई ही बन गई। शब्दों के जो हिंदी पर्याय अंतिम रूप से निश्चित होते थे, उनमें से हिंदी भाषी प्रांतों में भी बहुत से शब्द स्वीकृत नहीं हुए थे, उदाहरण के लिए ‘सेक्रेट्रिएट’ के लिए सचिवालय’ निश्चित हुआ था। मध्यप्रदेश में ‘संचालनालय’ कितना उच्चारण दुरूह शब्द तब से अब तक चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के लिए मराठी में ‘पंतप्रधान’ प्रयुक्त होता है। अपनी-अपनी ढपली अपना अपना राग के जो दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, वह आज हम सब सह रहे हैं। विविधताओं से भरे इस देश में केवल भाषा ही ऐसा माध्यम है जो हमें एकसूत्रता में बांध सकता है, यदि भाषा में भी हम एकमत हों, सुसंगठित न हो सके तो हमारे बिखराव को कोई नहीं रोक सकता।
हिंदी भाषा अंग्रेजीदां अफसरों के बीच मजाक की ही वस्तु है। ‘अंडर सेक्रेटरी’ को ‘नीचे सचिव’ कह कर हँसना आम बात है। कोई कहता है कि रेडियो को क्या कहेंगें विद्युत प्रसारण यंत्र ? तोलेभर अंग्रेजी शब्द के लिए सेर भर का हिंदी शब्द। वस्तुतः बालकृष्ण शर्मा ने रेडियो से अपने काव्य पाठ में एक बार कहा था-रेल को क्या कहेंगे ? ‘लौहपथ गामिनी’!
आचार्य रघुवीर जो राज्य सभा के सदस्य थे। शब्दों के लिए विशुद्ध संस्कृत की और जाने के पक्ष में थे। उन्होंने ईमानदारी से शब्दावली पर गंभीर चिंतन किया था और वह जिन परिणामों पर पहुंचे थे, वे बहुत तर्क सम्मत भी थे, पर बड़ी विचित्र बात है कि भाषा का विकास सदैव तर्क के आधार पर नहीं होता। लोग उनके सिद्धांतों को अति तक ले जा कर ऐसे-ऐसे शब्द गढ़ते थे जो शायद आचार्य रघुवीर को भी न सूझते जैसे ‘टाई’ के लिए ‘कंठ लंगोट’।
आज अंग्रेजी के बहुत से शब्द जैसे प्लेटफार्म, रेडियो, कप प्लेट, गिलास, टिकट और बस आदि सामान्य जन की भाषा में रच बस गए हैं। अंग्रेजी-भाषियों ने जहाँ-जहाँ राज्य किया वहाँ से बहुत से शब्द अंग्रेजी भाषा में मिला लिए। जैसे ‘रिक्शा’ जापानी शब्द है जो अंग्रेजी में भी रिक्शा है। अंग्रेजी में लैटिन, जर्मनी और भी अन्य कई भाषाओं के शब्द अपना लिए गए है, जिन्हें अज्ञानवश हम अंग्रेजी के ही समझते हैं। फारसी का दर, अंग्रेजी का डोर और ब्रज का द्वार ये तीनों अलग अलग भाषाएँ हैं परन्तु दरवाजे के तीनों वाचकों में कितनी समानता है। इसी प्रकार ब्रज का नियरे, अंग्रेजी के नियर (near) के कितना निकट है।
हैदराबाद में बोली जानी वाली दक्खिनी क्या हिंदी नहीं है। उसे हैदराबादी हिंदी की संज्ञा दी जाती है। भाषा की प्रवृत्ति होती है कठिन से सरलतर हो जाने की। यह साहित्यिक भाषा के सामान्तर विकसित होती रहती है। पहले संस्कृत से पालि, पालि से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ठ और अवहट्ठ से खड़ी बोली तक का सफर हिंदी ने तय किया है। सम्राट अशोक से लेकर अब तक भाषा परिवर्तित होती जा रही है। इस परिवर्तन में हजारों वर्षों का समय लगता है। अंग्रेजी भाषा जो शेक्सपीयर के समय थी, वर्तमान में ऐसी नहीं रही है। अंग्रेजी के भी दो रूप मुख्य हो गए हैं। अमेरिकन अंग्रेजी और ब्रिटिश अंग्रेजी। अमेरिकन संस्कृति वस्तुओं को सहज, सरल और जन के द्वारा सुप्राप्य बनाने की रही है। वहीं ब्रिटिश संस्कृति शासक और शासित में अंतर बनाए रखने एवं परंपरा को सख्ती से निभाने की है। भाषा के प्रति भी दोनों का यही व्यवहार है। परन्तु जानबूझकर अपनी सुविधा के लिए भाषा के साथ छेड़छाड़ करना एवं उसके मूल स्वरूप को बिगाड़ना अत्यंत गलत है। ऐसा व्यवहार किसी भी भाषा के लिए अभिशाप बन जाएगा। आजकल जैसे वाक्य पढ़ने में आ रहे हैं, विशेषतया फैशन से संबंधित लेखों में जैसे आजकल रेड कलर इन है, ब्लैक कलर आउट है। ऐसी भाषा से दुःख होता है, लगता है जानबूझकर भाषा से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेखक सही भाषा का प्रयोग ही नहीं करना चाहता। बेगम सीता और शहजादे राम-लक्ष्मण लिखा जाए तो अंतर्मन को पीड़ा तो होगी ही। नए प्रयोग किया जाए और नए शब्द अपना जाएँ किन्तु सोच समझकर।
जैसे साईकिल के लिए द्विचक्र वाहिनी शब्द प्रयोग करना उचित नहीं होगा क्योंकि आमजन भी साईकल शब्द समझता है। उसके प्रत्येक भाग के ब्रेक, रिम, टायर और पैडल आदि के नाम वह सहजता से प्रयोग करता है। वर्तमान में कम्प्यूटर, बैंक, सैल फोन, कैलकुलेटर, ट्रक, कार, टेक्सी, रेल, फेसबुक, मिस्ड कॉल, पैन, पेंसिल, आई.टी. आदि अनेकों शब्द हैं जिन्हें स्वीकारना ही पड़ेगा।
जो शब्द तकनीक से संबंधित है और आम लोगों के बीच प्रचलित है, चाहे वह किसी भाषा के हों उन्हें अपनाना ही पड़ता है यदि उनका सटीक प्रयोग कर भाषा समर्थ बनती है तो उन्हें अपनाने में क्या हर्ज है।
हिंदी विश्व की सरलतम भाषाओं में है, इसकी लिपि वैज्ञानिक है। हिंदी की स्वीकार्यता स्वयं ही व्यापक हो रही है। हिंदी व्यापार, व्यवसाय, इंटरनेट, शिक्षा, विज्ञान, बाजार के लिए प्रभावी, उपयोगी, सटीक एवं सक्षम भाषा है, हिंदी की प्रयोजनियता दिन प्रति दिन उभर कर आ रही है। इस लिए हिंदी को बनाए रखने के लिए हिंदी इतर शब्दों को अपनाना उचित है, परन्तु हिंदीपन को अक्षुण्ण रखते हुए।
डॉ. वर्षा महेश, मुंबई (महाराष्ट्र)

हमारी हिंदी! हमारा गौरव
वेद – पुराणों की एक स्वर्णिम गाथा है
हिंदी भारत के जनमानस की भाषा है
भावनाओं की अभिव्यक्ति का बंध है
संस्कारों की सरिता का अनुबंध है
जळधि सी गहरी है शिखर सी ठहरी है
रीति रिवाजों,परंपराओं की देहरी है
संस्कृति के संवर्धन की अभिलाषा है
हिंदी भारत के जनमानस की भाषा है
मनुष्यता का मान है,लोकगीतों का गान है
विषयों का ज्ञान है, व्यक्तित्व का निर्माण है
कलाओं का स्पंदन है, प्रकृति का वंदन है
मां भारती के भाल पर शब्दों का चंदन है
मुनियों का तप, गुणियों की जिज्ञासा है
हिंदी भारत के जनमानस की भाषा है
संस्कृत की प्रस्तुति है,देवों की स्तुति है,
पर्वों की संस्कृति, यज्ञों की पावन श्रृति है
रंगमंच का प्रसार है,राष्ट्र का विस्तार है
बिन भाषा ज्ञान के सूना सब संसार है
मनुज अभिव्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है
हिंदी भारत के जनमानस की भाषा है
मनोज कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली

हिन्दी दिवस
हिन्दी दिवस की आहट से शुभकामना और बधाई भेजने वालों का तांता लगा हुआ। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए बधाई दे दिए हैं कि उन्हें ज्ञात है, मैं हिन्दी सेवी हूँ। जैसे अन्य दिवस पर मिल जाती है। अधिकांश जन केवल दुःख प्रकट कर रहे हैं। कुछ व्यंग्य कर रहे हैं। शेष कर्तव्य मानकर उसकी इतिश्री। हिन्दी के मूर्धन्य व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का एक कथन भी खूब वायरल हो रहा है कि दिवस कमजोर का मनाया जाता है। बिल्कुल बुखार टाइप। जो मौसम बदलते वक़्त आना ही है। वही बुखार आज हिन्दी भाषियों को चढ़ा हुआ है। जैसे शिक्षक दिवस, महिला दिवस, श्रमिक दिवस, हिन्दी दिवस, कभी भी थानेदार दिवस, पुरुष दिवस, अधिकारी दिवस, अंग्रेजी दिवस नहीं मनाया जाता? तो सुनो! उनका दिवस होता ही नहीं, वे तो थोपे गए लोग/चीज हैं। दिवस उनका होता जिनके लिए हृदय में आस्था होती, उनका उत्सव मनता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षक की भूमिका, निर्माण में श्रमिकों की भूमिका और प्रत्येक घर में स्त्रियों की भूमिका की तरह ही संस्कृति के निर्माण में भाषा की भूमिका तय होती। और भारत में वह भाषा हिन्दी है। विभिन्न तरह के इमेज, वॉलपेपर और चित्र काव्य पंक्तियों से सुशोभित अर्पित किये जा रहे हैं। किन्तु उसका मर्म नहीं समझ पा रहे। मैं पूछता हूँ तुम! हिन्दी को इतनी आदरणीय क्यों बना रहे हो। उसकी पूजा नहीं करनी। उसे अपने आचरण और व्यवहार में लाना है। उसका प्रयोग बढ़ाना है। भाषा गतिशील होती है और गतिशीलता ही उसकी जीवंतता है। कुछ और लोग हैं जो हिन्दी प्रेम में अन्य भाषाओं, विशेषतः अंग्रेजी को कोस रहे हैं। अरे! अपनी भाषा को मान देने के लिए दूसरे को अपमानित करना या छोटा दिखाना जरूरी है क्या? वह भी भाषा है हमारी अतिथि भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हिन्दी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। पैंसठ करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। हिन्दी व्यापार, शिक्षा, संचार के साथ मनोरंजन और इंटरनेट की सबसे सशक्त भाषा है। विश्व के शीर्ष दस समाचार पत्रों में से छः हिन्दी में प्रकाशित होते हैं। दुनिया के 260 से अधिक विश्वविद्यालय स्नातक और परास्नातक के साथ शोध सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अनेक गैर हिन्दी भाषियों द्वारा की गयी हिन्दी सेवा स्तुत्य है। आप अंग्रेजी पढ़िये, सीखिए, बोलिए, पर इसे बैठक कक्ष तक सीमित करिए। अपनी रसोई और शयनकक्ष से दूर रखिये। हिन्दी प्रेमियों मैं आपको बता देना जरूरी समझता हूँ। कि हिन्दी भारतीय संस्कृति की तरह विशाल हृदया है। इसकी ग्राह्यता ही इसकी विशेषता है। हिन्दी ने सभी सम्पर्क भाषाओं से उनके शब्द ग्रहण किये हैं। आप विशुद्ध हिन्दी की तलाश में संस्कृत की गोद में पहुँच जायेंगे और आधुनिक हिन्दी की तलाश में हिंग्लिश के साथ खड़े पायेंगे। आख़िर इतना अन्वेषण क्यों? वह तो सबका स्वागत करती है। सबको अपनाती है। साथ ले चलती है। यहाँ किसी का विरोध नहीं है। वैमनस्य नहीं है। बस प्यार है। अपनापन है। साथ आओ मिलकर चलो। बस स्वयं को मत भूलो। 14 सितम्बर हिन्दी दिवस के रूप में हमारे जीवन और समाज के साथ संस्कृति में उसके योगदान के जीवंत उत्सव मनाने का और आदरणीय व्यौहार राजेंद्र सिंह जी की जन्म दिवस और उनके प्रयास के स्मरण का दिन है। बाकी हिन्दी तो हमारी रगों में लोरी, प्रेरणा, डांट, हँसी, ठहाकों के साथ घुट्टी की तरह दौड़ रही है। जिसमें हमने बोलना, गाना, पढ़ना, जीना सीखा है।
आज सम्पूर्ण देश में हिन्दी क्या कोई भी भाषा नहीं बोली जाती, या बोली नहीं जा सकती। क्योंकि भारत एक बहुभाषा-भाषी देश है। जिसके अनेक क्षेत्र में तरह-तरह की भाषाएँ और उनके क्षेत्रीय रूप बोलियों के रूप में प्रचलित हैं। भारत की भौगोलिक एवं संवैधानिक दोनों ही स्थितियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। किन्तु मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूँ। कि भारत यात्रा के दौरान मैंने जो देखा और पाया कि सम्पूर्ण भारत के नगरीय क्षेत्र में हिन्दी बहुत अच्छी तरह से समझी एवं व्यवहार में लायी जाती है। जिसका एकमात्र कारण इसका व्यावसायिक होना है। संचार में अधिगम्यता और सहज होने के कारण हिन्दी व्यापार की भाषा है। अरुणाचल के तवाँग और मेघालय के डाउकी से लेकर गुजरात के आख़िरी बिन्दु द्वारका और दमन-दीव के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी अंतरीप के तट पर बैठे लोगों तक हिन्दी समझी एवं बोली जाती है। जिस में हिन्दी फिल्मों, समाचार पत्रों टीवी सीरियल, विज्ञापन, सोशल मीडिया के साथ व्यावसायिक प्रतिबद्धता ने इसे मजबूत किया है। पाँच उप भाषाओं (पूर्वी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी) और अट्ठारह बोलियों (अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, कन्नौजी, खड़ीबोली, बुंदेली, हरियाणवी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, गढ़वाली, कुमाऊँनी एवं दक्खिनी) से संपृक्त हिन्दी आज भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक नगरों व राजधानियों में शिक्षण प्रशिक्षण की भाषा के रूप में सर्वमान्य एवं स्वीकृत है। ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के क्रम में मंदारिन और अंग्रेज़ी के बाद हिन्दी का तीसरा स्थान है। हिन्दी भले ही भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में संवैधानिक स्वीकृति से वंचित हो किन्तु करोड़ों हिन्दी प्रेमियों के हृदय में राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा के साथ जन-जन की भाषा के रूप में अधिष्ठित है।
डॉ.वीणा विज ‘उदित’, जालंधर (पंजाब)

प्रवासी साहित्य एवं संस्कृति में हिंदी का योगदान
प्रवासी भारतीयों की जीवन शैली और मातृभूमि के प्रति प्रेम व समर्पण में बढ़ोतरी हो रही है। वह दिन लद गए जब भारतीय विदेश जाकर अपनी कर्मभूमि में दिन रात इस कदर व्यस्त रहते थे कि उन्हें समय ही नहीं मिलता था कि पीछे लौट कर देख सकें या गहन संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर अपने दिल का हाल कह सकें। अपनी मातृभूमि से प्रेम के बीज जो उनके हृदय में पल रहे थे वे पल्लवित हो उठे हैं तकनीकी का सहारा लेकर ! विश्व बंधुत्व और दुनिया छोटी होने यानि कि ग्लोबलाइजेशन के कारण समीपता बढ़ गई है। जिसने देश और विदेश में बसे सभी भारतीयों को एकसमान धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है।
सर्वप्रथम मैं अस्सी के दशक से पूर्व अमेरिका में हिंदी की शिक्षा के विषय में बात करूंगी— जब हिंदी की शिक्षा चंद विश्वविद्यालयों व पारिवारिक शिक्षण तक ही सीमित थीl
अस्सी के दशक में भारतीयों की संख्या में वृद्धि अंतरजातीय विवाह और कुछ राजनैतिक कारणों से हिंदी के प्रति रुचि बढ़ी! साथ ही विश्व विद्यालयों ,मंदिरों व सामाजिक संगठनों में प्रारंभिक स्तर के हिंदी पठन-पाठन में बढ़ोतरी हुई। इसी समय में हिंदी प्रेमियों ने अंतरराष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन और हिंदी संस्थान की स्थापना की। उन्हीं दिनों हिंदी कवि सम्मेलनों का शुभारंभ काका हाथरसी को बुलाकर कवि सम्मेलन से शुरू हुआ और लोकप्रियता मिलने से हर वर्ष अमेरिका के कई शहरों में कवि सम्मेलन व मुशायरे आयोजित होने लगे थे। तभी से प्रवासी भारतीयों ने भी साहित्य सृजन आरंभ कर दिया था और अंतरराष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन ने त्रैमासिक पत्रिका “विश्वा” प्रकाशित करनी आरंभ कर दी। हिंदी की संस्था की शाखाएं भी कई राज्यों के बड़े शहरों में बनी ! कनाडा में भी हिंदी के प्रति जागरूकता दिखनी शुरू हुई थी तभी से।
माध्यमिक स्तर पर हिंदी की प्रथम औपचारिक कक्षा टैक्सेस राज्य के ह्यूस्टन (Houston) शहर में देश के सौ सर्वश्रेष्ठ हाई स्कूलों में से एक “बेलयर सीनियर हाई स्कूल” में केवल दस छात्रों से 1988 में श्री अरुण प्रकाश ने शुरू की। आज वहां पर सात स्तरों पर सौ से अधिक छात्र हिंदी सीख रहे हैं। यह देश का अकेला स्कूल है जहां तीस वर्षों से भी अधिक समय से भारत की सभ्यता, युवा हिंदू धर्म की औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है। 1992 में इसी स्कूल में अंतरराष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन का तीन दिन का देश का सबसे बड़ा हिंदी अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें भारत के बारह विद्वानों ने भाग लिया थाl
अरुण प्रकाश जी ने सन 1992 और 2002 में राइस विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन ( Houston) में तीन स्तरों की हिंदी कक्षाएं शुरू की और 2008 में “नमस्ते जी” नाम से 480 पेज की प्राथमिक हिंदी की पुस्तक प्रकाशित की। जिससे उन्हें कई सारे पुरस्कारों के साथ 2009 में “साउथ एशियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर” अवार्ड भी दिया गयाl सन 2002 में ह्यूस्टन के कवि सम्मेलन में मैंने भी प्रतिभागिता करी और मेरी कविता “घर बनाम मकान”की मार्मिकता ने ऑडियंस को रुला दिया।
हिंदी का सर्वाधिक विकास तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने राजनैतिक कारणों से हिंदी को “क्रिटिकल नीड लैंग्वेज” घोषित किया और इसके विकास के लिए कुछ मिलियन डॉलर की धनराशि दी। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने अमेरिकन काउंसिल फॉर द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस की मदद से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए। जिनमें से स्टार टॉक और डेवलपमेंट ऑफ हिंदी करिकुलम वन ग्रेड से ग्रेजुएट तक अमेरिका के लिए प्रमुख हैं। इसी समय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ने भी सहायता दी! और मिलिट्री स्कूल में हिंदी अनिवार्य हुई। इस सब में श्री अरुण प्रकाश जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय कई विद्यालयों, विश्वविद्यालयों व सामाजिक संस्थानों द्वारा हिंदी के विकास,प्रचार व शिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और तीन विद्यालयों में इंटरनेशनल Becca Laureate Hindi (IB)आईबी हिंदी भी उपलब्ध हैl
पिछले दशक से मैं कई ई -पत्रिकाओं जैसे “साहित्य कुंज’ कैनेडा से जिसे सुमन घई जी संचालित कर रहे हैं! इनकी ई पत्रिका में मैं आज तक लिख रही हूं और मेरी सर्वाधिक कहानियां छपी हैं! “अभिव्यक्ति अनुभूति” ई पत्रिका श्रीमती पूर्णिमा बर्मन दुबई से निकालती थी और इसमें कविता और कहानियां छपती थी इसके अलावा “ई-कविता ” नाम से न्यूयॉर्क अमेरिका से श्री अनूप भार्गव जी ने आरंभ की थी, मैं इन सबसे बरसों से जुड़ी रही। जिनमें मेरा लेखन अनवरत रूप से चलता रहा अर्थात इन ई- पत्रिकाओं में प्रवासी भारतीयों के साथ- साथ हम जैसे भारतीय लेखक, कवि आदि भी छप रहे थेl चंद्रमा के बढ़ते आकार की भांति प्रवासी भारतीयों की ख्याति बढ़ रही है। विदेशों में जितना भी लेखन हो रहा है उनका प्रकाशन भारत में हो रहा है जिससे प्रकाशक भी उत्साहित हैं। प्रवासी भारतीयों की किताबें भी धड़ाधड़ छप रही हैं। वे पहले भारत में फिर अपने देश में आकर भी इनका लोकार्पण करते हैं ! आजकल तो भारत की अधिकतर संस्थाएं प्रवासी भारतीयों को विभिन्न उपाधियां और ईनाम देकर उन्हें प्रोत्साहन देकर स्वयं भी गौरवान्वित हो रही हैं!
आप यह जानकर हैरान होंगे कि यहां एक ही शहर के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नाम से हिंदी की संस्थाएं खुली हुई है जिनमें लगातार गोष्ठियां होती रहती हैं। जिन में काव्य पाठ चलते हैं। सैन फ्रांसिस्को के” इनर आई क्लब “की एक गोष्ठी में मुझे बुलाया गया था जहां विभिन्न देशों की महिलाएं बैठी थी। उस गोष्ठी में अंग्रेज,अफ्रीकन,चाइनीस, कोरियन आदि सभी देशों की कविताएं अंग्रेजी में श्रीमती अंशु जौहरी ने पढ़ीं। जिससे सब एक दूसरे के भावों को समझ सकें। हैरान थी मैं यह सब सुनकर और देख कर कि हर देश की नारी उसी पीड़ा से ग्रसित हैं जिससे भारत की नारी अपने आप को पीड़ित मानती है। मुझे ” ग्लोबल हिंदी ज्योति संस्था ” वालों ने भी बुलाया था खुले मंच पर काव्य पाठ करने के लिए। बहुत आदर सत्कार किया श्रीमती अनीता कपूर ने और मेरे काव्य संग्रह “दरीचों से झांकती धूप”का लोकार्पण भी किया था। इस विषय में मेरा आलेख ट्रू मीडिया में छपा था। वहां हमारे माननीय राष्ट्रकवि श्री गोपाल दास नीरज जी के पोते भी पधारे थेl
प्रवासी भारतीयों की इन संस्थाओं में भारत के तत्कालीन हालात पर विचार-विमर्श भी होता है। यदि कोई विपदा की घड़ी आए तो यह प्रवासी भारतीय पैसे इकट्ठे कर के भारत भेजते हैं। “विश्व हिंदी ज्योति संस्था”के सदस्यों ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गरीब बच्चों के लिए पाठशाला खोली है। वे वहां जाकर उन्हें पढ़ने का सामान, यूनिफॉर्म आदि दिलाते हैं। सैन फ्रांसिस्को में श्रीमती नीलू गुप्ता, श्रीमती मंजू मिश्रा और उनकी सहकर्मियों ने ऐसी एक संस्था “उपमा” नाम से यूपी में खोली है जिसको देखने वे समय-समय पर भारत जाती रहती हैं और उन सब को मिलकर आते हैं आती हैं। इसी प्रकार श्रीमती सुधा ओम ढींगरा जो नॉर्थ कैरोलिना में है उन्होंने मध्य प्रदेश के सिहोर में स्थानीय साहित्यकार श्री पंकज सुबीर जी के साथ “ढींगरा फाउंडेशन” नाम से संस्था खोलकर बच्चों को कंप्यूटर प्रदान किए हैं और उनको शिक्षित किया जाता है!ये “विभोम स्वर” और “शिवना साहित्यकी” नाम से दो पत्रिकाएं निकालते हैं। मेरी चर्चित कहानी ” तुरपाई” इसी में छपी थी पहले। यहां अमेरिका में हिंदी सिखाने के लिए कम्युनिटी कॉलेज खुले हुए हैं जिनमें भारतीय छात्रों के साथ साथ विदेशी छात्रों को भी हिंदी सिखाई जाती है। विदेशी के नाम से केवल इंग्लैंड या अमेरिका ही नहीं,विभिन्न देशों में बसे भारतीय प्रवासी भारतीय कहलाते हैं। आप हैरान होंगे कि दुनिया के 176 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है!
अमेरिका में 65 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है! मेरी जानकार सहेली हिंदी की प्रवासी उपन्यासकार स्वर्गीय श्रीमती सुषम बेदी न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। और गुजरात की श्रीमती अंजना संधीर ने भी वहां कुछ समय हिंदी पढ़ाई थी। जैसा कि हम लोग मानते हैं की हिंदी संस्कृत की बेटी है और हमारी राष्ट्रभाषा है, सो यही इसकी विशेषता है ! इसके अलावा हिंदी की शब्द संपदा,विपुल साहित्य के कारण इसे वैज्ञानिक भाषा तो कहा ही गया है।” जैसा बोलो वैसा लिखो” यानी कि कंप्यूटर के लिए भी हिंदी भाषा सर्व उचित है, ऐसा माना गया है! इसलिए इसकी शिक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं आती है। अमेरिका के टैक्सेस राज्य में हयूस्टन शहर में डॉ. अरुण प्रकाश ने “बायलेयर हाई स्कूल, राइस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन ” में पिछले कई वर्षों से हिंदी विषय पढ़ाया है यह मैं आपको पीछे बता चुकी हूं l अगले सिलेबस में उन्होंने मेरा कहानी संग्रह “मोह के धागे” भी लगाया है। यहां बहुत आसानी से अंग्रेजी को ट्रांसलेट करके हिंदी सिखाई जाती है! इसके लिए –“नमस्ते जी!” पुस्तक अमेजॉन पर मिल जाती है l ह्यूस्टन मैं मेरी कॉलेज की सखी श्रीमती मंजू गुप्ता रहती हैं। दो मार्च 2019 में मेरे वहां पहुंचने पर, उन्होंने अपने घर एक शाम तकरीबन सौ जनों को निमंत्रित किया जिन्हें काव्य और साहित्य में रुचि थी। वे माईक बगैरा लेकर पहुंचे, और एक घंटे से ऊपर मेरी कविताओं के मुग्ध श्रोता बने रहे। अंत में कुछ लोगों ने अपनी कविताएं भी सुनाई, जो आज तक उनकी डायरी में चुपचाप जी रही थीं! उनका उत्साह देखते बनता था। गज़ल और शेरो शायरी भी सुनाई। फिर हम सब ने मिलकर देश भक्ति के फिल्मी गीत गाए। प्रवासी भारतीयों का मनभावन, रस से ओतप्रोत समय– एक यादगार संध्या बन गया था।
इसके अलावा अमेरिका के मंदिर, शिवालय, आर्य समाज,वैदिक सेंटर और पूजा स्थलों में भी हिंदी संस्कृति का प्रचार होता है — हिंदुओं के त्योहार मनाए जाते हैं, रामलीला होती है,दशावतार की कहानियां,अमृत मंथन की कथाएं, देशभक्ति के गीत, आदि सब शिक्षाप्रद कहानियां सिखाने के लिए बिना किसी वेतन के अवैतनिक सेवा की जाती है l होली, दिवाली, दशहरा,पोंगल,करवा चौथ, गुरपुरब आदि त्योहार मनाए जाते है !भारतीय संस्कृति को प्रवासी भारतीय अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाता है l
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी की हमारे भारतीय बॉलीवुड ने हिंदी का बहुत प्रचार किया है! जिस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सरल हिंदी मे डायलॉग बोलते हैं और संगीत इतना कर्णप्रिय है कि अंग्रेजी बोलते बच्चे भी हिंदी गाने धुन में गाते हैं! प्रवासी भारतीयों के बच्चे हिंदी फिल्में बहुत देखते हैं और प्रांतीय भाषाओं की फिल्में भी यहां बहुत चलती है जैसे पंजाबी, तेलुगू, तमिल, गुजराती, मराठी, बंगाली, बिहारी फिल्में l जिस तरह चाइनीस लोग अपने घर में चाइनीस भाषा बोलते हैं उसी तरह भारतीय भाषाएं भी घरों में बोली जाती हैं और भारतीय व्यंजन भी घरों में पकाए जाते हैं l यहां भी पंजाबी, हिंदी रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं l ढाबे का भी खाना मिलता है जिन का श्रेय पंजाबियों को जाता है l ग्लोबलाइजेशन के कारण वर्तमान युग में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है l आज से 20- 30 वर्ष पूर्व जो मुश्किलें थी विदेश में भारतीय सामान मिलने की, वह अब समाप्त हो गई हैं! क्योंकि हम सन 1992 से अमेरिका आ रहे हैं जिससे हमने यहां की जीवन शैली को परिवर्तित होते हुए देखा है और अनुभव किया है जो कि आज अति सुविधाजनक हो गई है l
आप हिंदी साहित्य की बात पूछेंगे तो इतना अवश्य बताना पड़ेगा कि हिंदी समझाने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि उन्हें अंग्रेजी आती है और हिंदी उन्हें सीखनी पड़ती है l इसलिए कोई भी भाषा का निरादर न करते हुए हम उसे सहयोगी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं l मातृभूमि की सेवा और देश के प्रति प्रेम भारतीय लोगों के मन में यहां स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है l राष्ट्र पर कोई भी विपत्ति आने पर यह लोग पीछे नहीं हटते हैं बल्कि बढ़-चढ़कर उसमें सहयोग देते हैं और देश की सेवा करने से नहीं चूकते l हमारे घर में बच्चों को संस्कृत के मंत्र सिखाए जाते हैं, वह हवन भी करते हैं और गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं l इनको बापू का गीत भी आता है—
” वैष्णव जनतो तेने कहिए पीर पराई पराई जाने रे”,
जबकि भारत में रहते हुए बच्चे बहुत कम होंगे जिन्हें यह गीत आता होगा l हमारी पोती को रामायण के सारे पात्र कंठस्थ हैं,आप कहीं से भी कुछ पूछ लीजिए l यह होता है संस्कारों का ज्ञान l आप प्रवासी भारतीयों के साहित्य और संस्कृति के विषय में यही सब तो जानना चाहते थे ना!
भारत की कई संस्थाएं आजकल विदेश में वेबीनार करने में सक्षम हो गई हैं और क्रियान्वित हैं। “महिला काव्य मंच” जिसके संस्थापक भारतीय रक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए श्री नरेश नाज़ हैं– ! इस मंच की भारत में यदि 200 से ऊपर शाखाएं हैं तो अमेरिका में साठ शाखाएं और कई देशों में शाखाएं खुल गई हैं।
“सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति ” के प्रतिदिन के सांध्य कार्यक्रम में ढेरों देश प्रतिभागिता कर रहे हैं। जिसे प्रज्ञान पुरुष श्री सुरेश नीरव गाजियाबाद से संचालित कर रहे हैं। जिसमें मैंने भी चार बार प्रतिभागिता करी थी ! सैनहोजै से द्विभाषी कवित्री श्रीमती अंशु जोहरी “बौछार”कवि गोष्ठी प्रतिमाह करती हैं। दिसंबर 2021और जुलाई 2025 में मैं भी इसकी विशिष्ट अतिथि थी और अभी भारत से द मैजिक मैन एन . चंद्रा का प्रोग्राम “वाणी मां भारती” हिंदी साहित्य साधिकाओं का प्रोग्राम —-जो 10 जनवरी से प्रारंभ होकर 8 मार्च तक चलेगा और जिस में देश- विदेश की कवित्रियां प्रतिभागिता कर रही हैं प्रतिदिन—-भी चल रहा है। जिसकी अध्यक्षता श्री हरीश नवल कर रहे हैं। और नीलम वर्मा जी संचालन में जुटी हुई हैं। यह सब प्रोग्राम वह हैं, जिनमें मैं भी समय-समय पर प्रतिभागिता करती रहती हूं। अंतरजाल ने समस्त विश्व को एक कर दिया है तो फिर साहित्य की क्या चिंता? हमारा साहित्य संपूर्ण विश्व में फलीभूत हो रहा है।
कोरोना आया, जहां उसने विनाश का तांडव खेला वही उसने वेबीनार करने का लोगों को एक रास्ता सुझा दिया, जिससे सब एक होते जा रहे हैं। इसने देशों की दूरियां मिटा दी है और जो कविताएं किताबों में बंद सोई हुई थीं, उन्हें जगा दिया है। वह अपने पंख फैलाए सब के कानों में मिश्री घोल रही हैं। मैं अमेरिका में आकर भी प्रतिदिन किसी ना किसी वेबीनार से जुड़ी हुई हूं और अपने आप को भाग्यशाली मानती हूं कि मैं साहित्य से दूर नहीं हुई विदेश में आकर।
अभी कुछ दिनों पूर्व टोरंटो (कनाडा) की अखिल विश्व हिंदी समिति तथा भारतीय कॉन्सुलट के संयुक्त तत्वाधान में विश्व हिंदी दिवस ( 10 जनवरी )की पूर्व संध्या पर विचार संगोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल मंच से ज़ूम के माध्यम से ऑनलाइन किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर श्री भगवान शर्मा ने की तथा उद्घाटन आदरणीय कौन्सुलेट सुश्री अपूर्वा श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर विश्व के लगभग 34 देशों के तथा भारतीय विद्वानों और कवियों ने सहभागिता की। संपूर्ण सत्र का गोपाल बघेल मधु जी ने संचालन किया।
इसी प्रकार नॉर्वे से हमारे प्रवासी भारतीय आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी हिंदी साहित्य पर बहुत काम कर रहे हैं उनकी कई पुस्तकें भारतीय विभिन्न भाषाओं में भी अनुवादित की गई हैं। इंग्लैंड से श्री तेजेंद्र शर्मा जी हिंदी के एक सशक्त कहानीकार हैं! उषा राजे सक्सेना भी बहुत अच्छी कथाकार हैं वही रहती हैं। इन सब से वेबीनार पर सहभागिता होती रहती है। शरद आलोक जी तो प्रो.डा. हरमहिन्दर सिंह बेदी जी (राष्ट्रपति पुरस्कृत) के साथ हमारे घर जालंधर में भी पधारे थे!
विदेश में बस रहे प्रवासी भारतीय अपने देश की साड़ी और अन्य वेशभूषाओं को त्योहार पर पहनते हैं और जींस पहन कर काम भी डट कर करते हैं l देश से बाहर रहकर भी वे अपने देश में जी रहे हैं और जहां जाते हैं एक छोटा सा या कह लो “मिनी हिंदुस्तान” बना लेते हैं l इसका स्पष्ट उदाहरण आपने देखा होगा टीवी पर जब मोदी जी ट्रंप के साथ” हाउडी” प्रोग्राम के लिए अमेरिका के हयूस्टन शहर में आए थे, तो भारतीय समूह उनके स्वागत में उमड़ पड़ा था l इन्हीं प्रवासी भारतीयों के कारण आज हिंदी का डंका यूनाइटेड नेशन तक बज रहा हैl
शैली, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

हिन्दी-दिवस का सार
ठान लें कि हिन्दी को मन से अपनायेंगे,
किसी एक बन्दे को हिन्दी सिखायेंगे,
अशुद्ध लिखते जो, उन्हें शुद्धता बतायेंगे,
नोटिस बोर्ड’ को, ‘सूचना-पट्ट’ बनायेंगे,
हिन्दी-दिवस का तब, सार समझ पायेंगे।
बच्चों को हिन्दी की वर्तिनी पढ़ायेंगे,
गीता, रामायण से परिचित करायेंगे,
भाषा व संस्कृति का, गौरव बतायेंगे
हम क्यों ग़ुलाम बने, कारण समझायेंगे
हिन्दी-दिवस का तब, सार समझ पायेंगे
हेलो-हाय, ओके-बाय सब भूल जायेंगे
प्रणाम,नमस्कार, विदा- आचरण में लायेंगे,
जन्मदिवस, प्रात, रात- हैप्पी ना होवेंगे,
शुभ, मंगल, साधुवाद, आशीष बोलेंगे,
हिन्दी-दिवस का तब, सार समझ पायेंगे
अंग्रेज़ी बोलने का रौब नहीं झाड़ेंगे
हिन्दी को पिछड़ों की, भाषा ना मानेंगे
हिन्दी में बोलते जब, आप ना लजायेंगे
हिन्दी को आप अपनी, अस्मिता बनायेंगे,
हिन्दी-दिवस का तब, सार समझ पायेंगे
आयोजन करने से, हिन्दी ना आयेगी,
कविताई करने से, हिन्दी ना भायेगी,
भारत के गौरव से, हिन्दी को जोड़ेंगे
अंग्रेज़ी पढ़कर भी, हिन्दी ही बोलेंगे
हिन्दी दिवस तब ही सार्थक कर पायेंगे
डॉ॰ अर्जुन गुप्ता ‘गुंजन’, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

हिंदी साहित्य की सामाजिक तथा लोकतान्त्रिक भूमिका
साहित्य का मूल तत्त्व सभी का हितसाधन है। साहित्य साधक अपने मन में उठने वाले भावों को जब लेखनीबद्ध करके भाषा के माध्यम से प्रकट करता है तब वह ज्ञानवर्धक अभिव्यक्ति के रूप में साहित्य कहलाता है। हिंदी साहित्य अतीत से प्रेरणा प्राप्त करता है, वर्तमान का चित्रण करता है तथा भविष्य का मार्गदर्शन करता है। साहित्यकारों ने अपने भावों को अपनी रचना के माध्यम से एक आकार दिया। यही साहित्यिक रचना समाज के नवनिर्माण में पथप्रदर्शक की महत्वपूर्ण भूमिका निभायी तथा लोकतंत्र की स्थापना व इसके विकास में भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया।
हिंदी साहित्य एक सशक्त माध्यम है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। जहाँ एक तरह यह सत्य के सुखद परिणामों को चिन्हित करता है, वहीं असत्य का दुखद अंत करके शिक्षा प्रदान करता है। सुसंगठित साहित्य व्यक्ति तथा उसके चरित्र निर्माण में सहायक होता है। इसलिए समाज के नवनिर्माण में साहित्य की मुख्य भूमिका होती है। हिंदी साहित्य में सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यों तथा विश्वाशों को प्रतिविम्बित करने की अपार शक्ति है। हिंदी साहित्य में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के साथ ही संस्कृतियों तथा संस्कारों को संरक्षित करने की शक्ति भी है। हिंदी साहित्यिक रचनाएँ सामाजिक तथा राजनितिक टिप्पणी के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहाँ पाठकों को सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। हिंदी साहित्य के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने तथा राष्ट्र में समता एवं न्याय का विकास करने की प्रेरणा मिलती है। हिंदी साहित्य की रचनाएँ अन्याय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करतीं हैं तथा कम जनसँख्या वाले समूहों के अधिकारों की बात उठाती हैं।
हिंदी साहित्य हमारे समाज को संस्कार प्रदान करने का कार्य करता है, महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है तथा विभिन्न कालखंडों की विसंगतियों एवं विरोधाभासों को चिन्हित करके हमारे समाज को सन्देश देता है, जिसके द्वारा समाज में सुधार आता है, जिससे सामाजिक चेतना को गति प्राप्त होती है। सामाजिक व्यवस्था तथा राष्ट्र के विकास में साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास गवाह है हमारे समाज में या राष्ट्र में जितने भी परिवर्तन आये हैं उन सब में हिंदी साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कबीरदास ने लिखा – “पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूँ पहाड़।” साहित्यकार समाज में फैली कुरीतियों, विषमताओं तथा विसंगतियों के बारे में लिखकर जनमानस को जागरूक करने का कार्य करता है। जब-जब हमारे समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आयी है, तब-तब हिंदी साहित्य ने मार्गदर्शन का कार्य किया है। हिंदी साहित्य का हमारे समाज तथा लोकतंत्र पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने अभिव्यक्ति के लिए अवसर तथा स्थान दिया, समझ तथा सहानुभूति को बढ़ावा दिया तथा आलोचनात्मक विचारधार को उत्तेजित करने का कार्य किया।
साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। दर्पण सिर्फ वाह्य आकृतियों, विकृतियों तथा विशेषताओं का दर्शन कराता है, जबकि साहित्य हमारे समाज की आतंरिक विकृतियों तथा विशेषताओं को चिन्हित करता है। समाज और साहित्य में अन्योनाश्रित सम्बन्ध होता है। साहित्य समाज की खामियों को चित्रित करने के साथ साथ उनका समाधान भी प्रस्तुत करता है। यथार्थ चित्रण तथा सामाजिक प्रसंगों की जीवंत अभिव्यक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य हमारे समाज का नवनिर्माण करता है। तुलसीदस, सूरदास, कबीरदास, मल्लिक मोहम्मद जायसी, रहीम, रसखान से लेकर भारतेन्दु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, दिनकर, निराला, प्रसाद तथा नागार्जुन तक की श्रंखला के रचनाकारों नें समाज के नवनिर्माण तथा उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी अनुपम सशक्त रचनाओं के माध्यम से उन्होंने शासनतंत्र के खिलाफ जाकर सामाजिक नवनिर्माण के लिए कदम उठाये। सर्वहारा वर्ग के दर्द को अपनी रचनओं के माध्यम से उजागर किया। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं – “जो दलित है, पीड़ित है, संत्रस्त है, उसकी साहित्य के माध्यम से हिमायत करना साहित्यकार का नैतिक दायित्व है।“ प्रेमचंद नें अपनी सभी रचनाओं में गरीबों, किसानो, मजलूमों की संवेदना का बड़ी संजीदगी से चित्रण किया। बीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को जनता का संचित प्रतिबिम्ब माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को ज्ञानराशि का संचित कोष कहा है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य को जनसमुदाय के ह्रदय का विकास कहा है।
साहित्य समाज का केवल दर्पण ही नहीं होता, बल्कि उसका दीपक भी होता है, जो समाज में फैली कुरीतियों, कुप्रथाओं तथा कुशासन को आलोकित करता है। साहित्य के आलोक से सामान में संचेतना का संचरण होता है। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता व संस्कृति को वहाँ के साहित्य के माध्यम से जाना जा सकता है। किसी साहित्यकार नें यह लिखा है – “अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं हैं। मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है।” हिंदी भाषा के साहित्यकारों नें अपनी लेखनी के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत का चित्रण किया है, समसामयिक सामाजिक गतिविधियों का सूक्ष्म चित्रण तथा विवेचन प्रस्तुत किया है तथा इस प्रकार समाज का सदैव मार्गदर्शन किया है। तुलसीदास, कबीरदास, भारतेन्दु, प्रेमचंद, निराला, मुक्तिबोध जैसे अनेकानेक साहित्यकारों नें साहित्य के माध्यम से समाज में करुणा, सदाचार, मानवीयता, परोपकार तथा बंधुत्व की भावना को स्थापित करने का सन्देश दिया। “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” की मूल भावना को केंद्र में रखकर इन्होने साहित्य सृजन किया।
पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे जीवन मूल्यों तथा आदर्शों को प्रभावित किया है। पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति के चकाचौंध में हमारे समाज में जो विकृति पैदा हो रही है उसके निराकरण के लिए आज के दौर में उत्कृष्ट तथा मार्गदर्शी साहित्य सृजन का तकाजा है। यह आवश्यक है कि हम साहित्य को नित नूतन आयाम दें, जिसके द्वारा हमारा प्राचीन वैभव पुनः कायम हो सके। मुक्तिबोध के अनुसार – “अब अभिव्यक्ति से सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब”। कट्टरवाद के खिलाफ भी साहित्यकारों को अपनी कलम उठानी पड़ेगी। समाज के प्रति हिंदी साहित्य का ईमानदार तथा जवाबदेह होना अति आवश्यक है। हिंदी कविता समाज से तभी जुड़ सकती है जब वह अभिव्यक्ति, अनुभूति, प्रतीति के स्तर पर पाठकों की संवेदना को छू सके। भारतवर्ष में जब आधुनिक भारतीय भाषाओँ का उदय तथा विकास हुआ, तब भक्ति आंदोलन के कालखंड के साहित्य ने पुरे देश में सामाजिक एकता का सूत्रपात किया। भक्ति काव्य चाहे हिंदी भाषा में लिखा गया हो या किसी और भाषा में, सभी का एक ही स्वर था – “जात-पात पूछे नहीं कोई, हरी को भजै सो हरी का होई।” इसी प्रकार से स्वाधीनता आंदोलन के कालखंड में पुरे भारतवर्ष में एक ही स्वर गूंज उठा – “मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढाने, जिस पथ जाएँ वीर अनेक।” कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक पुष्प की अभिलाषा ने भारतीयों की अभिलाषा का रूप ले लिया, तब जाकर अंग्रेजी राज का सूरज अस्त हुआ।
वर्तमान में हिंदी साहित्य-शिल्पियों ने देश की सामाजिक तथा लोकतान्त्रिक स्थिति का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। कई साहित्यकारों ने भारतवर्ष के अतीत का गौरव गान किया है तो कईयों ने अपनी रचनाओं में ललकार तथा गर्जना के साथ बलिदान की संवेदना को उद्घृत किया है। कईयों ने वर्तमान सामाजिक तथा लोकतान्त्रिक स्थिति की दुर्दशा का चित्रण किया है। राष्ट्रीयता की भावना के विकास में हिंदी के आधुनिक काल की रचनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। लोकतान्त्रिक भावना से राष्ट्रवाद को सम्बल प्राप्त होता है। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का यह कथन तर्कसंगत है – “हमारा देश विशाल राष्ट्र की भावना तथा संकल्पना के वैदिक युग से परिचित रहा है। हिंदी साहित्य समाज तथा लोकतंत्र की आतंरिक तथा बाह्य प्रगति के लिए हमेशा से कल्पवृक्ष बना हुआ है। साहित्य ने हमेशा खड़े होकर पीड़ितों के आँसू पोंछे हैं। हमारा हिंदी साहित्य मानव को बाहर तथा भीतर से परिष्कृत करने का कार्य करता आ रहा है। हिंदी साहित्य तन तथा मन दोनों को सभ्य बनाता है। वर्तमान हिंदी साहित्य प्राकृतिक राष्ट्रीयता का मानवीकरण नहीं करता, बल्कि यह समाज तथा देश को सामाजिक संदर्भो के साथ चिन्हित करने का प्रयास करता है। किसी कवि ने लिखा है – “जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह ह्रदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।”
भारतवर्ष में लोकतंत्र की स्थापना तथा विकास में हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका को नाकारा नहीं जा सकता है। लोकतंत्र का अर्थ है “लोगों का शासन”। लोकतंत्र राजनैतिक व्यवस्था की सबसे अच्छी तरकीब है। लोकतंत्र को बनाने तथा उसे कायम रखने में हिंदी साहित्य की अति विशिष्ट भूमिका है। वर्तमान में लोकतंत्र शासन की एक प्रणाली मात्र बन कर रह गयी है। हिंदी साहित्य लोकतंत्र को सांस्कृतिक-समाज के रूप में हासिल कर इसे एक उत्तम शैली के रूप में विकसित करना चाहता है। वर्त्तमान हिंदी साहित्य में लोकतान्त्रिक मूल्यों की स्थापना को लेकर स्पष्ट रूप से छटपटाहट दिखाई पड़ती है। आजादी के 78 वर्ष पुरे होने के बाद भी रोटी, कपडा और मकान की समस्या का हल नहीं हो पाना, लोकतान्त्रिक व्यवस्था के वास्तविक चेहरा को प्रस्तुत करता है। आज के हिंदी साहित्य में इसके प्रति संवेदना तथा आक्रोश दिखाई पड़ता है। जहाँ आज का साहित्यकार अपने साहित्य में वर्तमान के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करता है, वहीं देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक तथा लोकतान्त्रिक विसंगतियों पर प्रहार करता है। अपनी रचना के मध्य से हिंदी साहित्यकार सुधार की कामना करता है तथा पुनर्जागरण के लिए जनता का आह्वान करता है। लोकतंत्र को स्थापित करने और उसे बनाये रखने में हिंदी साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण साहित्य की भूमिका निर्विवाद है। स्वतंत्रता के पूर्व लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता के पश्चात् लोकतंत्र में बहुत बदलाव आ चुका है। आज अपने देश में स्वतंत्र लोकतंत्र का प्रभाव हिंदी साहित्य में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् साहित्यकारों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हुई है। वर्तमान में साहित्यकारों पर अधिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र की पहचान जनता के सुख दुःख से होती है।
आज के लोकतंत्र और हिंदी साहित्य पर विचार-विमर्श करना समकालीन परिवर्तन के दृष्टिगत अनिवार्य हो गया है। किसी भी देश का साहित्य वहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हिंदी रचनाकारों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो गयी। हिंदी साहित्य के कलमकारों ने सामाजिक तथा लोकतान्त्रिक विकास में बाधक बने तत्वों को जीवंत रूप में साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सामाजिक तथा लोकतान्त्रिक चेतना को अभिव्यक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य हिंदी साहित्य के साहित्यकारों ने कुशलता के साथ किया। आज हिंदी के साहित्यकारों पर बहुत अधिक जिम्मेदारी भी है। आज भी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जनता लोकतान्त्रिक अधिकारों के लिए तरस रही है। हिंदी के कवियों ने इसके प्रति जनता को जागृत करने का कार्य किया ह। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कालजयी कृति “रश्मिरथी” में लिखा है –
अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है।
न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।
इस कारण से ही कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ।
जो भव्य भारतवर्ष के उत्कर्ष का कारण हुआ।
प्रेमचंद ने लिखा है – “साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है।” साहित्यकार का जनसंपर्क तथा सोच व्यापक होता है। लेकिन आज के लोकतंत्र में साहित्यकारों की सोच बदल गयी है। आज का हिंदी साहित्यकार पद, लोभ, मोह, मुद्रा तथा साहित्यिक पुरस्कार पाने के लालच में अपने कर्त्तव्य से भटक गया है। रघुवीर सहाय की कविताओं में आज के लोकतंत्र की स्पष्ट झलक मिलती है। उनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है कि बहुत से परिवर्तन हुए है लेकिन जनता के दुःख-दर्द में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं है। उनका काव्य-संग्रह “आत्महत्या के विरुद्ध” में लोकतान्त्रिक मूल्यों के ह्रास का उल्लेख है। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने विख्यात उपन्यास “मैला आँचल” में लिखा है – “गरीबी और जहालत दो ऐसी बीमारी है, जिन्हे दूर करना बेहद जरुरी है।” समाचार-पत्र जिन्हे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है, वह स्वयं लोकतंत्र की हत्या में शामिल हैं। उन्हें अपनी भूमिका तथा अपने कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। कुछ ईमानदार मीडिया हाउस भी हैं जो अपने कर्त्तव्य-पथ पर अडिग हैं। आज भी समाज तथा लोकतंत्र के समग्र विकास के लिए हिंदी साहित्य के पुरोधाओं को समन्वित तथा संगठित होकर लेखन कार्य तथा जनजागरण का कार्य करना होगा। जय हिन्द, जय हिंदी !!
डॉ.पूर्णिमा, पटियाला (पंजाब)

हिन्दी का पूजन पग-पग है!!
हिन्दी से तन-मन खिल जाए।
हिन्दी से सब गम मिट जाए।।
हिन्दी भाषा अजर अमर है;
हर भाषा में घुल-मिल जाए।।
स्वर व्यंजन हम जब लिखते हैं।
दीप दिलों में तब जलते हैं।।
हिन्दी भाषा के गौरव से ;
विश्व पटल पर जन सजते हैं।।
भाषा को सम्मान दिलाएं।
बाल युवा वृद्ध को पढ़ाएं।।
हिन्दी को समृद्ध करें सभी;
भारत का आँगन महकाएं।।
बोल खड़ी बोली के कहते।
हिन्दी भाषी दिल में रहते।।
भाषा पर अधिकार जमा कर;
नदिया की धारा सा बहते।।
नवरस मीठा गान सुनाएं।
जीने का अरमान जगाएं।।
भाषा की दीवार तोड़कर;
हिन्द-प्रेम से भवन बनाएं।
ज्यों चाँद “पूर्णिमा” जग-मग है।
त्यों हिन्दी भाषा रग-रग है।।
महादेव के वंदन जैसा;
हिन्दी का पूजन पग-पग है।।
नन्दकुमार मिश्र आदित्य, चम्पारण (बिहार)

जय हिन्दी
जय हिन्दी जय हिन्द जयति जय
हम हिन्दी अपनायें निर्भय
हिन्दी हिन्दी हिन्दी हिन्दी
अखिल विश्व तब हो हिन्दीमय
सम्भाषण प्रारम्भमें जबतक ‘हेलो हाय’का हो खर्चा
जब तक ‘हैप्पी हिन्दी डे’ या ‘हैप्पी हिन्दी’-सी चर्चा
‘कङरेटा- कङरेटी’ ‘थैंकू-गुड मोरनिङ’ से गुड़-गोबर
तीन सौ चौंसठ दिनपर भारी हिन्दीदिवस तो बस मिर्चा
हिन्दी ही दौड़ेगी क्यों ना ? हिन्दी भी चल सकती क्या?
अब तक ना कर पाये, माना, अब तो लें संकल्प नया
अङरेजीकी बैसाखी पर कब तक होगा लंगड़ाना
आजादीका अमृताब्द भी आया, आकर चला गया
हिन्दी दिवस नहीं, हिन्दीयुग, हिन्दी हो आकल्प
आत्म-चेतना जग जाये जब मनमें हो संकल्प
राष्ट्र-जागरण राष्ट्र-चेतना सारा कुछ बेमानी
राष्ट्र जल्पना बिना राष्ट्रभाषा अनकही कहानी
हिन्दी भाषा मात्र नहीं है, यह अस्मिता हमारी
ऊर्जा शक्ति हमारी हिन्दी नहीं पंगुता लाचारी
संविधान से शब्द ‘इंडिया’ जबतक न हो निरस्त
ठूंठ गाछ हिन्दी बिन हिन्द, भारत अस्त-व्यस्त
दिया राष्ट्रभाषा का दर्जा हमने अगर नहीं इस वक़्त
राष्ट्रभक्ति का मानें कैसे दौड़ रहा रग-रगमें रक्त ?
उर्मिला यादव ‘उर्मि’, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
हिन्दी भारत भाल की बिन्दी
हिन्द से हिन्दी,हिन्दी से हिन्दुस्तान पहचान हमारी।
सबसे प्यारी न्यारी है हिंदी भारत भाल की बिन्दी।।
सरल सरस और सुहावनी कोयल-सी मीठी बोली।
जैसी कथनी वैसी करनी कर अंग्रेजी पोल खोली।।
भाषाओं की सरताज सूरत में लगती बड़ी भोली।
सबसे प्यारी न्यारी है हिंदी भारत भाल की बिन्दी।।
प्रथम वैज्ञानिक लिपि जिसकी महिमा अमित अपार।
दामन में है जिसके शब्दों और भावों का भरा भंडार।।
सुन्दरता में चार चाॅंद लगाते हैं छंद और अलंकार।
सबसे प्यारी न्यारी है हिंदी भारत भाल की बिन्दी।।
संस्कृत सुता ब्राह्मी से विकसित भारत राज दुलारी।
बोली में रखती तीजा स्थान माने दुनियाॅं यह सारी।।
रचकर साहित्य अनूठा हो गई जग में सब पर भारी।
सबसे प्यारी न्यारी है हिंदी भारत भाल की बिन्दी।।
दो अयोगवाह, ग्यारह स्वर और तेंतीस व्यंजन।
दो द्विगुण। चार संयुक्त और एक विशिष्ट व्यंजन।।
जब मिल जाऍं सारे तब बन जाता कुनबा तरेपन।
सबसे प्यारी न्यारी है हिंदी भारत भाल की बिन्दी।।

डॉ अनीता वर्मा जी नमस्कार ।
परिश्रम पूर्वक इस अंक का सम्पादन हुआ है । साधुवाद । पत्रिका के माध्यम से देश विदेश में हिन्दी के प्रचार प्रसार से मन उत्साहित व प्रफुल्लित होता है । विदेशी धरती पर हिन्दी के बढ़ते कदम निश्चित सुखद भविष्य की बढ़ते नजर या रहे हैं । मेरा विनम्र निवेदन है कि कभी हिन्दी भाषा की अपनी कठिनाइयों पर भी चर्चा होनी चाहिए । आगत शब्दों की किस सीमा तक स्वीकार्यता उचित है ,इस पर भी विचार आवश्यक प्रतीत होता है ।
पुन: साधुवाद ।
डॉ वेद व्यथित