
इस श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेषांक में अनीता वर्मा– संपादकीय; नर्मदा प्रसाद उपाध्याय–दिल्ली; डॉ. वरुण कुमार–दिल्ली; नरेन्द्र कोहली; डॉ. संध्या सिलावट- मध्य प्रदेश; डॉ शिप्रा शिल्पी सक्सेना– जर्मनी; डॉ॰ जयशंकर यादव- कर्नाटक; श्रीमती सुमन माहेश्वरी- फरीदाबाद; डॉ महादेव एस कोलूर– कर्नाटक; कात्यायनी डॉ पूर्णिमा शर्मा–दिल्ली; हरिहर झा- आस्ट्रेलिया; अजेय जुगरान; डॉ सुनीता शर्मा- ऑस्ट्रेलिया; डॉ अरुणा गुप्ता– दिल्ली; डॉ रमा सिंह- जयपुर; लीला तिवानी- नई दिल्ली की रचनाएँ संकलित हैं।
- अनीता वर्मा – संपादकीय
- नर्मदा प्रसाद उपाध्याय – मानव इतिहास का महानायक : कटे जंजीर खुले दरवाजे… (आलेख)
- डॉ. वरुण कुमार – भारतीय कलाओं में कृष्ण (आलेख)
- नरेन्द्र कोहली – वह आ गया है (आलेख)
- डॉ. संध्या सिलावट – श्रीकृष्ण और उनकी व्यापकता (आलेख)
- डॉ शिप्रा शिल्पी सक्सेना – जर्मनी में गुंजायमान : जय कन्हैया लाल की (आलेख)
- डॉ॰ जयशंकर यादव – कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम (आलेख)
- श्रीमती सुमन माहेश्वरी – श्री कृष्ण की महिमा (आलेख)
- डॉ महादेव एस कोलूर – बंशी (आलेख)
- कात्यायनी डॉ पूर्णिमा शर्मा -कृष्ण कथा (कविता)
- हरिहर झा – केशव रहे पुकार (कविता)
- अजेय जुगरान – बाँसुरी में कान्हा (कविता)
- डॉ सुनीता शर्मा – प्रेम, भक्ति और जीवन के रंग में रंगी जन्माष्टमी (कविता)
- डॉ अरुणा गुप्ता – दिल्ली ६ – दिन जन्माष्टमी के (कविता)
- डॉ रमा सिंह – दोहे कृष्ण जन्म पर (कविता)
- लीला तिवानी – आए मेरे श्याम सखी खुशियां मनाओ री (कविता)
संपादकीय
अनीता वर्मा

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब मैं प्रकट होता हूँ। गीता में ये कहने वाले कृष्ण भारतीय जनमानस से इस तरह से जुड़े हैं कि हर भारतीय देश में हो या विदेश में उनकी भक्ति के रंग में रंग जाता है। अपने साथ होने वाले अन्याय पर उन्हें याद करता है। जब भी स्वयं को दुविधा में पाता है अपने भीतर की छटपटाहट से मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे जीवन के इस कारागार से मुक्त करो। हर क्षण, हर पल वह स्वयं को उनसे जुड़ा हुआ पाता है। कृष्ण उनको अपने जैसे लगते हैं। वो हर पल उनसे संवाद करता हैं। कृष्ण उन्हें एक ऐसे छोटे बालक दिखते हैं जो अपनी बालपन की लीलाओं मन को मोह लेते हैं , इस नटखट बालपन में वो अपने घर के नन्हें -मुन्ने बच्चों को देखता हैं। जन्माष्टमी पर अपने बच्चों को कृष्ण और राधा के स्वरूप में तैयार करना यहीं संवाद तो है।
कृष्ण ने जहां एक तरफ़ कर्म को सर्वोपरि बताते हुए सदैव निष्काम भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित किया है वहीं दूसरी तरफ़ अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने के लिए भी प्रेरित किया है। नए सामाजिक मूल्यों व धार्मिक मान्यताओं के स्थापित करने वाले कृष्ण के रंग में ना केवल भारतीय अपितु विदेशी भी रंगें हुए हैं। शंखनाद के साथ, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए कृष्ण जीवन से मृत्यु तक हर बार नए संदर्भो में नए आयाम स्थापित करते हुए नवीन संकल्प व प्रेम का संदेश देते हैं।
वैश्विक हिंदी परिवार का यह विशेषांक भी कृष्णमय और बहुत विशिष्ट है क्योंकि अगर कृष्ण पर रचनात्मकता की बात हो रही हो तो साहित्यकारों में सबसे स्वत: ही स्मरण में पहला नाम आदरणीय डॉ श्री नरेन्द्र कोहली जी का आता है। उनका ये विशेष आलेख हमारे विशेष आग्रह पर उनकी पत्नी डा. मधुरिमा कोहली जी ने हमें भेजा है।
साथ ही इसमें सभी सम्मानित लेखकों की रचनाएँ सम्मिलित हैं जिनमें कृष्ण के जीवन के सभी अध्याय सम्मिलित हैं जो हम सबके जीवन का आधार हैं। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ वात्सल्य, राधा के प्रेम का श्रृंगार और मीरा की भक्ति तो है ही, साथ ही जीवन जीने की प्रेरणा भी है।
इन्हीं सब रंगों से कृष्ण के प्रेम से सिंचित ये विशेषांक आप सबके समक्ष।
नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, दिल्ली

मानव इतिहास का महानायक : कटे जंजीर खुले दरवाजे….
आपने कभी सोचा है, कि वे जेल में ही क्यों जन्मे?
भादो की काली अँधेरी रात में जब वे आये, तो सबसे पहला काम यह हुआ कि जंजीरे कट गयीं। जन्म देने वाले के शरीर की भी, और कैद करने वाली कपाटों की भी। वस्तुतः वह आया ही था जंजीरे काटने… हर तरह की जंजीर!
जन्म लेते ही वह बेड़ियां काटता है। थोडा सा बड़ा होता है, तो लज्जा की जंजीरे काटता हैं। ऐसे काटता है कि सारा गांव चिल्लाने लगता है- कन्हैया हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। सब चिल्लाते हैं- बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं, लड़कियां सब… कोई भय नहीं, कोई लज्जा नही!
वह प्रेम के बारे में सबसे बड़े भ्रम को दूर करता है, और सिद्ध करता है कि प्रेम देह का नही हृदय का विषय है। माथे पर मोरपंख बांधे आठ वर्ष की उम्र में रासलीला करते उस बालक के प्रेम में देह है क्या? मोर पंख का रहस्य जानते हैं? मोर के सम्बन्ध में लोक की एक प्राचीन धारणा है कि वह मादा से शारीरिक सम्बन्ध नही बनाता। मेघ को देख कर नाचते मोर के मुह से गाज़ गिरती है, और वही खा कर मोरनी गर्भवती होती है। यह वैज्ञानिक रूप से सत्य न भी हो, पर युगों से लोक की मान्यता यही रही है। माथे पर मोर मुकुट बांधे वह बालक इस तरह स्वयं को गोस्वामी सिद्ध करता है। वह एक ही साथ “पूर्ण पुरुष” और “गोस्वामी” की दो परस्पर विरोधी उपाधियाँ धारण करता है।
कुछ दिन बाद वह समाज की सबसे बड़ी रूढ़ि पर प्रहार करता है, जब पूजा की पद्धति ही बदल देता है। अज्ञात देवताओँ के स्थान पर लौकिक और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा को प्रारम्भ कराना उस युग की सबसे बड़ी क्रांति थी। वह नदी, पहाड़, हल, बैल, गाय, की पूजा और रक्षा की परम्परा प्रारम्भ करता है। वह इस सृष्टी का पहला पर्यावरणविद् है।
थोडा और बड़ा होता है तो परतंत्रता की बेड़ियां काटता है, और उस कालखंड के सबसे बड़े तानाशाह को मारता है। ध्यान दीजिये, राजा बन कर नही मारता, आम आदमी बन कर मारता है। कोई सेना नहीँ, कोई राजनैतिक गठजोड़ नहीं। एक आम आदमी द्वारा एक तानाशाह के नाश की एकमात्र घटना है यह।
इसके बाद वह सृष्टि की सबसे बड़ी बड़ी पुरुषसत्ता पर प्रहार करता है। तनिक सोचिये तो, आज अपने आप को अत्याधुनिक बताने वाले लोग भी क्या इतने उदार हैं कि सामाज की परवाह किये बगैर अपनी बहन को अपनी गाड़ी पर बैठा कर उसके योग्य प्रेमी के साथ विदा कर दे? पर वह ऐसा करता है। ठीक से सोचिये तो स्त्री समानता को लागु कराने वाला पहला व्यक्ति है वह। वह स्त्री की बेड़ियां काटता है।
कुछ दिन बाद वह एक महान क्रांति करता है। नरकासुर की कैद में बंद सोलह हजार बलात्कृता कुमारियों की बेड़ी काट कर, और उनको अपना नाम दे कर समाज में रानी की गरिमा दिलाता है।
फिर वह उंच नीच की बेड़ियां काटता है और राजपुत्र हो कर भी सुदामा जैसे दरिद्र को मित्र बनाता है, और मित्रता निभाता भी है। ऐसा निभाता है कि युगों युगों तक मित्रता का आदर्श बना रहता है।
फिर अपने जीवन के सबसे बड़े रणक्षेत्र में अन्याय की बेड़ियां काटता है। कहते हैं कि यदि वह चाहता तो एक क्षण में महाभारत ख़त्म कर सकता था। पर नहीं, उसे न्याय करना है, उसे दुनिया को बताना है कि किसी स्त्री का अपमान करने वाले का समूल नाश होना ही न्याय है। वह स्वयं शस्त्र नहीं छूता, क्योकि उसे पांडवों को भी दण्डित करना है। स्त्री आपकी सम्पति नही जो आप उसको दांव पर लगा दें, स्त्री जननी है, स्त्री आधा विश्व् है। वह स्त्री को दाव पर लगाने का दंड निर्धारित करता है, और पांडवों के हाथों ही उनके पुर्वजों का वध कराता है। अर्जुन रोते हैं, और अपने दादा को मारते हैं। धर्मराज का हृदय फटता है पर उन्हें अपने मामा, नाना, भाई, भतीजा, बहनोई को मारना पड़ता है। अपने ही हाथों अपने बान्धवों की हत्या कर अपनी स्त्री को दाव पर लगाने का दंड वे जीवन भर भोगते हैं। वह न्याय करता है। वह अन्याय की बेड़ियां तोड़ता है।
*वह मानव इतिहास का एकमात्र नायक है। वह महानायक है, रियल हीरो है।
डॉ. वरुण कुमार, दिल्ली

भारतीय कलाओं में कृष्ण
भारत के साहित्य समेत समस्त कला रूपों में कृष्ण को प्रमुख स्थान मिला है। कृष्ण की मानवीय भूमिका अत्यंत विविधतापूर्ण और विपरीत ध्रुवों को समेटनेवाली है। वे प्रेमी भी हैं, योगी भी हैं, रणनीतिकार भी हैं, रणछोड़ भी हैं, योद्धा भी हैं। वे अध्यात्मपुरुष भी हैं और कामनाओं के तीव्रतम भोग के आलम्बन भी। वे सबकुछ छोड़कर चल देनेवाले त्यागी भी हैं और जीवन के जंजालों में उलझनेवाले लोक पुरुष भी। इसलिए उनकी लीलाओं में कवियों, कलाकारों को भावनाओं के वैविध्य को व्यक्त करने का प्रचुर अवसर मिलता है। भारतीय धर्म, दर्शन, कलाएँ सबमें उनकी व्यापक उपस्थिति है। प्राचीन और मध्यकालीन काव्य का धर्म और दर्शन से जैसा गहरा नाता रहा है, उसमें यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
कृष्ण को कलापुरुष कहा जाता है। कला के जितने उपादान हैं वे सब कृष्ण में समाहित हैं। भागवत पुराण में एवं अन्य कई ग्रंथों में उन्हें सोलह कला सम्पूर्ण पुरुष कहा गया है। किंतु वहाँ ये सोलह कलाएँ अवतारी पुरुष के दिव्य गुण हैं। आज हम कला का जो अर्थ लेते हैं – वह है ललित कला – यानि काव्यकला, चित्रकला, संगीत, नृत्यकला, मूर्तिकला, अभिनयकला वगैरह। इन सभी में कृष्ण छाए हुए-से हैं। आप भारत के किसी भी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जाएँ, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या कर्नाटकी संगीत, वहाँ कृष्ण को लेकर बनी बंदिशों और पदों का गायन सुनने को मिल ही जाएगा। प्राचीन ध्रुपद में शिव और गणेश की आराधना होती है लेकिन सबसे अधिक कृष्ण की लीलाओं का गायन होता है। लोकसंगीत में भी कृष्ण और राधा की छेड़छाड़, विरह, उपालंभ आदि का वर्णन सर्वाधिक होता है। भारत में हर दूसरे घर में कृष्ण की छवियाँ और कृष्ण की पेंटिंग सजी हुई मिल सकती हैं। ऐसा व्यक्तित्व संभवतः संसार में दूसरा नहीं। उत्तर प्रदेश का वृंदावन-मथुरा तो कृष्ण की बाल्यकाल और यौवनकाल की लीलाओं का क्षेत्र ही है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में उज्जैन, तो गुजरात में द्वारका, पश्चिम की ओर जाएँ तो पुण्डरीक तक यानी महाराष्ट्र में कृष्ण पहुँचे हुए हैं। दक्षिण में श्रीरंगम अगर विष्णु का क्षेत्र है तो कृष्ण का भी क्षेत्र माना जाता है। श्रीशैलम, श्रीरंगपट्टणम आदि कृष्णोपासना के लिए प्रसिद्ध हैं, और वहाँ उनके मंदिरों में संगीत, नृत्य, चित्रों, मूर्तियों, अभिनय आदि कला माध्यमों के आलम्बन बनते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र तो इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। असम, मणिपुर, बंगाल अगर तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र रहा तो साथ-साथ कृष्णोपासना की भी सबसे प्रिय भूमि। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रसिद्ध है कि वे कृष्ण की क्रीड़ाओं से संबंधित जयदेव की पदावली का गायन करते करते बेसुध हो जाते थे। गीतगोविंदकार जयदेव वर्तमान उड़ीसा क्षेत्र के हैं। उड़ीसा का पूरा क्षेत्र कृष्णोपासना का है। वहाँ के पुरी मंदिर में कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। गीतगोविंद विशेषकर संगीत और नृत्य की दुनियाँ में सबसे समादृत ग्रंथ है। गीतगोविंद की पदावलियों का आज भी बहुलता से गायन होता है, उनपर नृत्य होता है। मुझे याद आती है बचपन में अपने गाँव की कीर्तन मंडली में मेरे बड़े पिताजी और उनके दोस्तों का ‘धीर समीरे गंगा तीरे बसति बने बनमाली’ का हारमोनियम, झाल और मृदंग पर गायन। पूरी मंडली एक साथ गीत गोविन्द को गाती थी। सबों को उसके छंद याद थे। कुछ वैसे ही जैसे बंगालियों को रवीन्द्र संगीत उनके होठों पर रहता है और वे उसे समवेत रूप से गाते हैं। आज बिहार से वह पीढ़ी और वह परम्परा विलुप्त सी है। चित्रकला में भी गीतगोविंद को विशेष स्थान हासिल है। इसके छंदों पर आधारित चित्रों की श्रृंखलाएँ बनीं और बन रही हैं। मंदिर हमारे यहाँ धर्म-साधना और उपासना के केन्द्र रहे हैं। मंदिरों के माध्यम से मूर्तिकला और वास्तुकला में भी कृष्ण को व्यापक स्थान मिला है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का अभी उल्लेख हुआ। अपार भारतीय जनसमुदाय ने मंदिरों के माध्यम से गूढ़ अपने धार्मिक-दार्शनिक विचारों-मान्यताओं और आख्यानों को मूर्त रूप दिया है और अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है।
थोड़ा इतिहास की ओर दृष्टि डालें। प्राचीनता की दृष्टि से चित्रकला के क्षेत्र में कृष्ण का अंकन कम से कम ढाई हजार वर्ष पूर्व से मिलना शुरू हो जाता है – शैल चित्रों के रूप में अत्यंत प्राचीन युग से। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में ग्वालियर से लगभग ७० किलोमीटर दक्षिण में टिकला में शैल चित्रों में कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन की एक शैलचित्र मिलता है। चित्र के ऊपर शिला की सतह पर अत्यंत प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा है। हैदराबाद के राज्य संग्रहालय में एक महत्वपूर्ण पंचमूर्ति रखी हुई है जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कोंडामोटू में मिली थी। इस पंचमूर्ति में सभी पाँच वृष्णि व्रजों को उनके वंशावली क्रम से उकेरा गया है – संकर्षण, वासुदेव कृष्ण, नरसिंह, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। यह मूर्ति तीसरी/चौथी शताब्दी के अंत की है। मध्य युग के दौरान भारतीय चित्रकला पर फारसी प्रभाव पड़ा किंतु चित्रों के विषय में कृष्ण छाए रहे। जिस रीतिकाव्य की हम विलासप्रियता के कारण आलोचना करते हैं उसे कृष्ण की श्रृंगारिक क्रीड़ाओं ने मनोनुकूल विषय प्रदान किया। विशेषकर होली खेलने का विषय तो क्या काव्य, क्या चित्र, क्या नृत्य, सबमें अत्यंत प्रिय रहा। आधुनिक काल में भी रवींद्रनाथ ठाकुर और अन्य आधुनिक चित्रकारों ने भी श्रीकृष्ण को अपनी कला के माध्यम से जीवित किया है। मकबूल फिदा हुसैन ने कृष्ण की छवि को अपने चित्रों में अनूठे और आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया है। सतीश गुहो एक समकालीन चित्रकार हैं जिन्होंने कृष्ण के विभिन्न रूपों और भावनाओं को अपने चित्रों में चित्रित किया है। इसी तरह वर्तमान में प्रणय वाजपेयी, रघुवीर सिंह आदि ने कृष्ण की पूजा, लीलाओं को, उनके विविध पक्षों को चित्रित करने के लिए अपनी कलात्मक दृष्टि का उपयोग किया है।
नृत्य के तीन अंग हैं – नृत्त और नाट्य और संगीत। नृत्त जहाँ अंगों से मुद्राओं की निर्मिति, उनके संयोजन और संचालन का पक्ष है, नाट्य उसका अभिनय का पक्ष है। इन तीनों अंगों में, विशेषकर नाट्य में, नर्तक-नर्तकी द्वारा नवरस यानी नौ रसों की अभिव्यक्ति के लिए कृष्ण की कथा का ही आधार लिया जाता है। गायक कृष्ण से संबंधित पद या बंदिश गाता है और नृत्य करनेवाला या वाली उसे नृत्य करके उसके भावों को व्यक्त करता है। कत्थक में तो दरबारीपन ज्यादा है, लेकिन इससे गंभीरतर शास्त्रीय नृत्य शैलियों, जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुडि, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी आदि सभी में ऐसा देखने को मिलेगा। विशेषकर मणिपुरी की, ओडिसी की और मोहिनीअट्टम की तो कृष्ण के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती। जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा-वृंदावन आदि सभी प्रमुख मंदिरों में कृष्ण की लीलाओं का गायन और नर्तन होता है। विशेषकर उत्तर भारत में शहर-शहर, गाँव-गाँव में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होते हैं। मेरे शहर मुंगेर में, सावन के महीने में झूलन का त्योहार चलता है, जिसमें शहर के अभिजात वर्ग (डॉक्टर-इंजीनियर-डीएम कलेक्टर) से लेकर अनाज के आढ़तिए व्यापारी तक शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हैं। शास्त्रीय संगीत के ये कार्यक्रम मंदिर में, पुराने राजा के राजमहल की बैठकी में, किसी के घर में तो अनाज के आढ़त गोला में ही आयोजित होते हैं। जन्माष्टमी के दिन इसका समापन होता है। कृष्ण आज भी, हमारी तमाम आधुनिकता और धर्मनिरपेक्षता और प्रगति के बावजूद, हमारे मनोमय जगत के लीलापुरुष हैं।
कृष्ण की जो लीलाएँ काव्य में, चित्रों में छायी रही हैं उनमें प्रमुख हैं – उनकी बाल लीलाएँ, यमलार्जुन मोचन, कालिय मर्दन, गोवर्धन धारण, बकासुर वध, शिशुपाल वध, सुदामा प्रसंग, यौवन लीलाएँ, रुक्मिणी हरण, विराट रूप प्रदर्शन और महाभारत प्रसंग जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में कृष्ण-अर्जुन संवाद गीता का उपदेश प्रमुख है आदि। इन लीलाओं का मूर्तिकला में भी बहुधा उपयोग हुआ है। शिल्पकारों ने भगवान कृष्ण के रूप-सौंदर्य को उनके बाल रूप, बाँसुरी बजाते हुए पीताम्बर सज्जित रूप, राधा के साथ उनकी युगल मूर्ति आदि के जरिए मूर्त किया है। उन्होंने कृष्ण की सौम्यता, भव्यता और भक्ति की भावनाओं को विभिन्न आभूषणों, वस्त्रों और अभिव्यक्तियों के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है। ये मूर्तियाँ भारतीय मंदिरों और पूजा स्थलों की शोभा बढ़ाती हैं और जन-मन को आस्था और प्रेरणा प्रदान करती हैं। संगीत में उनकी बाल लीलाओं और यौवन लीलाओं को विशेष प्रमुखता मिली है। यह उल्लेख सिर्फ इस बात की ओर इशारा करता है इन कलाओं में इन लीलाओं की बारम्बारता या परिमाण अधिक है। अन्यथा कृष्ण से जुड़ा हर प्रसंग हमारे काव्य और कलाओं में वर्णित चित्रित हुए हैं। क्यों न हो, वे हमारे जातीय नायक हैं।
नरेन्द्र कोहली
प्रस्तुति- डॉ मधुरिमा कोहली
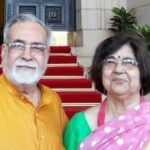
वह आ गया है
”बोलो वीरभद्र ! क्या समाचार लाए हो।”
”तो आपने पहचान ही लिया।” वीरभद्र मुस्कराया, ”हम दोनों की परीक्षा हो गई। आपकी दृष्टि समर्थ है; और मेरी वेश-परिवर्तन कला अभी इतनी सधी हुई नहीं है।…”
”क्या समाचार है ?” वसुदेव की इन बातों में कोई रुचि नहीं थी।
”स्वामी ! बलराम और देवी रोहिणी सकुशल हैं। किंतु पता नहीं क्यों कंस, नंद के पुत्र कान्हा से प्रसन्न नहीं दीखता। कंस नहीं चाहता कि कान्हा स्वस्थ और शक्तिशाली बने। वह उसके विरुद्ध कुछ न कुछ तो करता ही रहता है। आपने शकट, पूतना, तृणावर्त इत्यादि की घटनाएं सुन ही ली होंगी। किंतु अब एक नई बात हुई है।”
”क्या है वह ?” देवकी भी पूर्ण तन्मयता से सब कुछ सुन रही थीं।
”बालक क्रीड़ा के लिए जाते तो प्रतिदिन ही हैं; किंतु इधर ताप और उमस के कारण वे कंदुक-क्रीड़ा के लिए यमुना-तट पर चले गए।
*****
मनसुखा ने कंदुक पकड़ लिया।
”अरे क्या हुआ ?” सबने एक साथ ही पूछा।
”कान्हा ! मां ने कहा था कि कालिय-दह के निकट मत जाना।” मनसुखा ने कहा।
”तो मत जा न!” कान्हा ने कहा, ”कंदुक क्यों पकड़ लिया ?”
”हम कालिय-दह के निकट ही तो खेल रहे हैं।” मनसुखा बोला, ”कालिय नाग किसी समय भी दह से निकल कर आ सकता है। वह न भी आए। हमारा कंदुक ही दह में जा सकता है।”
”अरे तू कंदुक तो फेंक भाई ! यह तो हर समय अपनी आशंकाओं से ही पीड़ित रहता है।”
”जाने तुम लोग इस प्रकार हठ क्यों करते हो।” मनसुखा चिढ़ कर बोला, ”और कोई स्थान नहीं है क्या खेलने को। कालियदह के तट पर ही खेलना क्यों आवश्यक है ?”
”तुम इतने उद्विग्न क्यों हो मनसुखा ?”
”कंदुक की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। मुझे तो केवल यही ध्यान आता रहता है कि हम से थोड़ी ही दूर, उस जल के भीतर एक भयंकर नाग रहता है, जो किसी भी क्षण बाहर आ सकता है।”
”अरे तो हमारे समाज में नाग वह अकेला ही है क्या ? और भी तो हैं, जो निरंतर दूसरों को दंश करते रहते हैं। समाज में विष फैलाते रहते हैं।”
”हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए न !” मनसुखा ने अपनी मां के शब्द दुहरा दिए।
”उनसे भयभीत होकर दूर भागते रहना चाहिए ? उनका सामना नहीं करना चाहिए ?”
”अरे वह नाग है। सारा दह उसके विष से विषैला हो गया है। कोई उस जल को पिए तो ही मर जाए।”
”तुम उससे दूर भाग जाओगे तो दह का जल अमृत में नहीं बदल जाएगा, दह के तट की धरती भी विषैली हो जाएगी।”
”तुम यह क्यों नहीं कहते कान्हा ! कि तुम कालिय को मार देना चाहते हो, इसीलिए जानबूझ कर यहां खेल रहे हो ?” मधुमंगल ने कहा।
”अरे वह तो निर्बुद्धि जीव है। उसे क्या पता है कि उसके काटने से किसी को क्या हो जाता है, पर हम तो मनुष्य हैं। हमें ही कुछ समझदारी से काम करना चाहिए। हम क्यों उसके निकट जाते हैं ?”
”बोलो कान्हा ! दो उत्तर।”
”हमारा झगड़ा कराना चाहते हो ?” कान्हा हंसा, ”देखो अग्निदत्त ! हम मनुष्य हैं, इसीलिए विधाता के सारे जीवों के साथ शांति से रहते हैं। वैसे भी हम गोपाल हैं। क्या हमने गऊ से कभी शत्रुता की ? वह हमारी देखभाल करती है, हम उसकी देखभाल करते हैं। हम अश्वों के भी मित्र है। कुकुर भी हमारे समाज का अंग बन कर ही रहते हैं। हमारे पास कितने ही पक्षी भी हैं।”
”तो फिर हम नागों के ही शत्रु क्यों हैं ?”
”हम तो कालिय नाग को भी कुछ नहीं कह रहे। कंदुक जाकर दह में गिर जाएगा तो हम कंदुक को निकाल लाएंगे। दह तो सबका है। वह उसपर अपना एकाधिकार क्यों समझता है। जो सार्वजनिक संपत्ति को हड़पेगा, वह समाज का मित्र कैसे हो सकता है।”
सिर पर मटकी लिए हुए पद्मा उधर से आ निकली।
”अरे तुम लोग फिर कालियदह के निकट आ गए। नंद राय से कह दूंगी। कान्हा तू ही इन सबको ले आया होगा।”
”आजकल सारी गोपियां स्वयं को कान्हा की मैया ही समझती हैं। सबको अधिकार मिल गया है उसे धमकाने का।” श्रीदामा ने कहा।
”इसे तो मैं अभी ठीक करता हूं।” मनसुखा ने कहा।
मनसुखा ने उसकी मटकी का निशाना लगा कर कंदुक मारा। तब तक वह दो पग बढ़ा चुकी थी। लक्ष्य ठीक नहीं बैठा और कंदुक जाकर दह में गिर गया।
सब स्तब्ध खड़े रह गए।
”जाकर बताती हूं मैं तेरी मैया को मनसुखा ! कि तूने जानबूझ कर कंदुक दह में फेंका है।” पद्मा अधिकारपूर्वक बोली, ”चल कान्हा ! तू मेरे साथ घर चल।”
इससे पहले कि पद्मा उसे पकड़ ले, कान्हा भाग कर दह के तट पर उगे हुए कदंब के वृक्ष पर चढ़ गया।
पद्मा चिल्लाई, ”अरे तू क्या कर रहा है कान्हा ?”
कान्हा ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और कदंब से दह में कूद पड़ा।
पद्मा दहल गई : यह क्या क्या कान्हा ने !
ग्वालबाल जड़ काठ के समान खड़े रह गए।
पर पद्मा को जैसे कोई दौरा पड़ गया, ”अरे दौड़ो। जा कर नंद राय को सूचना दो। यशोदा को बताओ कोई जा कर कि कान्हा कालिय दह में कूद गया है।”
पद्मा की जिह्वा ही नहीं, उसके पग भी चल पड़े। वह ग्राम की ओर भागी। ग्वालबाल भी बिना किसी योजना के चारों दिशाओं में सहायता की खोज में भाग गए।
*****
देवकी ने जैसे अपने हाथों से अपना कलेजा थाम रखा था, ”फिर क्या हुआ ?”
”होना क्या था। नंद, यशोदा, गोप और गोपियां भागते हुए आए। सब लोगों ने चिल्ला-चिल्ला कर कान्हा को पुकारा। …कान्हा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। कालियदह में एक प्रकार का सन्नाटा था; और तट के वृक्ष स्तब्ध खड़े थे। यशोदा सब से आगे भागती हुई आई थीं। वे कान्हा को पुकार कम रही थीं, रुदन अधिक कर रही थीं। … और नंद यशोदा को पुकार रहे थे। किंतु वे सब से आगे थीं और दह के निकट थीं। तभी पीछे से नंद ने आ कर उन्हें पकड़ लिया, नहीं तो वे दह में कूदने को पूरी तरह प्रस्तुत थीं।
यशोदा छूटने के लिए हाथ-पैर मार रही थीं।
”छोड़ो मुझे। मैं तुम लोगों के समान पाषाण-हृदया नहीं हूं। मैं स्वयं लड़ लूंगी कालिय से। वह नाग ही तो है, कोई यमराज तो नहीं है।”
नंद समझा रहे थे, ”कुछ तो धीरज रख यशोदा ! हम अभी कुछ न कुछ प्रबंध करते हैं।”
यशोदा लड़ पड़ीं, ”क्या प्रबंध करोगे ? तट पर खड़े देखते रहोगे और नि:श्वास छोड़ते रहोगे। छोड़ो मुझे। मुझे कान्हा के बिना नहीं जीना है।”
यशोदा ने झटके से अपनी बांह छुड़ा ली। नंद ने लपक कर उन्हें पुन: पकड़ लिया। उनकी इस छीन- झपट के बीच ही कान्हा दह में से प्रकट हो गया। वह कूद कर तट पर आ गया। उसके हाथ में कंदुक था। यशोदा नंद को झटक कर कान्हा के पास पहुंचीं, ”कहां गया था तू ?”
कान्हा ने अबोध बालक के समान हाथ बढ़ा कर कंदुक दिखा दिया, ”अपना कंदुक लेने मैया ! कंदुक नहीं मिलता तो तुम मुझे दंडित करती न ! इस बार ऊखल से नहीं बांधतीं, किसी वृक्ष से बांध देतीं।”
यशोदा हंस नहीं पाईं, ”और कोई नहीं था कंदुक लाने वाला। सब जगह तुझे ही जाना होता है ?”
कान्हा हंसा, ”श्रेष्ठ पुरुष जो-जो करता है, सामान्य जन भी वैसा ही करते हैं; जो कुछ वह प्रमाणित करता है, साधारण जन उसी का अनुसरण करते हैं।… तो फिर मैं अपने मित्रों को कायरता का पाठ कैसे पढ़ा सकता था ? मैं पाप से लड़ूंगा, तो ही तो वे भी लड़ पाएंगे।”
”तू पाप से लड़ने आया था या कंदुक खेलने ?” यशोदा अपने असहाय क्रोध से मुक्त नहीं हो पा रही थीं।
”पाप से लड़ना ही तो मेरी कंदुक-क्रीड़ा है मैया।” कान्हा मुस्कराता जा रहा था।
*****
वसुदेव देख रहे थे कि वीरभद्र के इस सारे वर्णन को सुन कर देवकी उद्विग्न होती जा रही थीं। अभी तक तो वे संतुलित थीं; किंतु संभव था कि वे स्वयं को संभाल न पाएं और कुछ ऐसा कह दें, जो वीरभद्र के सम्मुख कहना उचित न हो।
”कोई और समाचार भी है वीरभद्र !” वसुदेव ने विषय बदल दिया।
”और सब सामान्य ही है। देवी रोहिणी और बलराम भैया सानन्द हैं। एक बात और है …।” वीरभद्र ने कहा, ”सारे व्रज-क्षेत्र में गोपाल लोग अखाड़ों की मिट्टी में श्रम कर अपना स्वेद बहा रहे हैं। लाठी और शूल इत्यादि का उनका अच्छा अभ्यास है। कहीं-कहीं खड्ग-परिचालन का भी प्रशिक्षण चल रहा है। नंद इस संदर्भ में बहुत जागरूक व्यक्ति हैं। अब जिस क्षण हम चाहेंगे, थोड़े से श्रम से उन्हें अच्छी प्रशिक्षित सेना में परिणत कर सकते हैं।”
”क्या इसी कारण से कंस वहां खुला आक्रमण नहीं करना चाहता ?”
”बहुत संभव है कि कुछ ऐसा ही हो।” वीरभद्र बोला, ”वह उन गोपों से खुली शत्रुता मोल लेना नहीं चाहता। नहीं तो उस सारे क्षेत्र में धरती से उगने वाली दूब भी उसकी शत्रु हो जाएगी।”
”अच्छा है कि नंद की ऐसी तैयारी है।” वसुदेव किसी गहरी चिंता में थे, ”देखना है कि संघर्ष के लिए कौन सा क्षण उपयुक्त है।”
”अच्छा! चलता हूं स्वामी !” वीरभद्र ने अपनी पोटली इत्यादि समेट ली।
”ठीक है। इसी प्रकार समाचार देते रहना।…किंतु चलते हुए हम दोनों को आशीर्वाद देना न भूलना।…”
वीरभद्र ने चकित भाव से उनकी ओर देखा।
”वह पूजा अर्थात् वासना गिद्ध-दृष्टि से इधर ही देख रही है।” वे बोले, ”यदि हमने तुम्हें प्रणाम नहीं किया और तुमने आशीर्वाद नहीं दिया, तो उसे संदेह हो जाएगा।”
”जैसी आपकी आज्ञा स्वामी!” वीरभद्र उठ खड़ा हुआ।
*****
संध्या समय देवकी ने वासना को विदा कर दिया।
”जाइए, घर के सारे कपाट बंद कर लीजिए।” वे वसुदेव से बोलीं, ”मुझे आपसे एक बात करनी है।”
वसुदेव ने घर के सारे कपाट भीतर से बंद कर लिए और वे निश्चिंत हो गए कि अब घर में पूर्ण एकांत था।
”बोलो।”
”मुझे अब और नहीं सुनना यह सब।” देवकी सहसा ही उत्तेजित होकर बोलीं, ”अब मैं अपने पुत्रों को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती। कितनी ही तो घटनाएं हो गईं, आज तक। यह तो महाविष्णु की कृपा है कि दोनों लड़के अभी तक सुरक्षित हैं। किंतु अब नंद उनकी रक्षा नहीं कर सकता। रोहिणी भी नहीं कर सकतीं। बेचारी यशोदा तो एक घरेलू महिला है, वह कहां-कहां कृष्ण-बलराम की रक्षा करती फिरेगी।…”
”तो ?” वसुदेव ने पूछा।
”अब मुझे स्वयं गोकुल जाना होगा।”
वसुदेव हंस पड़े, ”तो अब तुम जाकर असुरों से लड़ोगी और अपने पुत्रों की रक्षा करोगी ?”
”कर नहीं सकती ?” देवकी का मुख आवेश में लाल हो आया।
”कर क्यों नहीं सकतीं।” वसुदेव गंभीर हो गए, ”मां अपनी संतान पर संकट देखती है तो वह महिषासुरमर्दनी बन जाती है। पर बात यह नहीं है।”
”तो क्या बात है ?”
”बात यह है कि जिन पुत्रों को हमने इतने गोपनीय ढंग से कंस से बचा कर नंद के पास भेजा, उनको अब तुम गोकुल जाकर मथुरा ले आओगी और घोषित रूप से कंस को बताओगी कि वे तुम्हारे पुत्र हैं; ताकि कंस को उनकी हत्या करने की सुविधा हो जाए।”
”तो इस गोपनीयता के चक्कर में अपने पुत्रों को वहां छोड़ दूं, जहां वे एकदम असुरक्षित हैं। वहां उनके प्राण चले गए तो ?”
”उनके प्राण नहीं जाएंगे।” वसुदेव के स्वर में विश्वास की दृढ़ता थी।
”आप इतने विश्वास से कैसे कह रहे हैं ?”
”ध्यान दो देवकी !” वसुदेव जैसे किसी कल्पना-लोक में जा बैठे थे, ”जब तक शकटासुर, पूतना और तृणावर्त की घटनाएं हो रही थीं, तब तक मैं भी बहुत भयभीत था। मैं मानता था; और आज भी मानता हूं कि वे सब कंस के भेजे हुए भाड़े के हत्यारे थे। शुल्क लेकर हत्या करने वाले। किंतु अब …”
”अब क्या हो गया है ?”
”अब !” वसुदेव बोले, ”कालिय नाग को कंस ने नहीं भेजा। कालिय कृष्ण के पास नहीं गया। कृष्ण ही कालिय के पास गया है। उसे ललकारा है और उसे घायल कर अपना कंदुक लेकर वापस आया है।…”
”तो उससे क्या अंतर पड़ गया।” देवकी उसी प्रकार उत्तेजित थीं, ”जहां आस-पास इस प्रकार हिंस्र राक्षस और पशु हों; और इन बालकों की उचित देखभाल करने वाला, उनको रोक कर रखने वाला कोई न हो, वहां बालक तो असुरक्षित ही हुए न। यहां उन्हें मैं अपने कलेजे से लगा कर रखूंगी।”
”सुनो देवकी !” वसुदेव बोले, ”मेरे मन में एक नई बात आ रही है।”
”क्या ?”
”अपने शत्रु राक्षसों और हिंस्र पशुओं से स्वयं को बचाना कृष्ण के लिए एक अनिवार्यता थी; किंतु कालियदमन उसकी बाध्यता नहीं थी। वह उसने स्वेच्छा से किया है। क्यों संकट मोला उसने ?”
”बालक है। एक कंदुक के लिए अपने प्राणों पर खेल गया …।”
”नहीं !” वसुदेव आह्लादक आवेश में बोले, ”नहीं ! वह अपनी शक्ति प्रकट कर रहा है। वह संकेत दे रहा है कि वह कौन है और क्या करने आया है।”
”क्या कहना चाहते हैं आप ?”
”स्मरण करो उस भविष्यवाणी को।” वसुदेव बोले, ”तुम्हारे आठवें गर्भ की संतान के विषय में कहा गया कि वह कंस का वध करेगी। कृष्ण तुम्हारे आठवें गर्भ की संतान है।…”
देवकी चुपचाप वसुदेव की ओर देखती रहीं।
”वह बता रहा है कि तारणहार आ गया है।”
वसुदेव की आंखें बंद थी। लगता था, जैसे उनकी समाधि लग गई हो। चेहरे पर परमानन्द का भाव था और बंद आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। जाने उनको क्या उपलब्ध हो गया था।
”वह आ गया है।”
”कौन आ गया है ?”
”कंस का काल। संसार का तारणहार। महाविष्णु का अवतार। वह संसार को बता रहा है कि वह आ गया है। वह अपने आने की घोषणा कर रहा है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कंस जान भी जाए कि कृष्ण मेरा पुत्र है, तो भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कहता था न कि मुझे उस भविष्यवाणी पर विश्वास होता जा रहा है; क्योंकि कंस मेरे सातवें पुत्र को नहीं मार पाया। आठवें की रक्षा के लिए स्वयं भगवती योगमाया वर्षा के रूप में आ गईं। यमुना मैया मेरी रक्षा के लिए कवच बन गईं; और मेरी नौका बन कर मुझे तैरा कर नंद के घर पहुंचा कर सुरक्षित वापस ले आईं। अब तो मैं पूर्ण निष्ठा से कह सकता हूं कि कृष्ण जान- बूझ कर वे लीलाएं कर रहा है कि संसार जान सके कि वह कौन है। जो पहचान सकता है, पहचान ले कि वह कौन है। जो अंधा है, जो उसे पहचानता नहीं, पहचानना चाहता नहीं, या पहचान सकता नहीं, वह मूर्ख है। अविश्वासी और अविवेकी लोग उसे नहीं पहचानते, न पहचानें। पर वह बता रहा है कि वह आ गया है।”
डॉ. संध्या सिलावट, मध्य प्रदेश

श्रीकृष्ण और उनकी व्यापकता
हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत से देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। देवों के देव महादेव, पूर्ण अवतार श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा के साथ-साथ अन्य देवताओं की पूजा भी लोकप्रिय है। जब भी किसी को आदर्श की कोई बात समझानी होती है तो है तो हिंदू धर्मावलंबी सबसे पहले मर्यादा पुरुषोतम राम का उदाहरण देते हैं। विवाहित दंपती को आर्शीवाद देते हैं कि तुम्हारा जोड़ा शिव-पार्वती के समान कई जन्मों तक बना रहे। जब नन्हें-मुन्नों से लडियना होता है तो सभी यह कहते हुए दुलारते हैं कि मेरा छोटा सा कन्हैया, नटखट बाल-गोपाल। जब सखा भाव अथवा प्रेम भाव का उदाहरण देना हो तो झट श्री कृष्ण से उदाहरण दिया जाता है। मित्रता हो तो सुदामा-कृष्ण सी, या प्रेम होतो राधा-कृष्ण सा। भारत के जनमानस में शिव, राम व कृष्ण समाए हुए हैं।
श्रीकृष्ण को विष्णु का आठवॉं पूर्णावतार अवतार माना जाता है। 64 कलाओं में दक्ष श्रीकृष्ण में ईश्वर के सभी पूर्ण गुण विद्यमान थे। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को उन्होंने अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराके यह सिद्ध कर दिया था कि वह ही परमेश्वर हैं।
कृष्ण को महान मानने बनाने वाले अनेक धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक कारण हैं। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था प्रेम, युद्ध, राजनीति, कूटनीति, संगीत, नृत्य और योग सभी में अद्वितीय थे। वह सभी को सम्मान देते थे धन, जाति, वर्ग, लिंग का भेदभाव नहीं किया, सुदामा जैसे निर्धन मित्र से लेकर ग्रामवासी अहीर गोप-गोपियों तक, सबको समान प्रेम दिया। सबसे प्रेम करते थे, पर धर्म रक्षा और अधर्म के विनाश के लिये कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे अत्याचारियों का अंत किया और धर्म की स्थापना की।
उन्होंने सदा अपने रिश्तों को प्रेमपूर्वक निभाने का प्रयास किया, इसके लिए उन्होंने तुच्छ लोगों द्वारा किया गया अपमान भी निरंतर सहन किया। अपनी बुआ के प्रति प्रेम व आदर के कारण उनके पुत्र शिशुपाल द्वारा 100 बार गालियॉं देकर अपमानित करने पर भी क्षमा किया, परंतु 101वीं बार अपमान होने पर सुदर्शन चक्र से मार डाला। समर्थशाली होने पर भी अपनी बुआ के लिए उन्होंने निरंतर अपमान झेला।
कृष्ण एक बलशाली योद्धा हैं, परंतु जीवन का सहज आनंद और सरलता उन्होंने कभी नहीं त्यागी। उन्हें संगीत से भी उतना ही प्रेम है, तभी तो सुदर्शनचक्रधारी होते हुए भी उनके हाथ में बॉंसुरी सदा रहती है। वह संसार को प्रेरणा देते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी सब सहजता से साधा जा सकता है। कोई कितना भी ऊँचा उठ जाए, पर उसे धरातल पर बने रहना चाहिए। उसे पुराने नाते-रिश्तों को नहीं भूलना चाहिए। द्वारिकाधीश होने पर भी वह अपने बालकाल के मित्र निर्धन सुदामा को नहीं भूले।
श्री कृष्ण की पूजा अनेक रूपों में होती है, उनका प्रत्येक रूप अलग ही पहचान एवं महत्व रखता है।
कृष्ण के जिन रूपों की पूजा संसार में सर्वाधिक होती है, वे मुख्यतः श्रीकृष्ण का बाल रूप (लड्डू गोपाल/माखन चोर) और युवावस्था का रूप (मुरलीधर/गोपियों के प्रिय) हैं।
बाल कृष्ण (लड्डू गोपाल/ माखन चोर) -भगवान श्रीकृष्ण का यह रूप चंचल और प्यारे बालक का है, यह रूप वात्सल्य भक्ति का प्रतीक है, जिसमें भक्त भगवान को अपने बालक के रूप में प्रेम करते हैं। भक्त अपने घर में उन्हें शिशु-पुत्रवत पालते हैं, स्नान, ऋतु अनुसार वस्त्र-परिवर्तन, भोग अर्पण और शयन आदि करते हैं। भक्त और ईश्वर का संबंध औपचारिक नहीं, बल्कि स्नेहपूर्ण और सहज होना चाहिए। यशोदा के साथ बाल कृष्ण का संबंध दर्शाता है कि ईश्वर भी भक्त के प्रेम में बंध सकते हैं। यह भक्ति का सबसे निकट और स्नेहमय रूप है।
बाल कृष्ण का रूप बाल सौंदर्य और वात्सल्य प्रेम का प्रतीक है। उनकी मुस्कान, लीलाएँ एवं बांसुरी की धुन भक्त के हृदय में मधुर भाव जगाती हैं। यदि भक्त कवि भी हुआ तो फिर सूरदास के समान नेत्र न होते हुए भी वह ऐसी रचना रचता है कि पद सुनने वालों को को लगता है वे अपने संमुख ही बाल गोपाल को देख रहे हैं। बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण में मिलता है। जिन्हें आधार बनाकर पश्चात्वर्ती कवियों ने अनेक रचनाएं रचीं और अमर हो गए। बाल्यकाल में विषम परिस्थितियों में जन्म लेकर भी कृष्ण सदा ही आगे बढ़ते रहे। बाल्यकाल में ही उन्हें मारने आए अनेकों राक्षसों पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर और अघासुर आदि का वध किया। जिन्हें उनके मामा कंस ने उनकी हत्या करने भेजा था। लेकिन फिर भी वह यशोदा द्वारा रस्सी से बाँधने पर उसमें बँध जाते हैं जो इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर भी भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। कृष्ण प्रेम और जीवन के रस का अद्वितीय संगम हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण का जन्म हुआ था, इस दिन को जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों व घरों में कृष्ण से संबंधित झॉंकियॉं सजाई जाती हैं व सुंदर झूलों में लड्डू गोपाल को झुलाया जाता है और भोग अर्पित किया जाता है।
गोपाल कृष्ण-बाल्यकाल में श्रीकृष्ण गाय चराने जाते थे, अतएव उन्हें ‘गोपाल’ भी कहते हैं। बड़े भाई दाऊ के संग खेलते कृष्ण, अन्य ग्वाल-बालों के साथ शरारत, गाय चराना, यमुना नदी किनारे खेलना, माखन चुराना और ग्वालिनों को तंग करना ये सभी रूप सहजता और लोकजीवन के आनंद का प्रतीक हैं। प्रकट होता है कि ईश्वर केवल राजमहलों में नहीं सामान्य जीवन में भी विद्यमान हैं। वह जीवन में आनंद और सरलता का संदेश देते हैं। यमुना नदी का कालिया नाग अत्यंत भयानक था, परंतु गोपाल कृष्ण भयभीत हुए बिना उसके फन पर नृत्य करते हैं और उसका दमन कर देते हैं, स्पष्ट संदेश देते हैं कि जीवन की कठिनाइयों को भी खेल-खेल में समाप्त किया जा सकता है।
युवराज/मुरलीधर कृष्ण – प्रेम और भक्ति के परम आदर्श माने जाते हैं। ग्वाले को गोप और ग्वालिन को गोपी कहा जाता है। बांसुरी वादन से गोपियों को मोह लेते हैं, गोपियॉं आकर्षित होती हैं। उनसे प्रेम करती हैं। कृष्ण को परमात्मा का साकार रूप माना जाता है, जो भक्त से प्रेम करने के लिए स्वयं मानव रूप में आते हैं। यह माधुर्य भक्ति का सर्वोत्तम आदर्श है, जिसमें आत्मा (गोपियाँ) परमात्मा (कृष्ण) से मिलन की आकांक्षा रखती है।
जब भक्ति में प्रेमी-प्रेमिका जैसा भाव आ जाता है, भक्त के लिए ईश्वर ही जीवन का केंद्र बन जाता है। कृष्ण भक्ति में तल्लीन गोपियॉं घर-परिवार त्याग कृष्ण से मिलने के लिए चल देती हैं। यह भक्त का ईश्वर के प्रति सम्पूर्ण समर्पण का आदर्श है। कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं। रासलीला जीव और ब्रह्म के मिलन का आध्यात्मिक रास है, भोग-विलास नहीं, यह भक्ति को आनंद और सौंदर्य से जोड़ता है। पुराणों में गोपी-कृष्ण लीला का वर्णन है। इसमें गोप और गोपिकाएं रासलीला करते हैं। बरसाना, वृंदावन और मथुरा में यह रूप अत्यधिक पूज्य व लोकप्रिय है। लोकगीतों, नृत्यों और चित्रकलाओं में इस रूप का व्यापक चित्रण मिलता है।
रक्षक कृष्ण का यह रूप ‘परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्…’अर्थात् धर्म के लिए कभी-कभी हिंसा भी आवश्यक है, का प्रतीक है। धर्म के संस्थापक और अधर्म के विनाशक के रूप में वह अत्याचारियों का विनाश करते हैं, जिससे धर्म की स्थापना हो व समाज में न्याय और संतुलन बनाए रखा जा सके। इंद्र के प्रकोप के चलते जब वृंदावन आदि ब्रज क्षेत्र में जलप्रलय हुई थी, तब गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाकर सभी ग्रामवासियों की रक्षा की। किशोरावस्था में ही चाणूर, मुष्टिक और कंस जैसे बलशाली लोगों का वध किया। रक्षक कृष्ण यह सिद्ध करते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए साहस और कूटनीति दोनों अति आवश्यक है। जरासंध, नरकासुर, शिशुपाल जैसे अत्याचारियों का अंत करते हैं। नरकासुर की मृत्यु से 16,000 स्त्रियों की मुक्ति हुई जिनसे कृष्ण ने विवाह कर उनके साथ न्याय और करुणा का अद्वितीय संदेश दिया। लोकनाट्यों में उनके पराक्रम की कथाएँ मंचित की जाती हैं।
महाभारत के युद्ध के समय जब अपने प्रियजनों को देख अर्जुन अपने कर्त्तव्य पथ से विचलित होने लगे, तब अर्जुन के सारथी बने कृष्ण ने उन्हें योगेश्वर कृष्ण के रूप में गीता का उपदेश दिया। ज्ञान, कर्तव्य और धर्म-पालन के पथ पर आरूढ़ करने वाला सर्वोच्च संदेश दिया कि
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।
अर्थात् तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, कर्मफल पर नहीं, इसलिए कोई भी कर्म फल के लिए नहीं किया जाना चाहिये। अतः तुम कर्मफल का ध्यान ना रखो और अकर्मण्यता में आसक्त मत बनो।
गीता में अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत सभी दर्शनों का संगम मिलता है। श्री कृष्ण के विचार कालातीत और सार्वभौमिक हैं। गीता का आज भी उतना ही महत्व है, यह नेतृत्व, युद्धनीति, और नैतिक शिक्षा में पढ़ाई जाती है।
महात्मा गांधी ने गीता को अपनी ‘आध्यात्मिक डिक्शनरी’ कहते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन भी गीता का महत्व स्वीकार करते थे। श्रीमद्भगवद्गीता में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग का समन्वित संदेश है। कृष्ण का व्यक्तित्व केवल पौराणिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, वह पूरे विश्व को जीवन-ज्ञान प्रदाता, प्रेम सीखाने वाले, करुणा और न्याय प्रदान करने वाले के रूप में सामने आते हैं। उनके उपदेशों और लीलाओं से विभिन्न संस्कृति, भाषा और स्थानों के लोग प्रभावित हो जाते हैं। बालक के रूप में माखनचोर हैं तथा गीता का उपदेश देने वाले महान योगेश्वर भी। श्रीकृष्ण को महायोगी माना जाता है। उनमें कई तरह की यौगिक शक्तियां थीं। योग के बल पर ही वह मृत्युपर्यंत युवा रहे।
गीता में कर्मयोग का बहुत महत्व है। कर्मयोगी कृष्ण यह सिद्ध करते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए साहस और कूटनीति दोनों अति आवश्यक है। कृष्ण ने जो भी कार्य किए, उसे अपना कर्म माना, अपने कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यकता होने पर साम-दाम-दंड-भेद आदि सभी का प्रयोग किया, वर्तमान में कर्म करते हुए जीना ही उनका उद्देश्य रहा, जिससे अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। कूटनीति से कर्ण के कवच और कुंडल दान में दिलवा दिए, वहीं उन्होंने दुर्योधन के संपूर्ण शरीर को वज्र के समान होने से रुकवा दिया, जिससे पॉंडव विजयी हो सकें। वह धर्म की स्थापना कर सकें। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि जब-जब धर्म की हानि होगी, तब-तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा।
श्रीकृष्ण के गुरु सांदीपनी थे। जिनका आश्रम अवंतिका (उज्जैन) में था। कृष्ण ने उनके प्रति भी आदर्श शिष्य का दायित्व निभाया था, वह उनके मृत पुत्र को यमराज से मुक्त कराकर लाए और गुरु को गुरु दीक्षा में भेंट किया।
श्रीकृष्ण महान योद्धा थे। उन्होंने अपने समय के बड़े-बड़े शूरवीरों को पराजित किया था। जैसे जरासंध, कालयवन पौंड्रक और जाम्बवंत आदि से भयंकर युद्ध किया था। उनके पास शक्तिशाली सेना थी। जिसे दुर्योधन ने उनसे मॉंग लिया था। परंतु उन्होंने सर्वसमर्थ होने पर भी महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाया, अर्जुन के सारथी बने। जो एक योद्धा के लिये कमतर ऑंका जाता है। परंतु उनकी यह विनम्रता है।
उन्हें तो ‘रणछोड़ कृष्ण’ भी कहा जाता है क्योंकि वह जरासंध से शत्रुता के कारण उनके बंधु-बांधवों की रक्षा हेतु मथुरा छोड़कर द्वारिका जाकर बस गए। व्यर्थ में युद्ध करने की बजाए जितना हो सके उससे बचने का पथ भी कृष्ण ने दिखाया।
श्रीकृष्ण संबंधों को निभाने में विश्वास रखते थे। यथा संभव उन्होंने प्रत्येक संबंध को निभाने का प्रयास किया। उनकी 8 पत्नियां रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी थीं। जिनसे श्रीकृष्ण को 80 पुत्र थे। सुभद्रा उनकी बहन थी, जिसका विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से करवाया था और द्रौपदी उनकी मानस बहन थी। श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ था। द्रौपदी की रक्षा उन्होंने चीरहरण के समय की थी।
कृष्ण का एक महत्वपूर्ण रूप सखा के रूप में भी है। द्रौपदी भी श्रीकृष्ण की सखी थीं। नर और नारी दोनों ही उनके सखा और सखियॉं थें। उनके मुख्य सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोककृष्ण, वरूथप, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरन्द, सदानन्द, चन्द्रहास, बकुल, शारद, बुद्धिप्रकाश तथा अर्जुन आदि थे। राधा, ललिता, चन्द्रावली, श्यामा, तुंगविद्या, इन्दुलेखा और रंगदेवी आदि उनकी मुख्य सखियॉं थीं।
लोक साहित्य में बालकृष्ण के नंदगाँव के गोपियों को चिढ़ाने वाले नटखट बालक, माखनचोर तथा बांसुरी बजाने वाले बालक जिनकी लीलाओं में भोलेपन और शरारत का सम्मिश्रण होता है जैसे कई रूपों का वर्णन मिलता है।
युवक प्रेमी के रूप में राधा और गोपियों के साथ रास-लीला तथा माधुर्य भाव, विरह और मिलन (राधा का कृष्ण-वियोग-संयोग भावनात्मक गहराई के साथ) के गीतों के केंद्र कृष्ण हैं। लोकगीतों में कृष्ण नायक के रूप में हैं। ‘ब्रज के रसिया’ राधा-कृष्ण के प्रेम और होली की छेड़छाड़ के गीत हैं। ‘फाग गीत’ में होली के अवसर पर कृष्ण की रंग-लीलाएँ गाई जाती हैं। ‘सावन-भादो के झूला गीत’ जिनमें वर्षा ऋतु में कृष्ण राधा को झूला झुलाते हैं। बालकृष्ण के जन्म पर सोहर, मंगला, जन्मोत्सव गीत गाए जाते हैं, जो किसी सामान्य शिशु के जन्म के अवसर पर भी गाए जाते हैं।
लोककथाओं में गोकुल और नंदगाँव की गलियों में कृष्ण केवल देवता नहीं, बल्कि गाँव के ‘अपना लड़के’ जैसे हैं-कहीं वे चोरी किए हुए माखन को सखाओं में बाँट रहे हैं। कहीं गोपियों के घड़े फोड़ रहे हैं। कालिया मर्दन, गोवर्धन धारण, पूतना वध जैसी कथाओं के माध्यम से कृष्ण के संरक्षक और उद्धारक रूप का वर्णन मिलता है। इन लोक कथाओं में कृष्ण का ग्रामीण और कृषक समाज के लिए न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमान ग्रामीण लोकनायक के रूप में चित्रण मिलता है। जहॉं वह गरीब, असहाय और सताए हुए लोगों की सहायता करने वाले चतुर नायक हैं। किसी लोककथा में गोपियों के साथ हास्यपूर्ण संवाद और हंसी-मजाक का वर्णन भी है। कई बार चमत्कारिक शक्तियों के साथ ही मानव-जैसे व्यवहार से जुड़ा चित्रण भी मिलता है।
लोक नाट्यों और प्रदर्शन कलाओं में जैसे रासलीला में विशेषतः ब्रज में राधा-कृष्ण के प्रेम और भक्ति का मंचन किया जाता है। ‘कृष्णलीला’ में बचपन से लेकर महाभारत तक के प्रसंगों पर आधारित नाट्यरूपों का मंचन किया जाता है। यक्षगान (कर्नाटक), कथकली (केरल), नौटंकी (उत्तर भारत) एवं क्षेत्रीय रंगमंच शैलियों में कृष्ण की कथाएँ ही विषय होती हैं।
लोकसाहित्य में कृष्ण का भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व है। राधा-कृष्ण प्रेम और माधुर्य के प्रतीक हैं। उनका प्रेम सांसारिक सीमाओं से परे तथा आदर्श माना जाता है। इनका कीर्तन-श्रवण तथा सत्संग सामूहिक सहभागिता को बढ़ाते हैं, जो सामाजिक एकता का माध्यम बनते हैं। लोकजीवन में कृष्ण भक्ति नैतिक मूल्यों का संचार करती है। कृष्ण-कथाएँ और गीत पीढ़ियों से मौखिक परंपरा में चलायमान है, जिसमें कृष्ण केवल ईश्वर नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं प्रेम, मित्रता, साहस, चतुराई के प्रतीक हैं। कृष्ण का लोक साहित्य में स्थान अमिट और सर्वव्यापी है।
भक्ति आंदोलन ने कृष्ण को भक्ति और कविता दोनों का केंद्र बना दिया था। वल्लभाचार्य के अष्टछाप के आठों कवि सूरदास, कुंभनदास व नंददास आदि, रसखान (मुसलमान होते हुए भी), मीराबाई कृष्ण-प्रेम में लीन हो अमर हो गए।
पूरे विश्व में श्रीकृष्ण के भक्त हैं। भारत और विश्व में श्रीकृष्ण के काफी मंदिर हैं। इन समूहों में से एक समूह इस्कॉन (ISKCON) मंदिर भी है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्ण के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उद्देश्य कृष्ण के जीवन दर्शन को और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना है। यूरोप में इस्कॉन के लगभग 135 मंदिर हैं। स्पेन, इटली, बेल्जियम और फ्रांस जैसे स्थानों पर कृष्ण के अनुयायी हैं। रूस में भी इस्कॉन के लगभग 30 केंद्र हैं। नॉर्थ अमेरिका में ISKCON के लगभग 56 मंदिर हैं। साउथ अमेरिका में भी इस्कॉन के 60 मंदिर हैं। कनाडा में भी इस्कॉन के 12 केंद्र हैं। भारत से इतर एशिया में इस्कॉन के लगभग 80 केंद्र हैं। इनमें से अधिकतर सेंटर्स इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों में हैं। अफ्रीका में लगभग 69 केंद्र (सेंटर्स) हैं। डरबन का सेंटर महत्वपूर्ण माना जाता है। डरबन में विदेशों में होने वाली सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है। ऑस्ट्रेलिया में इस्कॉन के लगभग 6 मंदिर हैं, वहीं न्यूजीलैंड में 4 सेंटर्स हैं। इस प्रकार हमें कृष्ण की विश्वव्यापी भक्ति का परिचय मिलता है।
श्री कृष्ण के भारत में भी बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय मंदिर हैं, जहॉं जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा (उत्तर प्रदेश) में है। मान्यता है कि कंस की जेल में इसी स्थान पर श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था।
मथुरा में भी द्वारिकाधीश मंदिर है जिसका ग्वालियर रियासत के खजांची सेठ गोकुल दास पारीख ने 1814 में निर्माण करवाया था। कृष्ण को प्रायः ‘द्वारका के राजा’ या ‘द्वारकाधीश’ भी कहा जाता है। इसी नाम पर मंदिर का नाम रखा गया।
महाभारत में वर्णन है कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। द्वारका (गुजरात) में स्थित द्वारकाधीश मंदिर लगभग दो हजार वर्ष पुराना है। यह मंदिर चार धामों में से एक है।
श्री कृष्ण का बाल्यकाल वृन्दावन (उत्तर प्रदेश) में बीता। श्रीकृष्ण बांकेबिहारी भी कहलाते हैं। स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी मंदिर बनवाया था। इसे वृन्दावन का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कहा जाता है।
प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित है। जगद्गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मन्दिर के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। यह वृंदावन के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है।
उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर 800 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। यहॉं प्रति वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। इस धाम में श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं।
अहमदाबाद (गुजरात) के जगन्नाथ मंदिर में भी भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं।
उडुपी शहर (कर्नाटक) में स्थित श्रीकृष्ण मठ मंदिर 13वीं सदी में संत माधवाचार्य द्वारा निर्मित किया गया था। मंदिर के पास स्थित तालाब के पानी में मंदिर का प्रतिबिंब दिखाई देता है।
चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में स्थित इस मंदिर के गिरिधर गोपाल को व्यापारी अपने व्यापार में पार्टनर बनाने के लिए आते हैं, गिरिधर गोपाल को सेठ जी के नाम से बुलाते हैं और उन्हें सांवलिया सेठ कहते हैं।
गुरुवायुर शहर (केरल) में श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। यह मंदिर 5000 साल पुराना है, इसे भूलोक के बैकुंठ के नाम से भी पुकारा जाता है।
नाथद्वारा (राजस्थान) का मंदिर 12वीं शताब्दी में बना था।
बेंगलुरू (कर्नाटक) में स्थित इस्कॉन मंदिर पूरे विश्व में स्थित इस्कॉन मंदिरों में सबसे बड़ा है। बहुत सुंदर मंदिर है।
हर युग में लोग श्रीकृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहे हैं। श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व जीवन के हर मोड़ व अवस्था में व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है, बस इसे समझने की आवश्यकता होती है। कृष्ण केवल पूजा के देवता नहीं, वह प्रत्येक भक्त के मित्र, पुत्र, प्रेमी, सारथी और मार्गदर्शक के रूप में मानव के हृदय के निकट हैं। उनसे अपनी पीड़ा साझा कर भक्त निश्चिंत हो जाता है। यदि व्यक्ति उचित समय पर समझ जाए तो नाना प्रकार की परेशानियों जैसे निराशा और विषाद से स्वयं को सुरक्षित रख सकता है।
डॉ शिप्रा शिल्पी सक्सेना, जर्मनी

जर्मनी में गुंजायमान : जय कन्हैया लाल की
जन्माष्टमी मात्र एक धार्मिक उत्सव के रूप में ही नहीं वरन अधिकांशतः एक आत्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसका मुख्य कारण है कान्हा से आत्मिक प्रेम। “कान्हा” देव रूप से कहीं अधिक अपने बाल रूप में हमारे हृदय में वास करते है। बाल सखा कान्हा हो या माखन चोर कन्हाई हर रूप में मोहते है जैसे अपने ही बालक हो। इस बात को वो लोग अधिक गहराई से समझ सकते जिनके घरों में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, उनके बाल रूप की सेवा की जाती है।
प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मात्र भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी धूम धाम से मनाया जाता है। हमारा परिवार लड्डू गोपाल का उपासक है, ऐसे में जन्माष्टमी का पर्व बहुत उत्साह, विधि विधान एवं ललक के साथ मनाया जाता है। रात्रि में व्रत से शुरू हुआ पर्व, सुबह सुबह घर को पंजीरी की भीनी भीनी खुशबू से भर देता है। लड्डुओं की लालच में रसोईघर के आस पास गोल गोल मंडराती घरवालों की आँखें, पंच मेवों से बनी कत्लियों के थाल, गोंद और सोंठ की बर्फी, पंचामृत, तरह तरह के पकवान, तुलसी की पावनता( जिसे यहां बेसिल कहते है), फूलों के बंदनवार से सजे मंदिर के द्वार, चावल हल्दी के आटे की चौक, भजन एवं सोहर के मधुर स्वर कान्हा के स्वागत में मन को आनंद से सराबोर कर देते है।
यूं तो घर पर हम ये त्यौहार पूरे रीति रिवाज के साथ मनाते है, किंतु ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि जर्मनी में अनेक स्थानों पर जन्माष्टमी पूरी श्रद्धा से मनाई जाती है। विशेषकर इस्कॉन मंदिर में।
कोलोन ! जिस शहर में मै रहती हूं वहां जन्माष्टमी से पूर्व शहर के मुख्य बाजार Neumarkt में आपको विदेशी युवक युवतियां भारतीय परिधान में, माथे पर चंदन का टीका लगाए, ढोल , झांझ , मंजीरा बजाते हुए हरे रामा हरे कृष्णा गाते बजाते दिखने लगेगे। इन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे आप मथुरा वृंदावन में आ गए हों। सारा वातावरण उस क्षण कृष्णमय हो जाता है। इस्कॉन के साथ ही सार्वजनिक रूप से जन्माष्टमी अनेक व्यक्तिगत सांस्कृतिक स्थाओं एवं मंदिरों में भी मनाई जाती है।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जर्मनी के कई शहरों में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। जिसमें फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, हैम्बर्ग, बर्लिन, कोलोन, हागर, एसेन के ISKCON मंदिरो में, हरिओम मंदिर, कोलोन में एवं जगन्नाथ मठ बर्लिन में विशेष पूजा, भक्तिगीत, प्रसाद एवं अभिषेक के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
Abentheuer (Goloka-Dhama) इस्कॉन का ऐतिहासिक केंद्र, जन्माष्टमी के अवसर पर यहां दार्शनिक संगोष्ठी, सुमधुर कीर्तन, कथा तथा भक्तजनो मिलन का आयोजन किया जाता है। Heidenrod (Bhakti Marga) को मानने वाले इसके अनुयायी भजन, कीर्तन, रात्रि जागरण एवं विशेष प्रसाद के साथ आध्यात्मिक स्तर पर उत्सव का संयोजन करते है।
आपको जानकर अच्छा लगेगा इन मंदिरों में भी भारत की ही तरह रात्रि के 12 बजे पारंपरिक पूजाविधि का निर्वाह करते हुए खीरे से प्रभु का जन्म करवाया जाता हैं। शुभ-मुहूर्त पर दूध, दही, गंगाजल, शहद एवं जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाता है। कान्हा को नए वस्त्र पहनाकर, तिलक लगाकर, मोरमुकुट से सजाकर, भोग प्रसाद लगाया जाता है और फिर वही प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। घरों एवं मंदिरों में श्रीकृष्ण-जन्म की कथा से जुड़ी झाकियों का भी प्रदर्शन भी किया जाता है साथ ही कान्हा की बाल लीलाओं को बच्चों से साझा भी किया जाता है।
बच्चों, युवाओं और कलाकारों द्वारा कृष्ण लीला, प्रहसन व विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। जिसमें शास्त्रीय-लोक नृत्य, गीत, नाटक आदि शामिल हैं।
यूं तो सार्वजनिक रूप से दही हांडी रस्म को करना जर्मनी में स्वीकृत नहीं है किंतु कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करते हुए प्रतीकात्मक रूप से ‘दही हांडी’ का आयोजन किया जाता है।
भारतीय समुदाय स्थानीय जर्मन मित्रों के साथ मंदिरों, कम्युनिटी सेंटर्स या सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होकर पर्व को मिलजुलकर मनाते हैं। इस्कॉन (कोलोन) द्वारा गीता का पाठ हो या घर पर मिलजुल कर भजन कीर्तन करते हम भारतीय परिवार उद्देश्य सिर्फ एक, कान्हा के प्रति प्रेम, भक्ति एवं श्रद्धा भाव को समर्पित करना है।
यद्यपि भारत में जन्माष्टमी के अवसर पर जो रौनक होती है, वो रौनक यहां है देखने को नहीं मिलती। किंतु जर्मनी में जन्माष्टमी, शुद्ध आध्यात्मिक श्रद्धा, सांस्कृतिक एकता और सामुदायिक स्नेह का अद्भुत संगम है। भारतीय परंपराओं की जीवंतता जर्मनी के मंदिरों, समुदाय केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर गूँजती है – जहाँ भारतीयों के साथ स्थानीय निवासी भी इस पर्व में भाग लेते हैं और भारतीय संस्कृति के विविध रंगों को अनुभव करते है और झूम कर बोलते है “हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की।”
डॉ॰ जयशंकर यादव, कर्नाटक

कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम
भगवान के अवतारों में ‘कृष्णावतार’ जगजाहिर है। भगवान कृष्ण के श्रीमुख से नि:सृत परम रहस्यमयी दिव्य वाणी ‘श्रीमदभगवद्गीता’ है। यह एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसमें अर्जुन को निमित्त बनाकर, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया गया है जिसका आज तक पार नहीं पाया जा सका है और संभाव्य भी नहीं है। ‘श्रीमदभगवद्गीता’ का विश्व साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इसके पठन -पाठन और चिंतन -मनन से विचित्र और नए भाव स्फुरित होते रहते हैं जिससे मन बुद्धि चकित होकर तृप्त होते हैं। हर बार कुछ नया अनुभव और आध्यात्मिक लाभ होता है। इसको पहले श्लोक से लेकर आखिरी श्लोक तक और फिर उल्टा आखिरी श्लोक से शुरू करके पहले श्लोक तक पढ़ने से अद्भुत शांति मिलती है।
भगवान ने जीवों को स्वतन्त्रता प्रदान की है किन्तु हमें भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। अतएव ‘श्रीमदभगवद्गीता’ का प्राकट्य हुआ। जीव का मनुष्य रूप में जन्म अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। श्रीगीताजी का विशेष लक्ष्य यह है कि मनुष्य भले ही किसी वाद, मत या संप्रदाय को मानने वाला हो किन्तु हर परिस्थिति में उसका कल्याण हो। जीव में जड़ प्रकृति का अंश है और चेतन परमात्म तत्व है। साधक का चित्त से उपराम होने पर जड़ता से विच्छेद हो जाता है और वह परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हमें सुख आने पर सुखभोग की इच्छा का त्याग और दूसरों की सेवा करना चाहिए तथा दुख आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना श्रेयस्कर होगा। सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि रहने से मनुष्य अपने ‘स्वरूप’ की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाता। अतएव हमें अपने से भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए।
भगवान की प्राप्ति के लिए ‘करण सापेक्ष शैली ’ और ‘करण निरपेक्ष शैली’ में साधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ‘करण निरपेक्ष शैली’ में जल्द परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीतोक्त “कर्मयोग’ ‘ज्ञानयोग’ और ‘भक्तियोग’ तीनों ही ‘करण निरपेक्ष’ अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। जीव का ‘कर्मयोग’ से स्वयं की जड़ता का त्याग होता है। ‘ज्ञानयोग’ से स्वयं ही स्वयं को जानता है और ‘भक्तियोग’ में स्वयं ही भगवान की शरण में होता है। ये तीनों ही स्वतंत्रतापूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाले हैं। आइये, हम हर्षोल्लास और पूरे मनोयोग से ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ मनाएँ और कोई भी मार्ग अपनाकर परमात्म तत्व की प्राप्ति करें।
वसुदेव सुतम देवम, कंसचाणूर मर्दनम ।
देवकी परमानंदम, कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम ॥
श्रीमती सुमन माहेश्वरी, फरीदाबाद

श्री कृष्ण की महिमा
भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जगह-जगह श्री कृष्ण की विविध लीलाओं की सुंदर झांकियां सजाई जाती है जिसे बड़े मनोभाव से बड़े व छोटे सभी देखने आते हैं। श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी कहे जाते हैं। उनके बाल रूप की ही नहीं बल्कि हर अवस्था की छवि में एक चुंबकीय आकर्षण है, जैसे पूर्णिमा के दिन चांद अपने पूर्ण स्वरूप में रहता है, भरपूर चांदनी से धरती को सराबोर कर देता है, इसी तरह श्री कृष्ण भी 16 कलाओं से युक्त पूर्ण पवित्र दिव्य व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके मुकुट में सजा मोर पंख, होठों पर फैली मुस्कान, मधुर तान छेड़ती बांसुरी,स्वतः ही हर एक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हम जब श्री कृष्ण की झांकियां देखने जाते हैं तो उनके गुण अलग-अलग झांकी में दर्शाए जाते हैं। आज जरूरत है उन झांकियां को देखकर अपने मन दर्पण में झांकने की और उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करने की।
गीता में भगवान कहते हैं शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। साथ ही यह भी कहा जाता है जैसे कर्म करेगा इंसान, वैसा फल देगा भगवान। तो अच्छे कर्म करते रहें। श्री कृष्ण जो सकारात्मकता के प्रतीक हैं, हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की आस ना करो, फल के मोह में मत फंसो क्योंकि अनंत इच्छाएं ही दुख का कारण है।अपना जीवन जागरूक होकर चलाएं, आज में जीएं ,आज को बेहतर बनाएं। धैर्यता का गुण धारण करें और क्रोध अहंकार पर काबू पाएं, क्योंकि अहंकार या अभिमान ही विनाश का कारण है। सरल रहे, सहज रहें, सच्चाई का साथ रहे, प्रभु की भक्ति निश्चल, निष्कपट भाव से करें। प्यार व निस्वार्थ भाव से मित्रता का रिश्ता निभाएं। विपत्ति के समय आपसी मन मुटाव त्याग कर अपनों का साथ दें।
गिरधर गोपाल ने एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव की रक्षा की यानी सहयोग की एक उंगली अगर सब बढ़ाएं तो बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना आसानी से कर सकते हैं। मोर मुकुट धारी कृष्ण के मोर पंख यही सिखाते हैं कि हलके रहकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, उन्हें बोझ ना समझे। जीवन में सदा उत्साह उमंग बनाए रखें। गंभीरता और रमणीकता से जीवन की यात्रा को सुखद बनाएं। बांसुरी तो श्री कृष्ण के होठों पर सदा लगी रहती थी और उसकी मीठी धुन सुन सब चले आते थे यानी विषम परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखें,वाणी में मधुरता और मिठास रहे तो कृष्ण की दीवानी गोपियों की तरह सब आपके करीब आना चाहेंगे।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सही मायने में मनाना है तो अपना आत्म विश्लेषण करें कि हमने श्री कृष्ण के कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। जीवन में कठिन परिस्थिति या परेशानी सांप की तरह फन फैला कर आएंगी लेकिन उन परिस्थितियों का हंसते हंसते सामना करना ही सिखलाते हैं श्री कृष्ण। आपके मन, वचन, कर्म में पवित्रता व दिव्यता होगी तो स्वतः ही आकर्षण होगा जो आपके व्यवहार व चलन से स्पष्ट झलकेगा। तो झांकिए मन दर्पण में और बन जाइए वही जो आप चाहते हैं। सदा खुशी और उमंग से जीवन को खुशहाल बनाइए। इसी लिए पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सबको इंतजार रहता है। सच्ची जन्माष्टमी तब होगी जब हम श्री कृष्ण के किसी न किसी गुण को अपने जीवन में धारण कर सफल बनाएंगे।
डॉ महादेव एस कोलूर, कर्नाटक

बंशी
महात्माओं ने श्रीकृष्ण मुरली और गोपियों के प्रसंग को ईश्वर, माया और जीव के रुपक में घटाया है। इस रुपक में मुरली को माया बतलाया है। यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है, यही सब माया है। उस माया ने जीवमात्र को अपने वश में करलिया है। जहाँ तक हमारी इंद्रिया पहुँच सकती है वहाँ तक माया का ही साम्राज्य है । माया दो प्रकार की होती है विद्या और अविद्या। अविद्या माया वह माया है जो आत्मा और परमात्मा में जीव और ब्रह्म में विभेद कराती है, जिसके कारण जीव भााव के फंदे में फंसकर नाना तरह के दुःख झेलता है, दुसरी विद्या माया है जो सब तरह से अविद्या माया के प्रतिकूल है जिसके कारण जीवन अन्य सब जीवों को ब्रह्मवत ही जानता है।
श्रीकृष्ण की मुरली यही विद्यामाया है जो जीव को ब्रह्म से मिलाती है। गोपियाँ सब जीव हैं। मुरली (विद्यामाया) गोपियों (जीवों) का श्रीकृष्ण (परब्रह्म) से संयोग कराती थीं । कृष्ण अपने त्रिभंगी रुप से कदम्ब के पेड के नीचे स्थित होकर बंशी के सुर पर सुर क्या निकालते थे मानों वे श्रोताओं के हृदयों को खोजते थे । गोप गोपियाँ बंशीधर को खोजती थीं, पर श्रीकृष्ण भी उनको खोजते थे। जीव परब्रह्म को खोजता है यह सत्य है, किन्तु ब्रह्म भी जीव को खोजता है। कृष्ण की बंशी (माया) मानव हृदयों की खोज मे रहती थी, संगीतज्ञ कृष्ण मानव हृदय के अन्तस्तल में प्रवेश पाना चाहतें थे। अतः हम देखते है कि जब जब बंशीधर बृन्दावन मे प्रविष्ट हो जाता है तो जीव अपना अस्तित्व ही भूल जाता है। ज्यों- ज्यों परमात्मा हमारे हृदय में प्रविष्ट होता जाता है हमारा हृदय उसके स्वागत के लिए स्थान रिक्त करता जाता है। मुरली मे वह मोहिनी शक्ति है जो हमारे मन में प्रेम को जागृत कर देती है और स्थापित करती है हमारे हृदय में आत्मविसर्जन का भाव । यही वह प्रेम है जिसको श्रीकृष्ण (परब्रह्म) अपनी मुरली (माया) के द्वारा गोप व गोपियों (जीवों) के हृदय में खोजते थे।
परमात्मा हमारे हृदय को खोजता है। जो बच्चे की भाँति सरल स्वभाव से परमात्मा को अपने अंतस्तल में अवकाश दें तो, वही वास्तविक मुक्ति का अधिकारी है। यही सूर का जादू है ।
कात्यायनी डॉ पूर्णिमा शर्मा, दिल्ली

कृष्ण कथा
थी रात घनी कारी अँधियारी,
मेघ झूम कर बरस रहे थे ।
जल थल और आकाश मिलाने
हेतु, ज़ोर से गरज रहे थे ||
यमुना भी थी चढ़ी हुई काँधे
तक, मेघों का गर्जन था ।
हरेक भवन में व्याकुलता के
दानव का ही बस नर्तन था ||
कारागृह के दरवाज़े पर
कुछ प्रहरी पहरा देते थे ।
भीतर प्रसव वेदना से व्याकुल
नारी के स्वर उठते थे ।।
तभी ज़ोर की बिजली कड़की,
नेत्र सभी के बन्द हो गए ।
मूर्च्छित होकर सारे प्रहरी
धरती पर अवलुंठित हो गए ||
प्रणव समक्ष खड़े थे, देखा
देवसुता और वासुदेव ने ।
मनमोहक मुस्कान लिए वे
“जागो माँ” ये पुकार रहे थे ||
तभी मधुर शिशु क्रन्दन ने
कानों में अमृत घोल दिया था ।
श्यामवर्ण मोहक बालक ने
मात पिता को मुग्ध किया था ||
खुलीं सकल बेड़ियाँ पिता की,
सारे प्रहरी सोए पड़े थे ।
रखा सूप में शिशु को, पत्नी
से आज्ञा ले निकल पड़े थे ||
चरण पखारे हरि के यमुना,
शान्त भाव से नीचे आतीं ।
सारी जल की निधियाँ, दर्शन
के हित हरि के, दौड़ी आतीं ||
निकट लिटा जसुदा के कान्हा
को, कन्या को गोद उठाया ।
कारागृह में पहुँच, योगमाया
ने क्रन्दन तीव्र मचाया ||
जागे प्रहरी सभी तो देखा,
कोमल शिशु धरती पर पाया ।
तुरत संदेसा सुनकर मामा
निज भवनों से भागा आया ||
रोका बहुत देवकी और वसुदेव
ने, लेकिन कंस न माना ।
दिया धरा पर पटक बालिका
को, एक पल भी शोक न माना ||
“तेरा मोक्ष कराने के हित
जन्म हो चुका है भगवन का” ।
देकर यह संदेश, योगमाया
ने भव सागर गुँजाया ||
कारागृह में जन्म लिया, वसुदेव
देवकी सुत थे कान्हा ।
पर आँचल था भरा यशोदा
का, जिस गोदी खेले कान्हा ||
कालसर्प का योग बड़ा भारी
कुण्डली में पड़ा हुआ था ।
कितने रोगों दुर्घटनाओं
के कष्टों से भरा हुआ था ||
नष्ट किया उन सबही को, और
अमित पराक्रम दिखलाया था ।
माखन की चोरी करके, सबके
ही मन को मोह लिया था ||
बच्चों का पालन कैसे हो,
मात पिता को सिखलाया था ।
कितनी नैतिक शिक्षाओं को
निज लीला से सिखलाया था ||
राजनीति और कूटनीति का
मर्म तुम्हीं ने समझाया था ।
साम दाम और दण्ड भेद सब
उचित युद्ध में, सिखलाया था ||
प्रेम और सौहार्द रहे, यह
मर्म तुम्हीं ने समझाया था ।
कर्म करो निर्लिप्त भाव से,
दर्शन यह भी दिखलाया था ||
जो सम्मान प्रकृति को दोगे,
वह भी बिखराएगी ममता ।
इसी हेतु निज अँगुली पर
गोवर्धन को भी उठा लिया था ||
सारी गउएँ कामधेनु हैं,
अमृतपान कराएँगी ही ।
इसीलिए गउओं की रक्षा
का भी प्रण तुमने धारा था ||
सूझ बूझ से कर्म करो, निज
भाग्य विधाता बन जाओगे ।
कितने ही रण छोड़ो, करो
प्रयास, लक्ष्य को पा जाओगे ||
दया प्रेम करुणा के सागर,
तुमको वसुधा शीश नवाती ।
और चरण पखारे सागर,
नदियाँ कण्ठ हार बन जातीं ||
आकाश तुम्हारा नवल क्षेत्र,
द्युलोक तुम्हारा मस्तक है ।
यह धरा सकल है चरण कमल,
नासिका कुमार अश्विनी हैं ||
तुम सभी सूर्य चन्दा तारे
ग्रह नक्षत्रों के स्वामी हो ।
ये सभी तुम्हारी अनगिन देह
यष्टियों के ही रूप तो हैं ||
तुम ब्रह्मरूप में प्रकट हुए,
विस्तार सृष्टि का तुमसे ही।
तुम सकल कलायुत पूर्ण पुरुष,
है कठिन बहुत तुम सा बनना ||
पर सद्भावों से युत होकर
मानव माधव बन जाता है।
और अन्त समय में कृष्णरूप हो
ब्रह्मलीन हो जाता है ||
हरिहर झा, मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया

केशव रहे पुकार
राधा तकती पनघट पर या
युद्ध करे हुँकार
क्षण क्षण जीवन है संपूर्ण, केशव रहे पुकार।
संग गोपी के खेली रास
जग को रहे न भ्रम
मान दिलाने अबला को कब
पीछे पड़े कदम
नरकासुर की सौलह हजार ललना अंगीकार।
द्वारकाधीश का राजमहल,
सुदामा से प्रीत
आयाम अनोखे पल पल के
युद्ध या संगीत
कालिया नाग का फन कुचला, मुरली के फनकार।
अधरों पर बजती बंसी या
गिरि धारण करना
चेतन, जड़ में प्रेम, दंभ का
बूंद बूंद झरना
साग विदुर दे, दुर्योधन का मेवे से सत्कार।
गौपालक ने सबक सिखाया
इन्द्र अकड़बाज
मटकी फोड़ी,
कृष्न बचाये, द्रौपदी की लाज
झलक इक इक पूर्ण जीवित हो मूर्छा है बेकार।
मुड़ कर ना देखा वृंदावन,
पल निकला तो अंत
काल की धारा से निकलता
लम्हा हो जीवन्त
पल में किया गीता-ज्ञान से विश्व पर उपकार।
अजेय जुगरान

बाँसुरी में कान्हा
उनकी बाँसुरी सुनते – सुनते
प्राणों में माधुर्य भरते – भरते
पलों के पालों पार यमुना तक
मैं आ गया हूँ परम एकांत तट !
प्रतिध्वनि सौ सीपियों से आती भीनी
गोपियों की गेय पायल पदचाप धीमीं
दिखता यमुनाजल में यहाँ तैरता जीवंत
नील नभ का नयन भर प्रतिबिम्ब अनंत !
है कैसा यह नृत्यमंच अनोखा सृष्टि दृष्टि का सम झरोखा
पार करा सब सीमा रेखा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में करता एका!
मीत, निश्चित ही साँसों सधी बाँसुरी में हरि चौरसिया की
है निहित वो नवनीत प्रेमी राधे रसिया आनंद नंदन देवकी !
डॉ सुनीता शर्मा, मैलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया

प्रेम, भक्ति और जीवन के रंग में रंगी जन्माष्टमी
जन्माष्टमी केवल श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, करुणा और धर्म का स्मरण भी है। गोकुल की गलियों में गूँजती बंसी, राधा की आँखों में छलकता प्रेम, सुदामा की भक्ति, विदुर का सादापन —
ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि श्रीकृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि हर युग, हर हृदय के सखा, मार्गदर्शक और जीवन-संगीत हैं।
यह कविता उसी अमर प्रेम और भक्ति का एक विनम्र प्रणाम है।
कविता:
यशोदा के लाल, माखन चोर नटखट,
सिर सुशोभित मोरपंखी, नयनों में मधुर छलकन।
गोकुल की गलियों में रास रचाते,
बंसी की तान से जग को मोहित कर जाते।
जीवन कठिन, फिर भी इंद्रधनुषी,
तुम्हारे संग हर पीड़ा हो जाती सुगंधी।
प्रेम को जीना कैसा —
युगों-युगों से सिखाया तुमने,
न यह देह का आकर्षण,
यह तो आत्मा का पावन श्रृंगार।
राधा रोती रही तुम्हारी याद में,
तुम मुस्कुराते रहे राधा की बात में।
आंसू और हंसी — विरोधाभास जैसे,
पर तुम्हारे प्रेम में दोनों एक साथ बसे।
सुदामा के तंदुल, विदुर के साग,
रुक्मिणी के महल, राधा के राग —
हर रूप में भाव स्वीकारा,
प्रेम के बंधन में जग उतारा।
हे भोगेश्वर… हे योगेश्वर…
तुम्हारी गीता का अमर स्वर —
“कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन”
हर युग में देता सुमार्ग दर्शन।
आया जन्माष्टमी का पावन दिन,
गोकुल में गूँजे तुम्हारे चरण-छिन।
तुम्हारी मुरली की मधुर पुकार,
भक्ति में भीगे मेरे विचार।
कृष्ण तन… कृष्ण मन…
कृष्ण धर्म… कृष्ण कर्म…
चहुँ ओर गूँजे —
कृष्ण… कृष्ण… कृष्ण… कृष्ण…
राधा कृष्ण… राधा कृष्ण…
जब तक बहता है काल का प्रवाह,
तब तक अमर रहेगा तुम्हारा प्रेम —
सनातन, अद्वितीय, अपरिमेय।
डॉ अरुणा गुप्ता, दिल्ली

दिल्ली ६ – दिन जन्माष्टमी के
कृष्णोत्सव
त्योहार नहीं था केवल
एक दिन का,
कन्हैया का जन्म।
मची है धूम
कई दिनों से लग जाते थे
लोग, सजाने घरों को।
झांकियाँ बनेगी किसकी नायाब सबसे
क़तार होगी गली में किसकी
लंबी सबसे
होड़ सी थी लगती।
झूले पर ललना यशोदा का
दधी -माखन लपेटे
नटखट कन्हैया
गोपियों का दुलारा
नटवर रास -रसीला
बंसी बजैय्या
या कि सखा सुदामा का
लीलाधारी की लीला
करेगा कौन कितनी साकार।
बच्चा – बच्चा रहता जोशीला
लगे रहते दिन रात ,
ग़ज़ब की होती सजावट
रंग – बिरंगी बर्फ़ से सजाए जाते
मंदिर – मंदिर
बनती ऊँची मीनारें सिल्ली से बर्फ़ की ।
उचक उचक झांकते,
बजाते तालियाँ
नन्हे – मुन्ने।
ख़ुशी का पारावार,
लगता यों कि
गोप संग आ गए खुद करतार
किलकारी मानो मीठी बाँसुरी
गूंजती घर दुआर।
घर – घर बने पकवान
रोशनी से जाता नहा
शहर यह,जी भरके दुलार
ऐसा रहता कुछ समा
गूंजती घंटियाँ
भादो की रात
घनघोर बरसते कभी तो
बदरा बेताब
जमुना का उफान
मानो आज भी बेताब
छूने को चरण नंदलाल के।
पर कम न होता उछाह
दरस के पियासे नैन
झलक को एक
रहते बेताब
भीड़ का अंबार
उमड़ रहता जन – पारावार
यों मनाते हम त्योहार हर बार।
कम न होता कभी उल्लास।
मन रंजन के थे आधार।
हिल – मिल बनाते संसार।
डॉ रमा सिंह, जयपुर

दोहे कृष्ण जन्म पर
सुन कान्हा की बाँसुरी ऐसी तेज कटार।
चीर चीर दिल ले गई ना चितवन ना वार।।
वंशी कुछ ऐसी बजी बही प्रेम रसधार।
भावों का भण्डार ये गाती जीवन सार।।
नटवर नागर पर दिया ब्रज ने तन-मन वार।
नस -नस में बहता रहा साँवरिया का प्यार। ।
कण – कण में रमता सदा घट – घट उसका वास।
ब्रजमंडल के ईश पर सबका है विश्वास।।
नैन निहारें नवल छवि कृष्ण जन्म है आज।
तरह – तरह के बज रहे नन्द द्वार पर साज।।
श्यामल – श्यामल बदन है अधरों पर मुस्कान।
कृष्ण हिंडोला झूलते खींचें सबका ध्यान।।
सतरंगे से हो गए प्रेम रंग में डूब।
कान्हा राधा हो गए रास रचाया खूब।।
लीला तिवानी, नई दिल्ली

1. आए मेरे श्याम सखी खुशियां मनाओ री
आए मेरे श्याम सखी खुशियां मनाओ री
झूमो-नाचो-गाओ सखी मंदिर सजाओ री-
एक झांकी ऐसी हो कि पलने में नाथ हों
झूला झूलें दीनानाथ डोरी तेरे हाथ हो
डोरी सौंप श्याम को मंगल मनाओ री
झूमो-नाचो-गाओ सखी मंदिर सजाओ री-
एक झांकी ऐसी श्याम मखन चुराते हों
ग्वाल-बाल संग लेके लीलाएं रचाते हों
लीलाओं में सांवरे के मन को लगाओ री
झूमो-नाचो-गाओ सखी मंदिर सजाओ री-
एक झांकी ऐसी श्याम बांसुरी बजाते हों
बांसुरी की तान पे सृष्टि को नचाते हों
नाचो-नाचो सखी आओ श्याम को नचाओ री
झूमो-नाचो-गाओ सखी मंदिर सजाओ री-
एक झांकी ऐसी श्याम रास रचाते हों
राधिका के संग सारी गोपियां नचाते हों
गोपी बन जाओ तुम श्याम-श्याम गाओ री
झूमो-नाचो-गाओ सखी मंदिर सजाओ री-
एक झांकी ऐसी श्याम दरश दिखाते हों
आयु-बुद्धि-सेवा-वर प्रेमसे लुटाते हों
भक्ति-शक्ति-मुक्ति-वर पाने सखी आओ री
झूमो-नाचो-गाओ सखी मंदिर सजाओ री-
शरण तिहारी हे कृष्ण मुरारी
*****
2. शरण तिहारी हे कृष्ण मुरारी
शरण तिहारी हे कृष्ण मुरारी,
लाज रखो माधव भव-भयहारी,
द्रोपदी की लाज रखी चीर बढ़ाया,
हाथ बढ़ाकर टालो विपदा हमारी।
हे देवकी-सुत यशोदा के नंदलाल,
गीता-ज्ञान दे किया जग को निहाल,
भव से तरैया, धेनु-चरैया, माखनचोर,
रास-रचैया, नाग-नथैया, जय गोपाल।
गले बनमाल, माथे मोरमुकुट सोहे,
पीताम्बरधारी तेरी हर लीला मन मोहे,
जन्म-जन्म से तेरे दरश की प्यासी,
मन में आस ले दासी तेरी बाट जोहे।
नरसी की हुण्डी तारी, कुब्जा को तारा,
जग के कष्ट निवारे दुष्ट कंस को मारा,
मेरी वारी मेरे कन्हाई क्यों देर लगाई,
तेरी शरण आई तुझ पर तन-मन वारा।
