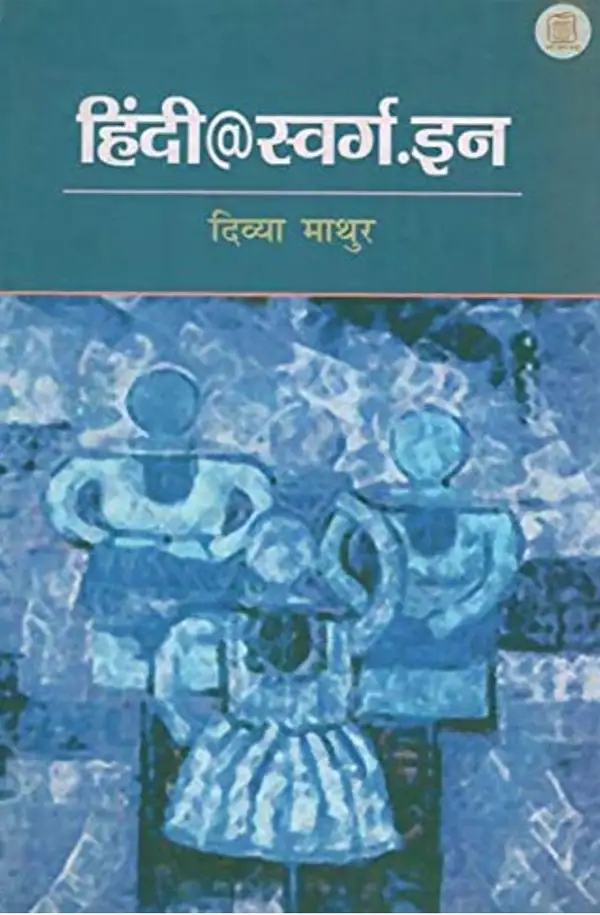
हिंदी@स्वर्ग.इन
कमल किशोर गोयनका
दिव्या माथुर इंग्लैंड के प्रसिद्ध हिंदी रचनाकारों में से एक हैं। उनकी रचनात्मकता के कई आयाम हैं —कविता, कहानी, नाटक, अनुवाद, फिल्म, गीत, गज़ल, रेडियो एवं दूरदर्शन में उनकी अपनी पहचान है। मेरा लगभग ढाई दशक पूर्व उनके कवयित्री रूप से परिचय हुआ और इसका श्रेय डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी को है जो इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त थे। डॉ. सिंघवी की जब इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति हुई तो मैंने बधाई दी और उनका जून, 1991 का लिखा उत्तर मुझे मिला जिसका यहाँ कुछ अंश उद्धृत है, क्योंकि यह अंश दिव्या माथुर के उस रचना-काल का एक चित्र उपस्थित करता है, जब वे कविताएँ लिख रही थीं और तब, सिंघवी जी के इंग्लैंड जाने के समय, वहाँ हिंदी की क्या स्थिति थी, ”यहाँ हिंदी में पत्राचार और बातचीत तथा वक्तव्यों का सिलसिला शुरू करने की कोशिश मैंने की है, किंतु यहाँ हिंदी के लिए संभावनाएँ बहुत सीमित हैं। यदि पत्र लिखवाना चाहूँ तो न कोई शीघ्रलिपिक है, न कोई कामचलाऊ यंत्र। यहाँ अधिकांश भारतवंशी लोग या तो पंजाबी-भाषी हैं या गुज़राती-भाषी। कल रात मैंने एक भाषण हिंदी और अंग्रेज़ी को मिलाकर दिया—मुझे भाषाओं का अंधाधुंध मिश्रण अटपटा लगता है, किंतु हिंदी के प्रयोग को प्रचलित करने के लिए यह भी करना पड़ा। सामान्य बातचीत में हिंदी का प्रयोग अवश्य होता है, किंतु अन्यथा नगण्य-सा। इन परिस्थितियों में डॉ. सिंघवी ने इंग्लैंड में हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकास का एक युग आरंभ किया जो इंग्लैंड के हिंदी प्रवासी साहित्य के इतिहास में ‘लक्ष्मीमल्ल सिंघवी युग ‘ के रूप में जाना जाएगा।
सिंघवी जी ने इंग्लैंड में, विशेषत: लंदन में, हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार किया, हिंदी लेखकों को लंदन बुलाया, हिंदी संस्थाओं की स्थापना कराई, हिंदी कवि-सम्मेलन कराए तथा अनेक हिंदी लेखकों की कृतियों का भारत में प्रकाशन कराया। इसी संदर्भ में उन्होंने मुझे दिव्या माथुर के कवयित्री रूप की जानकारी दी तथा उनके कहानी-संग्रह ‘रेत का लिखा’ को प्रकाशित कराने की जि़म्मेदारी सौंपी। दिव्या के दूसरे काव्य संकलन, ‘$खयाल तेरा’, का आमुख उन्होंने ही लिखा था इसलिए वह उनकी काव्य प्रतिभा से परिचित थे। मैं ऐसे अनेक रूपात्मक सहयोग मॉरिशस के हिंदी लेखकों को देता रहा था और मॉरिशस के प्रसिद्ध हिंदी लेखक अभिमन्यु अनत से बातचीत की पुस्तक छप चुकी थी। अत: दिव्या माथुर के इस काव्य-संग्रह को प्रकाशित कराने में मुझे प्रसन्नता हुई और इसलिए भी कि मेरे प्रवासी हिंदी लेखकों के परिवार का विस्तार हो रहा था।
दिव्या माथुर के काव्य-संसार के रसास्वादन से मेरी परिचय यात्रा आरंभ हुई। उनके छह कविता-संग्रह छप चुके हैं—’अंत: सलिता’ (1993), ‘खयाल तेरा (1998), ‘रेत का लिखा’ (1999), ’11 सितंबर: सपनों की राख तले’ (2002), ‘चंदन पानी’ (2007) तथा ‘झूठ, झूठ और झूठÓ (2008)। ‘रेत का लिखा’ की भूमिका में मैंने लिखा था कि दिव्या माथुर किसी एक विषय को केंद्र में रखकर उसके विविध पक्षों तथा रूपों को अपनी काव्यात्मक दृष्टि एवं संवेदना से आत्मसात् करके उन्हें जीवंत शब्दों में अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती है। यह काव्यात्मक क्षमता उनकी सर्जनात्मक कल्पना की घनीभूतता का प्रमाण है। दिव्या माथुर के अन्य काव्य-संग्रहों में भी विषय तथा अनुभूतियों की इस एकाग्रता का सौंदर्य मिलेगा।
दिव्या माथुर ने कहानी में कविता की तुलना में अच्छी पहचान बनाई है। उनकी कहानियाँ कुछ वर्षों से हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं, जिसके कारण उनका भारत में एक अच्छा पाठक वर्ग उत्पन्न हो गया है और हिंदी के प्रवासी कहानीकारों में उनका सम्मानपूर्ण स्थान बन गया है। दिव्या के अभी तक चार कहानी-संग्रह छप चुके हैं—’आक्रोश’ (2000), ‘पंगा’ (2010) तथा ‘2050’ (2011), और अब यह चौथा कहानी-संग्रह ‘हिंदी@स्वर्ग.इन’ (2013) पाठकों के हाथों में है। उनका पाँचवाँ कहानी-संग्रह ‘मेड इन इंडिया’ भी प्रैस में है।
दिव्या माथुर की सर्जनात्मक प्रतिभा का उदय यद्यपि आत्मकथात्मक कविता से हुआ था, किंतु उनकी पहली कहानी ‘प्रतीक्षा’ थी जो सन् 1962-65 के बीच में कभी लिखी गई थी। कहानी की मूल प्रेरणा लेखिका के घर के सामने रहनेवाली एक बाल-विधवा थी जिसे उसके घर के लोगों ने चुड़ैल बना दिया था। कहानी ऑटोमैटिक कानों के मज़ेदार प्रसंग से आरंभ होती है, परंतु वह एक विधवा की त्रासदी की मर्मस्पर्शी कहानी बन जाती है। कहानी में बिज्जी विधवा है, जिसकी सुहागरात से पहले ही दुल्हा चल बसा और वह पूरे घर की बैल की तरह सेविका बन गई और अपनी लाश को कंधे पर उठाए हवेली में घूमती रहती है। बिज्जी शालू को समझाती है कि पति की साँसों को पकडक़र रखना, अन्यथा उसके मरते ही सब इच्छाएँ चिता में जला दी जाएँगी। बिज्जी का जीवन और उसकी अनुभूतियाँ भारत में एक विधवा के दर्दनाक जीवन का उद्घाटन करती है। लेखिका की आयु उस समय 15 वर्ष के आसपास होगी, अत: लेखिका की अनुभूति की गहनता तथा सामाजिक सरोकार की दृष्टि को समझा जा सकता है। दूसरे कहानी ‘वह काली’ (1966-69) थी जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय की एक कहानी प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार मिला। लेखिका अपने शर्मीलेपन से पुरस्कार-समारोह में नहीं गई और कुछ समय बाद जब मुख्य अतिथि सर्वेश्वरदयाल सक्सेना से भेंट हुई तो वे लेखिका को ही काली लडक़ी समझ बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहानी की तारीफ की और लिखते रहने की प्रेरणा दी। इसके बाद ‘सदा सुहागिन’ कॉलेज पत्रिका में छपी जो भारत-पाक युद्ध के समय एक गुमशुदा सैनिक की पत्नी पर होने वाले अत्याचार की कहानी है। फिर उनकी 1972-78 के दौरान ‘नवभारत टाइम्स में ‘आत्महत्या के पहले’ तथा ‘आक्रोश’ दो कहानियाँ प्रकाशित हुईं।
दिव्या माथुर लंदन पहुँची तो नौकरी तथा दो बच्चों के पालन-पोषण के भार ने कहानी-रचना से कुछ दूर कर दिया। उन्होंने वहाँ रहते हुए 1985-86 में ‘दिशा’ कहानी लिखी जो एक ब्रेल पत्रिका के लिए लिखी गई थी। उनकी अब तक ‘संजीवन’, ‘आक्रोश’, ‘साँप-सीढ़ी’, ‘अपूर्व दिशा’, ‘फिर कभी सही’, आदि कहानियाँ ‘सारिका’, ‘कादंबिनी आदि पत्रिकाओं में छप चुकी थीं। दिव्या माथुर का 1997-98 में हिंद पॉकेट बुक्स के अमरनाथ से परिचय हुआ तो ‘ओडिसी’ (1998) शीर्षक से महिलाओं की कहानियों का अंग्रेज़ी अनुवाद छपा और उनका पहला कहानी-संग्रह ‘आक्रोश’ सन् 2000 में आया तथा इसकी भूमिका कमलेश्वर ने लिखी। भारत की लेखिकाओं की कहानियों का दूसरा अनुवाद ‘आशा’ सन् 2003 में प्रकाशित हुआ, परंतु अपनी कहानियों की रचना का कार्य स्थगित होता गया। डॉ. गोपाल गांधी ने सन् 1992 में लंदन के नेहरू-सेंटर में उनकी नियुक्ति की तो व्यस्तता के कारण कविताएँ ही लिखी गईं, परंतु कहानी के प्रति लगाव बना रहा और सन् 2010 में ‘पंगा’ तथा 2011 में ‘2050’ उनके दो कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए और उन्होंने प्रवासी कहानीकारों में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया। अब उनका यह कहानी-संग्रह ‘हिंदी@स्वर्ग.इन’ तथा इसके बाद आने वाला कहानी-संग्रह ‘गूगल’ उनकी पहचान को और भी पुष्ट तथा स्थायी बनाएगा।
इस कहानी-संग्रह में कुछ पूर्व में लिखी एवं संकलित कहानियाँ हैं तथा कुछ नई कहानियाँ हैं। इस संग्रह में 25 कहानियाँ हैं, जो जीवन के विविध आयामों, पक्षों तथा विभिन्न संवेदनाओं की कहानियाँ हैं जो दिव्या माथुर के अपने कहानी-संसार की रचना करती हैं। दिव्या माथुर के निजी एवं सामाजिक अनुभवों के इस कहानी-संसार में अपना देश और परदेश दोनों उपस्थित है और पूरी वास्तविकता के साथ उपस्थित है। वे यद्यपि कई दशकों से लंदन में हैं, किंतु उनका मातृदेश भारत कई रूप-रंगों, जीवन की कई सचाइयों तथा अच्छाइयों-बुराइयों के साथ जीवित है। ‘संजीवन’ दिल्ली की एक सँकरी गली में रहनेवाली विवाहिता सीमा की कहानी है जो पति, सास के साथ रहती है और पति और सास दोनों से पीडि़त है और एक कोठरी में घुटती रहती है। उसका वेतन पति उड़ा लेता है और सास व्यंग्य करती है और उसके पीहर का भी शोषण होता है, किंतु वह मिसेज़ गोयल की कोठी में रहने पहुँच जाती है। यही उसके लिए संजीवन है। सीमा इस प्रकार पश्चिम की आधुनिकता के बिना ही अपना नया रास्ता बनाती है और लेखिका भारतीय स्त्री में नए सिरे से जीने की आकांक्षा उत्पन्न करती है और वह इसके लिए पति-परिवार सबकी मर्यादा तोडक़र अपने लिए जीने को तत्पर होती है।
‘आक्रोश’ एक भारतीय स्त्री के गर्भपात कराने की मार्मिक कहानी है, जो तीसरी संतान इसलिए पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले ही दो बेटियों का पालन-पोषण कठिन है। कहानी में उसके पति अशोक का निर्मोहीपन और क्रिकेट मैच देखने की उत्सुकता हिंदुस्तानी पत्नी की बेबसी और महत्त्वहीनता को उद्घाटित करती है। ‘सांप-सीढ़ी’ कहानी बच्चोंवाली विधवा के जीवन की कहानी है जिसमें विधवा का बेटा राहुल अपनी माँ का सम्बल बनता है। हिंदुस्तानी जीवन और समाज की ऐसी कहानियाँ दिव्या माथुर की गहन-दृष्टि और उनके भारतीय सरोकारों से परिचित कराती हैं। इनमें उनकी मौलिकता के साथ जीवन को नई दृष्टि से चित्रित करने का कौशल है।
दिव्या माथुर की विदेशी रंगमंच पर घटित होने वाली कहानियों के अधिकांश पात्र भी भारतीय हैं। इस प्रकार से भारतीय पात्रों की विदेशी परिवेश, परिस्थितियों, नए संबंध-सूत्रों तथा स्वदेश-परदेश मिश्रित सरोकारों की कहानियाँ हैं। ‘वैलेंटाइंस डे’ कहानी है तो भारतीय चरित्रों की है, किंतु रंगमंच है लंदन और मदन अपनी एक न एक प्रेमिका के साथ वैलेंटाइंस डे को मनाना चाहता है। वह अपने साथियों में अपने व्यवहार के कारण बदनाम है और उसकी प्रेमिकाएँ भी उसके छैलेपन को जान गई हैं। उसकी पुरानी प्रेमिका उससे काफी खर्च कराती है और अपनी सहेलियों-शैला और एंजी के साथ उसे सबक सिखाती हैं। भारतीय स्त्री-पुरुष भी योरोपियनों की तरह प्रेमी-प्रेमिका बदलते रहते हैं और भोग ही केंद्र बन जाता है।
‘नीली डायरी’ भी इसी प्रवृत्ति की कहानी है। पुरुष की स्त्री को भोगने की चरमावस्था की कहानी है। पात्र यहाँ भी सब भारतीय हैं। कहानी लंदन की है। रमन रिजवान पंद्रह सालों में अठानवें औरतों के साथ सो चुका है। उन सबके नाम उसने अपनी नीली डायरी में लिखे हुए हैं और वह अब सौ की गिनती पूरी करना चाहता है। संयोग से उसके पड़ोस में कपूर परिवार आकर रहता है और इस परिवार की अधेड़ रीमा, अल्हड़ बेटी ज़ारा तथा नई नवेली बहू स्नेहा तीनों ही रमन के काम-जाल में फँसने को तैयार हैं। रीमा तो स्वयं आकर समर्पण करती है और रमन स्नेहा को वश में करके नीली डायरी में सौ की संख्या पूरी करने की तैयारी कर लेता है। इस कहानी से स्पष्ट है कि योरोप में भारतीय स्त्री-पुरुष भी योरोपियन हो गए हैं और यौन-संबंध एवं भोग-तृप्ति ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। योरोपियन जीवन-शैली ने भारतीयों का भारतीयपन छीनकर उन्हें पूरा भोगवादी बना दिया है, परंतु ‘बचाव’ कहानी में इंग्लैंड भागकर गई भारतीय स्त्री निंदिया अपने बौस के बलात्कार के प्रयास पर खौलता पानी डालकर भाग खड़ी होती है और अपनी यौन-पवित्रता की रक्षा करती है। इंग्लैंड में हिंदुस्तानी समाज बदल गया है, किंतु निंदिया जैसी हिंदुस्तानी स्त्री में हिंदुस्तानी चमक अभी बाकी है और वह अपने स्त्रीत्व की रक्षा कर सकती है। इस कहानी में लेखिका की सहानुभूति निंदिया के साथ है।
दिव्या माथुर की कहानियों में फैंटेसी की भी प्रवृत्ति है। रचनाकार फैंटेसी में अपनी कल्पना से एक नए संसार की रचना करता है, जो यथार्थ न होकर भी जीवन के किसी अकल्पनीय पक्ष का उद्घाटन करता है। फैंटेसी रचनाकार की दुर्बलता नहीं है, उसकी कल्पनाशीलता का परिणाम है कि वह पाठक को एक नए परिदृश्य, एक नई संवेदना तथा एक नए संसार से साक्षात्कार कराती है। ‘पुरू और प्राची’ ऐसी ही कहानी हैं जो बीकानेर के एक मारवाड़ी व्यापारी और उसके अमेरिका निवासी पुत्र तथा उसकी विदेशी पत्नी रुडक़ी स्थिति प्राची स्पेस सेंटर के कैपसूल से चाँद की यात्रा करते हैं और इन पात्रों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं। चांद-यात्रा के बाद नारायण परिवार का जीवन ही बदल जाता है, व्यापार आसमान छूने लगता है, पिता-पुत्र दोनों के एक-एक संतान होती है और हरि नारायण नए उपक्रमों के बारे में सोचता है। कहानी मनुष्य की महत्त्वाकांक्षा और लिप्सा का रोचक वर्णन करती है, प्रचार और व्यापार में उन्नति होती है और यह फैंटेसी है। लेखिका 2050 में एक ऐसे मानवीय समाज की कल्पना करती है जहाँ ‘हाई आई-क्यू’ वाले पति-पत्नी ही संतान पैदा कर सकेंगे और उन्हें इसके लिए ‘समाज सुरक्षा परिषद्’ की परीक्षा से गुज़रकर अनुमति लेनी होगी। ‘समाज सुरक्षा परिषद् के अधिकारी रेसिस्ट हैं और वे भारतीय जोड़ों को विदेशी स्पर्म से संतानोपत्ति के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु वेद और ऋचा इसे ठुकरा देते हैं। परिषद् 2050 तक ऐसा मानव समाज बनाना चाहती है जिसमें कोई गरीब, बीमार और बेकार न हो और इसके लिए वह भावी माता-पिता की परीक्षा लेकर ही अनुमति देती है। परिषद् पति-पत्नी की भावनाएँ कुचलती है, गर्भपात कराती है, आत्महत्या की अनुमति देती है और विरोध को कुचलती है। यह गोरी जाति का नया षड्यंत्र है एशियाई जनसंख्या को कम करने का, परंतु कहानी कहती है कि भारत सरकार भी इंग्लैंड के तरीकों को अपनाने पर विचार कर रही है। कहानीकार की कल्पना एक ऐसे मानवीय समाज को देखती है जिसमें गोरों का प्रभुत्व होगा, सब मनुष्य श्रेष्ठ होंगे और निम्न कोटि के मनुष्यों का संतानोत्पत्ति का अधिकार छीन लिया जाएगा। कहानी एक फैंटेसी है, किंतु यदि इसके सत्य होने की संभावना है तो यह भयभीत करती है। मनुष्य और प्रकृति की इस लड़ाई में यदि मनुष्य जीतता है तो मनुष्य समाज का रूप-रंग रचना सब बदल जाएगा। मनुष्य भावनाविहीन एवं अमानवीय बनकर यांत्रिक मनुष्य बनकर रह जाएगा। कहानी की यह फैंटेसी उसे बड़ी कहानी बनाती है। दिव्या माथुर की ‘हिंदी@स्वर्ग.इन’ कहानी भी एक फैंटेसी है, लेकिन वह दूसरे प्रकार की है। इसमें दिव्या माथुर स्वयं एक पात्र हैं। वह एक कार दुर्घटना के बाद स्वर्ग पहुँचती हैं तो वहाँ कमलेश्वर, लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, महावीर शर्मा, मनोहरश्याम जोशी, कन्हैयालाल नंदन, प्रभा खेतान आदि से भेंट होती है और परस्पर संवाद होता है। यह कहानी दिव्या माथुर के नेहरू सेंटर के कार्यक्रमों तथा उनके साहित्य पर चर्चा करती है और प्रवासी साहित्य का प्रसंग भी आ जाता है। दिव्या माथुर प्रवासी साहित्य की उपेक्षा पर चोट करती हुई स्वर्ग में उपस्थित हिंदी लेखकों से कहती हैं, ‘तो फिर उन सबका जि़क्र पत्र-पत्रिकाएँ क्यों नहीं करतीं? आप जैसे लेखकों के पास समय ही नहीं हम लेखकों को ठीक से पढऩे-सुनने का। जाने-माने लेखक भी एक-आध कहानी और कविता पढक़र अपने को प्रवासी-एक्सपर्ट कहलवाने लगते हैं। इस प्रकार फैंटेसी भी जीवन के कुछ यथार्थ को सामने ले आती है। कहानी पूर्णत: कपोल कल्पना है, किंतु नई संवेदना तथा नई तकनीक का प्रयोग है। कहानी स्वर्ग में घटित होकर भी धरती के जीवन का रसास्वादन कराती है और फैंटेसी जीवन से जुड़ जाती है।
दिव्या माथुर की ये कहानियाँ एक नया आस्वादन कराती हैं और कहानीकार के रूप में उनकी अलग पहचान को स्थापित करती हैं। वह प्रवासी हिंदी कहानीकारों में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और अपनी मौलिकता तथा अनुभवों के नए संसार को बनाए रखती हैं। उनकी कहानियों में जीवन का वैविध्य है, सघन संवेदना है, और अभिव्यक्ति में प्रेषणीयता है। उनकी कहानियों में भारत जीवित है, इंग्लैंड में रहने वाला भारत भी जीवित है तथा वहाँ का भावी भारत भी कहानियों में विद्यमान है। दिव्या माथुर के पास एक भारतीय दृष्टि है जो सीधे हस्तक्षेप तथा लेखकीय उपस्थिति के बिना भी अपने संकेतों, कथावस्तु तथा पात्रों के व्यवहारों तथा सरोकारों से व्यंजित होती है। वे कहानीकार के रूप में भारतीयता एवं भारतीय जीवन-मूल्यों की स्थापना के प्रति आग्रहशील नहीं हैं, किंतु वे बड़ी तटस्थता के साथ अपने भारतीयपन को उजागर कर देती हैं। उनकी कहानियों में जो भारतीय स्त्री है, उसके कई रूप हैं—पश्चिमी और भारतीय, परंतु लेखिका का पक्ष भारतीय स्त्री के साथ है। ‘बचाव’ कहानी में निंदिया के बचाव में यही भारतीयता काम करती है। दिव्या माथुर में एक बोल्डनैस है, इसी कारण वे ‘नीली डायरी’ जैसी कहानियाँ लिख सकी है। उनमें फैंटेसी का सौंदर्य भी है और साथ ही जीवन-यथार्थ की मार्मिकता भी है। वह एक ऐसी कहानीकार हैं जो जीवन को सीधे-सरल रूप में, बिना किसी नाटकीयता के साथ प्रस्तुत कर देती हैं और सच यह भी है कि उनके कहानीकार में अनछुए प्रसंगों तथा अलिखित जीवन-छवियों के चित्रण की और उन्हें प्रेषणीय भाषा में अभिव्यक्त करने की क्षमता है। उनकी कहानी-यात्रा में अभी बड़ी संभावनाएँ हैं। हिंदी कहानी साहित्य को उनकी मास्टरपीस रचना की प्रतीक्षा रहेगी। वे प्रवासी हिंदी कहानी में महत्त्वपूर्ण स्थान बना चुकी हैं और हिंदी की मुख्यधारा में भी उनके उचित स्थान को अब कोई चुनौती नहीं दे सकता।
*** *** ***
